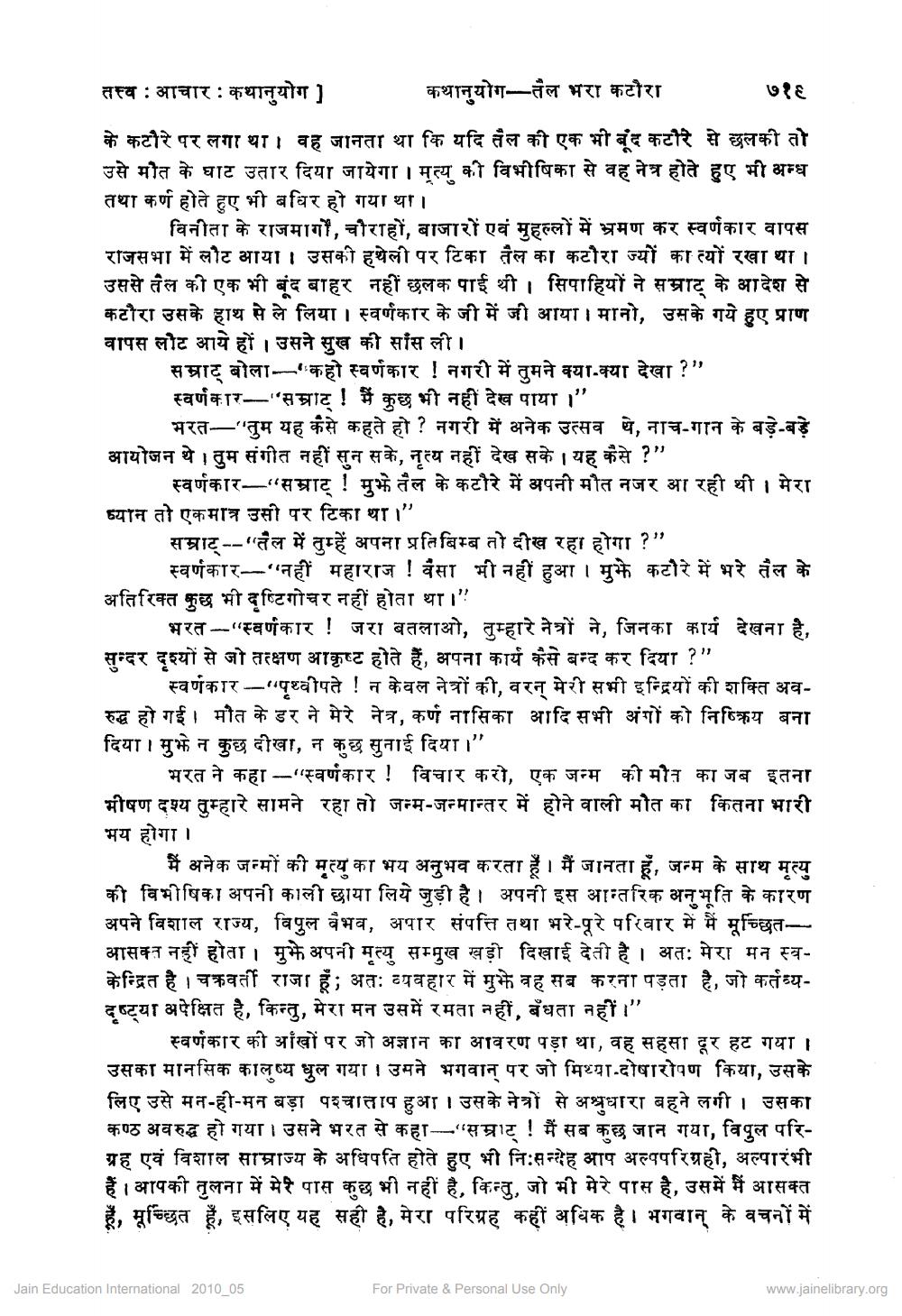________________
तत्त्व : आचार : कथानुयोग ] कथानुयोग-तैल भरा कटोरा के कटौरे पर लगा था। वह जानता था कि यदि तैल की एक भी बूंद कटौरे से छलकी तो उसे मौत के घाट उतार दिया जायेगा। मृत्यु की विभीषिका से वह नेत्र होते हुए भी अन्ध तथा कर्ण होते हुए भी बधिर हो गया था।
विनीता के राजमार्गों, चौराहों, बाजारों एवं मुहल्लों में भ्रमण कर स्वर्णकार वापस राजसभा में लौट आया। उसकी हथेली पर टिका तैल का कटौरा ज्यों का त्यों रखा था। उससे तेल की एक भी बूंद बाहर नहीं छलक पाई थी। सिपाहियों ने सम्राट के आदेश से कटौरा उसके हाथ से ले लिया। स्वर्णकार के जी में जी आया। मानो, उसके गये हुए प्राण वापस लौट आये हों। उसने सुख की सांस ली।
सम्राट् बोला-'कहो स्वर्णकार ! नगरी में तुमने क्या-क्या देखा?" स्वर्णकार-“सम्राट् ! मैं कुछ भी नहीं देख पाया।"
भरत–'तुम यह कैसे कहते हो ? नगरी में अनेक उत्सव थे, नाच-गान के बड़े-बड़े आयोजन थे। तुम संगीत नहीं सुन सके, नृत्य नहीं देख सके । यह कैसे ?"
स्वर्णकार-"सम्राट् ! मुझे तैल के कटोरे में अपनी मौत नजर आ रही थी। मेरा ध्यान तो एकमात्र उसी पर टिका था।"
सम्राट -- "तैल में तुम्हें अपना प्रतिबिम्ब तो दीख रहा होगा ?"
स्वर्णकार--"नहीं महाराज ! वैसा भी नहीं हुआ । मुझे कटोरे में भरे तैल के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता था।"
भरत - "स्वर्णकार ! जरा बतलाओ, तुम्हारे नेत्रों ने, जिनका कार्य देखना है, सुन्दर दृश्यों से जो तत्क्षण आकृष्ट होते हैं, अपना कार्य कैसे बन्द कर दिया ?"
स्वर्णकार -"पृथ्वीपते ! न केवल नेत्रों की, वरन् मेरी सभी इन्द्रियों की शक्ति अवरुद्ध हो गई। मौत के डर ने मेरे नेत्र, कर्ण नासिका आदि सभी अंगों को निष्क्रिय बना दिया। मुझे न कुछ दीखा, न कुछ सुनाई दिया।"
भरत ने कहा -"स्वर्णकार ! विचार करो, एक जन्म की मौत का जब इतना भीषण दश्य तुम्हारे सामने रहा तो जन्म-जन्मान्तर में होने वाली मौत का कितना भारी भय होगा।
मैं अनेक जन्मों की मृत्यु का भय अनुभव करता हूँ। मैं जानता हूँ, जन्म के साथ मृत्यु की विभीषिका अपनी काली छाया लिये जुड़ी है। अपनी इस आन्तरिक अनुभूति के कारण अपने विशाल राज्य, विपुल वैभव, अपार संपत्ति तथा भरे-पूरे परिवार में मैं मूच्छितआसक्त नहीं होता। मुझे अपनी मृत्यु सम्मुख खड़ी दिखाई देती है। अत: मेरा मन स्वकेन्द्रित है । चक्रवर्ती राजा हूँ; अत: व्यवहार में मुझे वह सब करना पड़ता है, जो कर्तव्यदष्ट्या अपेक्षित है, किन्तु, मेरा मन उसमें रमता नहीं. बँधता नहीं।"
स्वर्णकार की आँखों पर जो अज्ञान का आवरण पड़ा था, वह सहसा दूर हट गया। उसका मानसिक कालुष्य धुल गया। उसने भगवान् पर जो मिथ्या-दोषारोपण किया, उसके लिए उसे मन-ही-मन बड़ा पश्चाताप हुआ। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसका कण्ठ अवरुद्ध हो गया। उसने भरत से कहा-“सम्राट् ! मैं सब कुछ जान गया, विपुल परिग्रह एवं विशाल साम्राज्य के अधिपति होते हुए भी निःसन्देह आप अल्पपरिग्रही, अल्पारंभी हैं । आपकी तुलना में मेरे पास कुछ भी नहीं है, किन्तु, जो भी मेरे पास है, उसमें मैं आसक्त हूँ, मूच्छित हूँ, इसलिए यह सही है, मेरा परिग्रह कहीं अधिक है। भगवान् के वचनों में
____Jain Education International 2010_05
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org