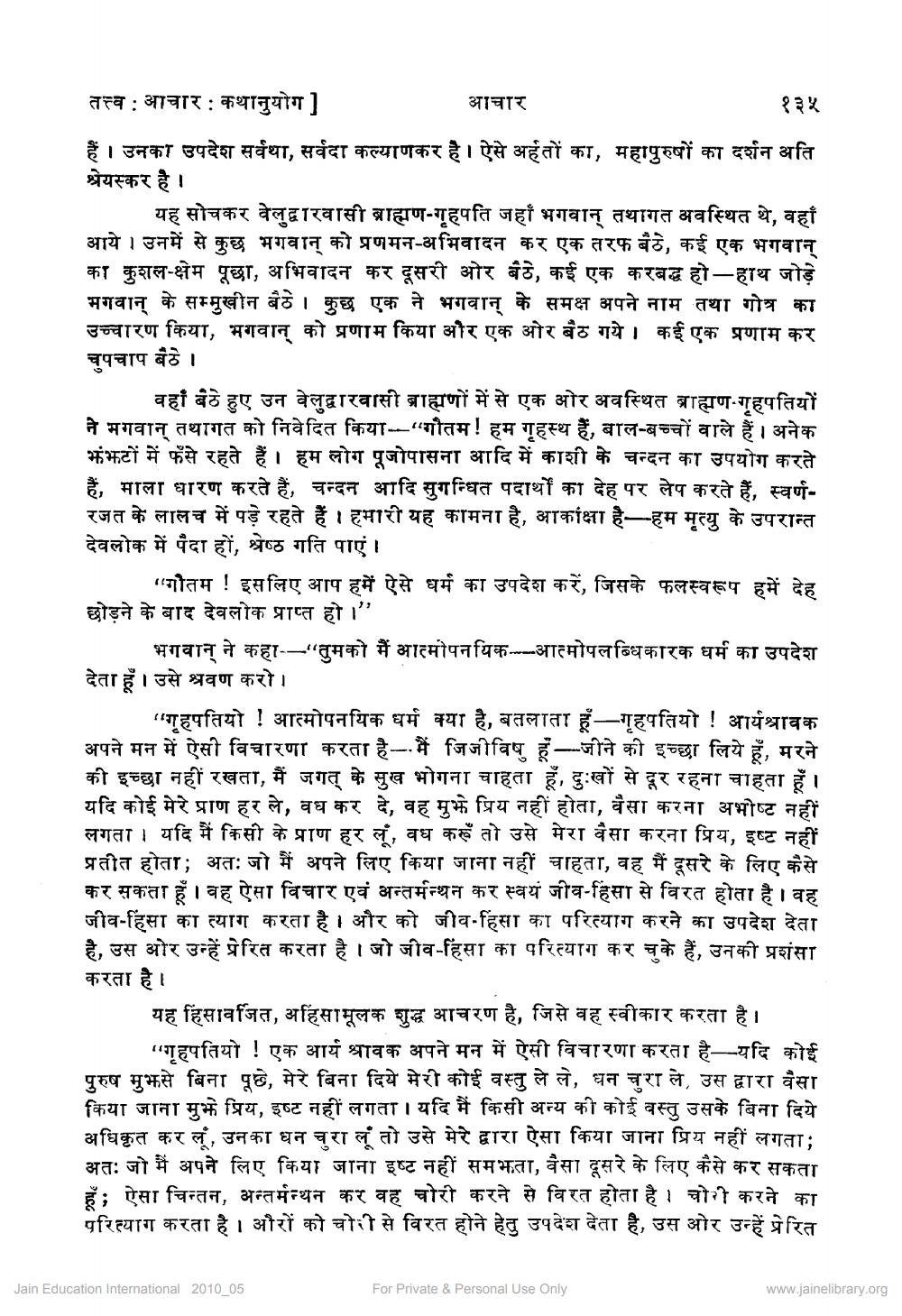________________
तत्त्व : आचार : कथानुयोग]
आचार
१३५ हैं । उनका उपदेश सर्वथा, सर्वदा कल्याणकर है। ऐसे अर्हतों का, महापुरुषों का दर्शन अति श्रेयस्कर है।
यह सोचकर वेलुद्वारवासी ब्राह्मण-गृहपति जहाँ भगवान् तथागत अवस्थित थे, वहाँ आये । उनमें से कुछ भगवान् को प्रणमन-अभिवादन कर एक तरफ बैठे, कई एक भगवान् का कुशल-क्षेम पूछा, अभिवादन कर दूसरी ओर बैठे, कई एक करबद्ध हो-हाथ जोड़े भगवान् के सम्मुखीन बैठे। कुछ एक ने भगवान् के समक्ष अपने नाम तथा गोत्र का उच्चारण किया, भगवान को प्रणाम किया और एक ओर बैठ गये। कई एक प्रणाम कर चुपचाप बैठे।
वहाँ बैठे हुए उन वेलुद्वारवासी ब्राह्मणों में से एक ओर अवस्थित ब्राह्मण-गृहपतियों ने भगवान् तथागत को निवेदित किया-“गौतम! हम गृहस्थ हैं, बाल-बच्चों वाले हैं। अनेक झंझटों में फंसे रहते हैं। हम लोग पूजोपासना आदि में काशी के चन्दन का उपयोग करते हैं, माला धारण करते हैं, चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थों का देह पर लेप करते हैं, स्वर्णरजत के लालच में पड़े रहते हैं। हमारी यह कामना है, आकांक्षा है-हम मृत्यु के उपरान्त देवलोक में पैदा हों, श्रेष्ठ गति पाएं।
"गौतम ! इसलिए आप हमें ऐसे धर्म का उपदेश करें, जिसके फलस्वरूप हमें देह छोड़ने के बाद देवलोक प्राप्त हो।"
भगवान् ने कहा--"तुमको मैं आत्मोपनयिक..-आत्मोपलब्धिकारक धर्म का उपदेश देता हूँ। उसे श्रवण करो।
गृहपतियो ! आत्मोपनयिक धर्म क्या है, बतलाता हूँ-गृहपतियो ! आर्यश्रावक अपने मन में ऐसी विचारणा करता है-.मैं जिजीविषु हूँ-जीने की इच्छा लिये हूँ, मरने की इच्छा नहीं रखता, मैं जगत् के सुख भोगना चाहता हूँ, दुःखों से दूर रहना चाहता हूँ। यदि कोई मेरे प्राण हर ले, वध कर दे, वह मुझे प्रिय नहीं होता, वैसा करना अभीष्ट नहीं लगता । यदि मैं किसी के प्राण हर लूं, वध करूँ तो उसे मेरा वैसा करना प्रिय, इष्ट नहीं प्रतीत होता; अतः जो मैं अपने लिए किया जाना नहीं चाहता, वह मैं दूसरे के लिए कैसे कर सकता हूँ। वह ऐसा विचार एवं अन्तर्मन्थन कर स्वयं जीव-हिंसा से विरत होता है। वह जीव-हिंसा का त्याग करता है। और को जीव-हिंसा का परित्याग करने का उपदेश देता है, उस ओर उन्हें प्रेरित करता है । जो जीव-हिंसा का परित्याग कर चुके हैं, उनकी प्रशंसा करता है।
यह हिंसावजित, अहिंसामूलक शुद्ध आचरण है, जिसे वह स्वीकार करता है।
"गृहपतियो ! एक आर्य श्रावक अपने मन में ऐसी विचारणा करता है—यदि कोई पुरुष मुझसे बिना पूछे, मेरे बिना दिये मेरी कोई वस्तु ले ले, धन चुरा ले, उस द्वारा वैसा किया जाना मुझे प्रिय, इष्ट नहीं लगता । यदि मैं किसी अन्य की कोई वस्तु उसके बिना दिये अधिकृत कर लूं, उनका धन चुरा लूं तो उसे मेरे द्वारा ऐसा किया जाना प्रिय नहीं लगता; अतः जो मैं अपने लिए किया जाना इष्ट नहीं समझता, वैसा दूसरे के लिए कैसे कर सकता हूँ; ऐसा चिन्तन, अन्तर्मन्थन कर वह चोरी करने से विरत होता है। चोरी करने का परित्याग करता है। औरों को चोरी से विरत होने हेतु उपदेश देता है, उस ओर उन्हें प्रेरित
____Jain Education International 2010_05
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org