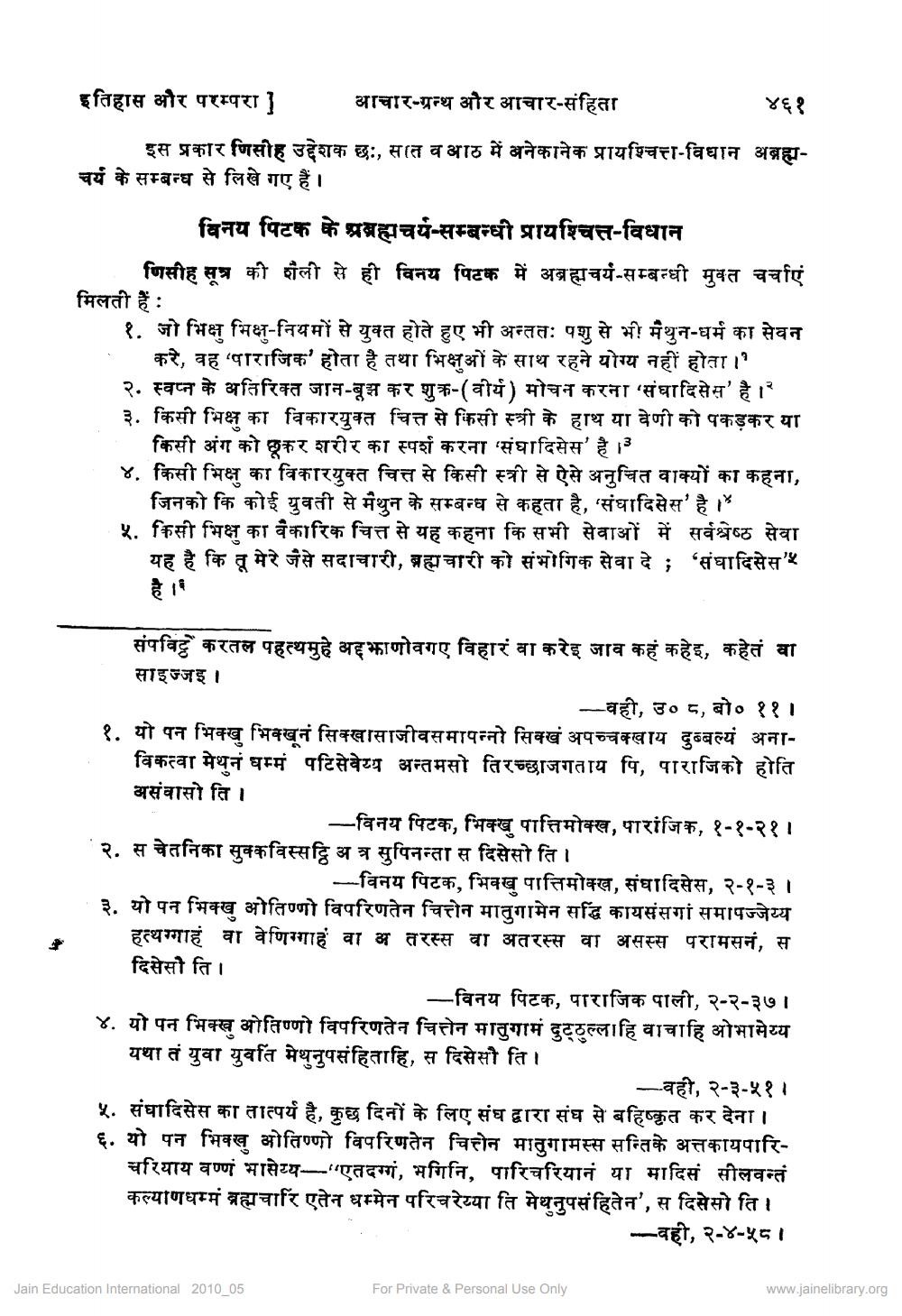________________
४६१
इतिहास और परम्परा] आचार-ग्रन्थ और आचार-संहिता
इस प्रकार णिसीह उद्देशक छः, सात व आठ में अनेकानेक प्रायश्चित्त-विधान अब्रह्मचर्य के सम्बन्ध से लिखे गए हैं।
विनय पिटक के अब्रह्मचर्य-सम्बन्धी प्रायश्चित्त-विधान णिसीह सूत्र की शैली से ही विनय पिटक में अब्रह्मचर्य-सम्बन्धी मुक्त चर्चाएं मिलती हैं :
१. जो भिक्षु भिक्षु-नियमों से युक्त होते हुए भी अन्ततः पशु से भी मैथुन-धर्म का सेवन - करे, वह पाराजिक' होता है तथा भिक्षुओं के साथ रहने योग्य नहीं होता।' २. स्वप्न के अतिरिक्त जान-बूझ कर शुक्र-(वीर्य) मोचन करना ‘संघादिसेस' है। ३. किसी भिक्षु का विकारयुक्त चित्त से किसी स्त्री के हाथ या वेणी को पकड़कर या
किसी अंग को छूकर शरीर का स्पर्श करना 'संघादिसेस' है। ४. किसी भिक्षु का विकारयुक्त चित्त से किसी स्त्री से ऐसे अनुचित वाक्यों का कहना, __जिनको कि कोई युवती से मैथुन के सम्बन्ध से कहता है, 'संघादिसेस' है। ५. किसी भिक्षु का वैकारिक चित्त से यह कहना कि सभी सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ सेवा
यह है कि तू मेरे जैसे सदाचारी, ब्रह्मचारी को संभोगिक सेवा दे ; ‘संघादिसेस'५
के
संपवि? करतल पहत्थमुहे अद्दझाणोवगए विहारं वा करेइ जाव कहं कहेइ, कहेतं वा साइज्जइ।
-वही, उ० ८, बो० ११ । १. यो पन भिक्खु भिक्खूनं सिक्खासाजीवसमापन्नो सिक्खं अपच्चक्खाय दुब्बल्यं अना
विकत्वा मेथुनं धम्म पटिसेवेय्य अन्तमसो तिरच्छाजगताय पि, पाराजिको होति असंवासोति ।
-विनय पिटक, भिक्खु पात्तिमोक्ख, पारांजिक, १-१-२१ । २. स चेतनिका सुक्कविस्सट्ठि अत्र सुपिनन्ता स दिसेसो ति ।
--विनय पिटक, भिक्खु पात्तिमोक्ख, संघादिसेस, २-१-३ । ३. यो पन भिक्खु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामेन सद्धि कायसंसगां समापज्जेय्य
हत्थग्गाहं वा वेणिग्गाहं वा अ तरस्स वा अतरस्स वा असस्स परामसनं, स दिसेसो ति।
__-विनय पिटक, पाराजिक पाली, २-२-३७ । ४. यो पन भिक्खु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामं दुठ्ठल्लाहि वाचाहि ओभासेय्य यथा तं युवा युवति मेथुनुपसंहिताहि, स दिसेसो ति।
-वही, २-३-५१। ५. संघादिसेस का तात्पर्य है, कुछ दिनों के लिए संघ द्वारा संघ से बहिष्कृत कर देना। ६. यो पन भिक्खु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामस्स सन्तिके अत्तकायपारि
चरियाय वण्णं भासेय्य-"एतदग्गं, भगिनि, पारिचरियानं या मादिसं सीलवन्तं कल्याणधम्मं ब्रह्मचारिं एतेन धम्मेन परिचरेय्या ति मेथुनुपसंहितेन', स दिसेसो ति ।
-वही, २-४-५८ ।
Jain Education International 2010_05
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org