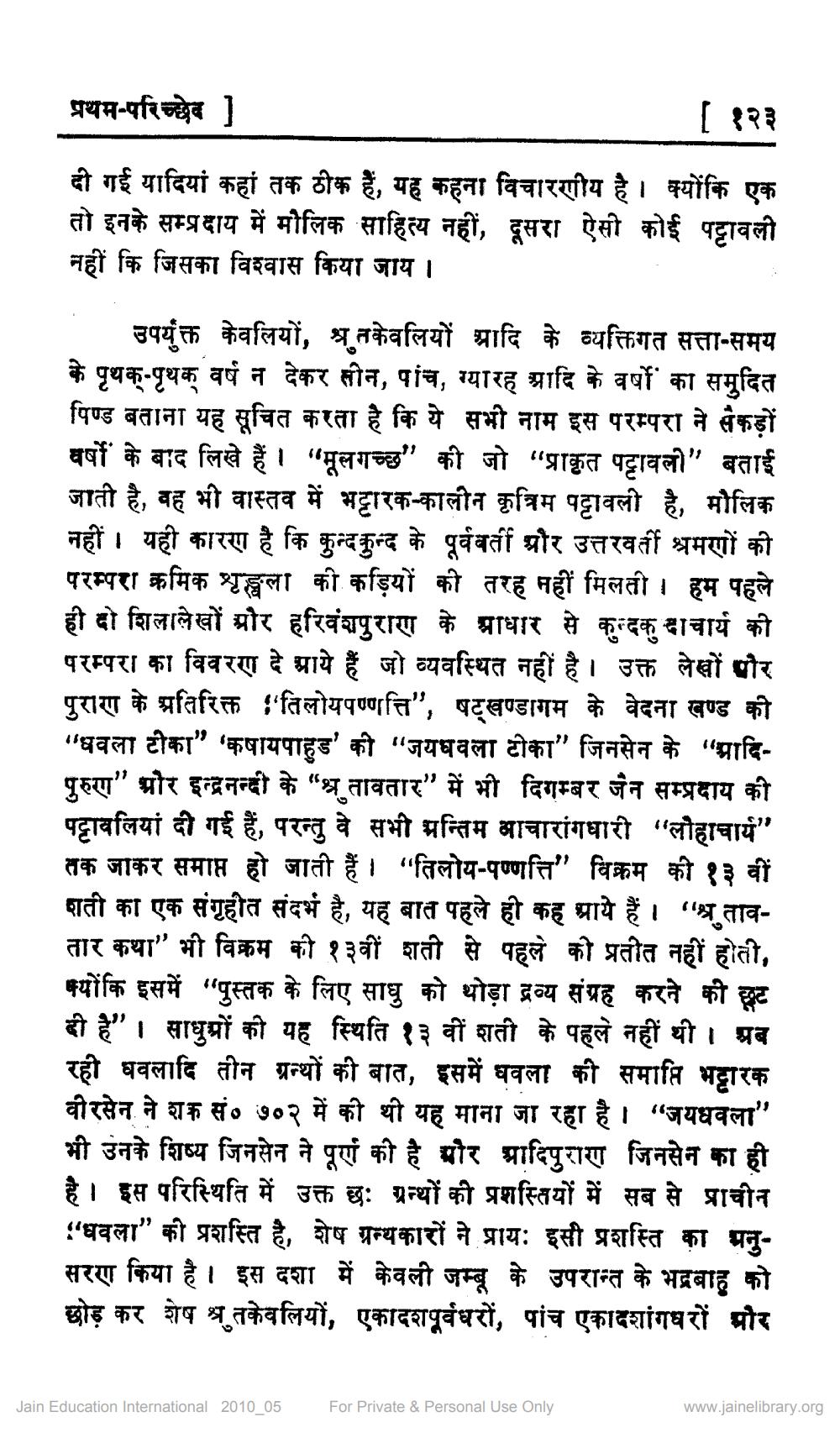________________
प्रथम-परिच्छेद ]
[ १२३
दी गई यादियां कहां तक ठीक हैं, यह कहना विचारणीय है। क्योंकि एक तो इनके सम्प्रदाय में मौलिक साहित्य नहीं, दूसरा ऐसी कोई पट्टावली नहीं कि जिसका विश्वास किया जाय ।
उपर्युक्त केवलियों, श्रुतकेवलियों आदि के व्यक्तिगत सत्ता-समय के पृथक्-पृथक वर्ष न देकर सीन, पांच, ग्यारह आदि के वर्षों का समुदित पिण्ड बताना यह सूचित करता है कि ये सभी नाम इस परम्परा ने सैकड़ों वर्षों के बाद लिखे हैं। "मूलगच्छ" की जो "प्राकृत पट्टावलो" बताई जाती है, वह भी वास्तव में भट्टारक-कालीन कृत्रिम पट्टावली है, मौलिक नहीं। यही कारण है कि कुन्दकुन्द के पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती श्रमणों की परम्परा क्रमिक शृङ्खला की कड़ियों की तरह नहीं मिलती। हम पहले ही दो शिलालेखों और हरिवंशपुराण के आधार से कुन्दकु क्षाचार्य की परम्परा का विवरण दे पाये हैं जो व्यवस्थित नहीं है। उक्त लेखों पौर पुराण के अतिरिक्त "तिलोयपण्णत्ति", षट्खण्डागम के वेदना खण्ड की "धवला टीका" 'कषायपाहुड' की "जयधवला टोका" जिनसेन के "मादिपुरुण" और इन्द्रनन्दी के "श्रु तावतार" में भी दिगम्बर जैन सम्प्रदाय की पट्टावलियां दी गई हैं, परन्तु वे सभी अन्तिम आचारांगधारी "लोहाचार्य" तक जाकर समाप्त हो जाती हैं । "तिलोय-पण्णत्ति" विक्रम की १३ वीं शती का एक संगृहीत संदर्भ है, यह बात पहले ही कह पाये हैं। "श्रु तावतार कथा" भी विक्रम की १३वीं शती से पहले की प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इसमें "पुस्तक के लिए साधु को थोड़ा द्रव्य संग्रह करने की छूट दी है" | साधुनों की यह स्थिति १३ वीं शती के पहले नहीं थी। अब रही धवलादि तीन ग्रन्थों की बात, इसमें धवला की समाप्ति भट्टारक वीरसेन ने शक सं० ७०२ में की थी यह माना जा रहा है । “जयधवला" भी उनके शिष्य जिनसेन ने पूर्ण की है और प्रादिपुराण जिनसेन का ही है। इस परिस्थिति में उक्त छः ग्रन्थों की प्रशस्तियों में सब से प्राचीन "धवला" को प्रशस्ति है, शेष ग्रन्थकारों ने प्रायः इसी प्रशस्ति का अनुसरण किया है। इस दशा में केवली जम्बू के उपरान्त के भद्रबाहु को छोड़ कर शेष श्रुतकेवलियों, एकादशपूर्वधरों, पांच एकादशांगधरों और
Jain Education International 2010_05
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org