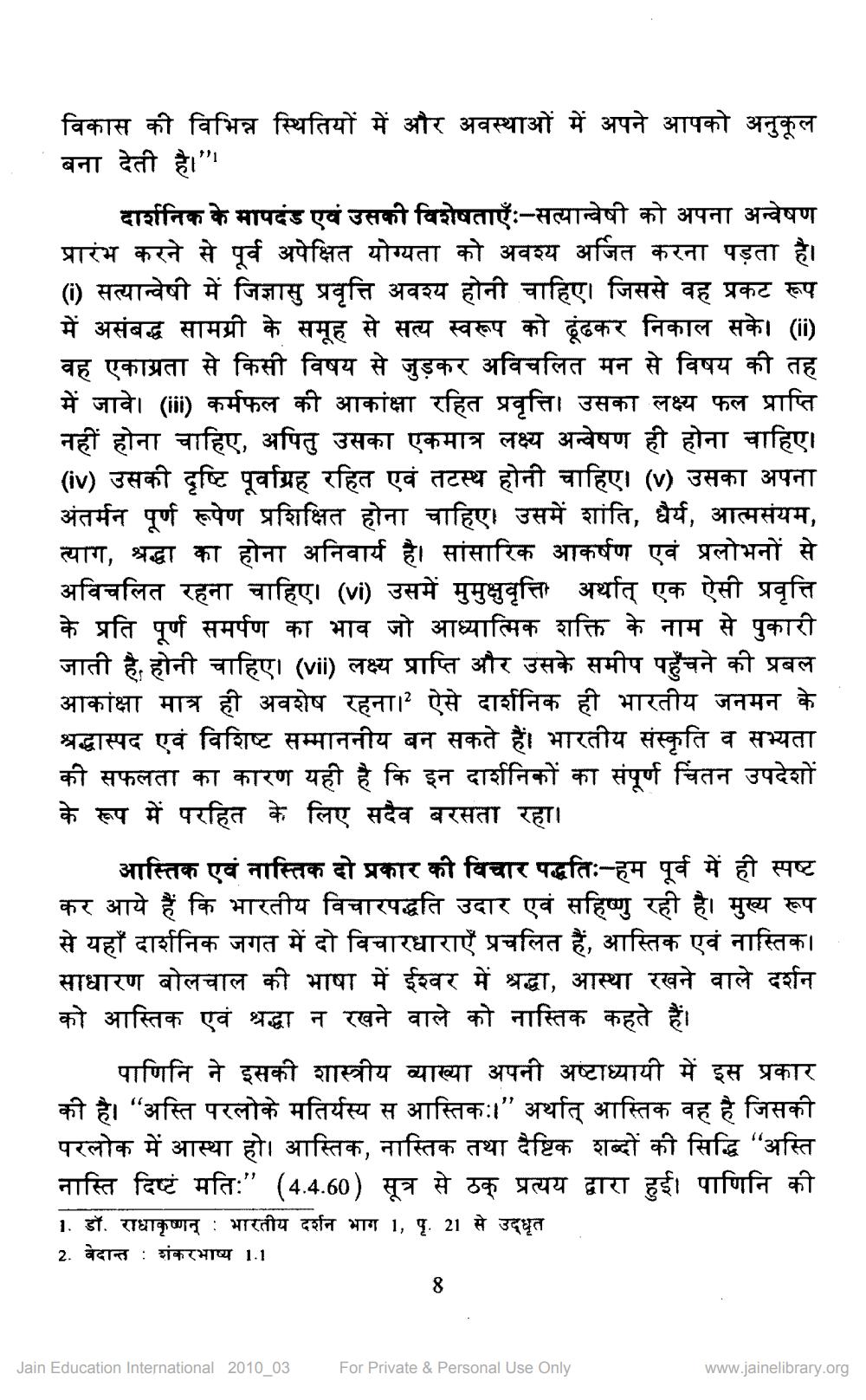________________
विकास की विभिन्न स्थितियों में और अवस्थाओं में अपने आपको अनुकूल बना देती है।"
दार्शनिक के मापदंड एवं उसकी विशेषताएँ:-सत्यान्वेषी को अपना अन्वेषण प्रारंभ करने से पूर्व अपेक्षित योग्यता को अवश्य अर्जित करना पड़ता है। (i) सत्यान्वेषी में जिज्ञासु प्रवृत्ति अवश्य होनी चाहिए। जिससे वह प्रकट रूप में असंबद्ध सामग्री के समूह से सत्य स्वरूप को ढूंढकर निकाल सके। (ii) वह एकाग्रता से किसी विषय से जुड़कर अविचलित मन से विषय की तह में जावे। (iii) कर्मफल की आकांक्षा रहित प्रवृत्ति। उसका लक्ष्य फल प्राप्ति नहीं होना चाहिए, अपितु उसका एकमात्र लक्ष्य अन्वेषण ही होना चाहिए। (iv) उसकी दृष्टि पूर्वाग्रह रहित एवं तटस्थ होनी चाहिए। (v) उसका अपना अंतर्मन पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित होना चाहिए। उसमें शांति, धैर्य, आत्मसंयम, त्याग, श्रद्धा का होना अनिवार्य है। सांसारिक आकर्षण एवं प्रलोभनों से अविचलित रहना चाहिए। (vi) उसमें मुमुक्षुवृत्तिः अर्थात् एक ऐसी प्रवृत्ति के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव जो आध्यात्मिक शक्ति के नाम से पुकारी जाती है, होनी चाहिए। (vii) लक्ष्य प्राप्ति और उसके समीप पहुँचने की प्रबल आकांक्षा मात्र ही अवशेष रहना। ऐसे दार्शनिक ही भारतीय जनमन के श्रद्धास्पद एवं विशिष्ट सम्माननीय बन सकते हैं। भारतीय संस्कृति व सभ्यता की सफलता का कारण यही है कि इन दार्शनिकों का संपूर्ण चिंतन उपदेशों के रूप में परहित के लिए सदैव बरसता रहा।
आस्तिक एवं नास्तिक दो प्रकार की विचार पद्धतिः-हम पूर्व में ही स्पष्ट कर आये हैं कि भारतीय विचारपद्धति उदार एवं सहिष्णु रही है। मुख्य रूप से यहाँ दार्शनिक जगत में दो विचारधाराएँ प्रचलित हैं, आस्तिक एवं नास्तिक। साधारण बोलचाल की भाषा में ईश्वर में श्रद्धा, आस्था रखने वाले दर्शन को आस्तिक एवं श्रद्धा न रखने वाले को नास्तिक कहते हैं।
पाणिनि ने इसकी शास्त्रीय व्याख्या अपनी अष्टाध्यायी में इस प्रकार की है। “अस्ति परलोके मतिर्यस्य स आस्तिकः।" अर्थात् आस्तिक वह है जिसकी परलोक में आस्था हो। आस्तिक, नास्तिक तथा दैष्टिक शब्दों की सिद्धि "अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः” (4.4.60) सूत्र से ठक् प्रत्यय द्वारा हुई। पाणिनि की 1. डॉ. राधाकृष्णन् : भारतीय दर्शन भाग 1, पृ. 21 से उद्धृत 2. वेदान्त : शंकरभाष्य 1.1
8
Jain Education International 2010_03
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org