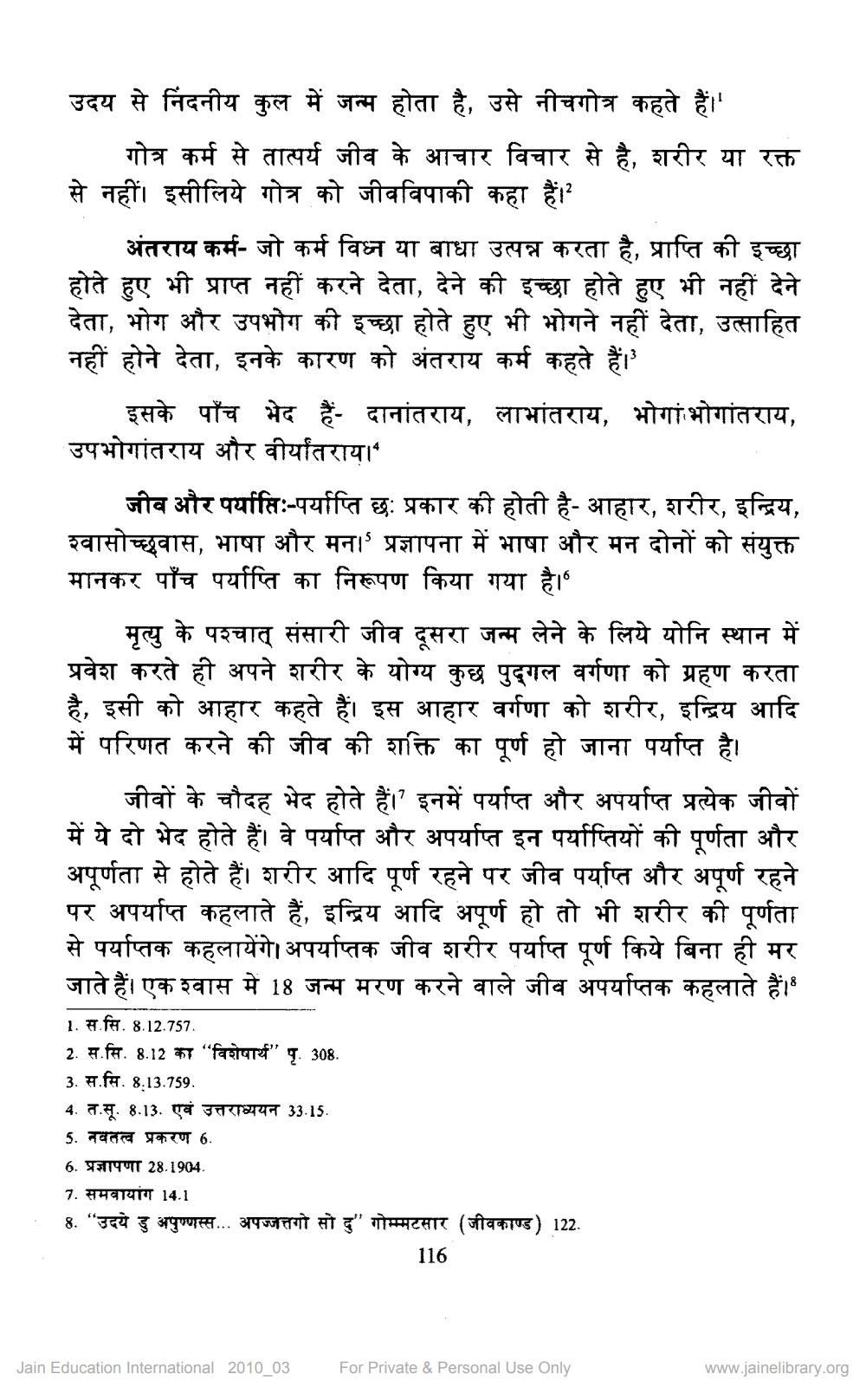________________
उदय से निंदनीय कुल में जन्म होता है, उसे नीचगोत्र कहते हैं।'
गोत्र कर्म से तात्पर्य जीव के आचार विचार से है, शरीर या रक्त से नहीं। इसीलिये गोत्र को जीवविपाकी कहा हैं।
अंतराय कर्म- जो कर्म विन या बाधा उत्पन्न करता है, प्राप्ति की इच्छा होते हुए भी प्राप्त नहीं करने देता, देने की इच्छा होते हुए भी नहीं देने देता, भोग और उपभोग की इच्छा होते हुए भी भोगने नहीं देता, उत्साहित नहीं होने देता, इनके कारण को अंतराय कर्म कहते हैं।'
इसके पाँच भेद हैं- दानांतराय, लाभांतराय, भोगांभोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय।'
जीव और पर्याप्तिः-पर्याप्ति छः प्रकार की होती है- आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन।' प्रज्ञापना में भाषा और मन दोनों को संयुक्त मानकर पाँच पर्याप्ति का निरूपण किया गया है।
मृत्यु के पश्चात् संसारी जीव दूसरा जन्म लेने के लिये योनि स्थान में प्रवेश करते ही अपने शरीर के योग्य कुछ पुद्गल वर्गणा को ग्रहण करता है, इसी को आहार कहते हैं। इस आहार वर्गणा को शरीर, इन्द्रिय आदि में परिणत करने की जीव की शक्ति का पूर्ण हो जाना पर्याप्त है।
जीवों के चौदह भेद होते हैं।' इनमें पर्याप्त और अपर्याप्त प्रत्येक जीवों में ये दो भेद होते हैं। वे पर्याप्त और अपर्याप्त इन पर्याप्तियों की पूर्णता और अपूर्णता से होते हैं। शरीर आदि पूर्ण रहने पर जीव पर्याप्त और अपूर्ण रहने पर अपर्याप्त कहलाते हैं, इन्द्रिय आदि अपूर्ण हो तो भी शरीर की पूर्णता से पर्याप्तक कहलायेंगे। अपर्याप्तक जीव शरीर पर्याप्त पूर्ण किये बिना ही मर जाते हैं। एक श्वास में 18 जन्म मरण करने वाले जीव अपर्याप्तक कहलाते हैं। 1. स.सि. 8.12.757. 2. स.सि. 8.12 का “विशेषार्थ" पृ. 308. 3. स.सि. 8.13.759. 4. त.सू. 8.13. एवं उत्तराध्ययन 33.15. 5. नवतत्त्व प्रकरण 6. 6. प्रज्ञापणा 28.1904. 7. समवायांग 14.1 8. "उदये डु अपुण्णस्स... अपज्जत्तगो सो दु" गोम्मटसार (जीवकाण्ड) 122.
116
Jain Education International 2010_03
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org