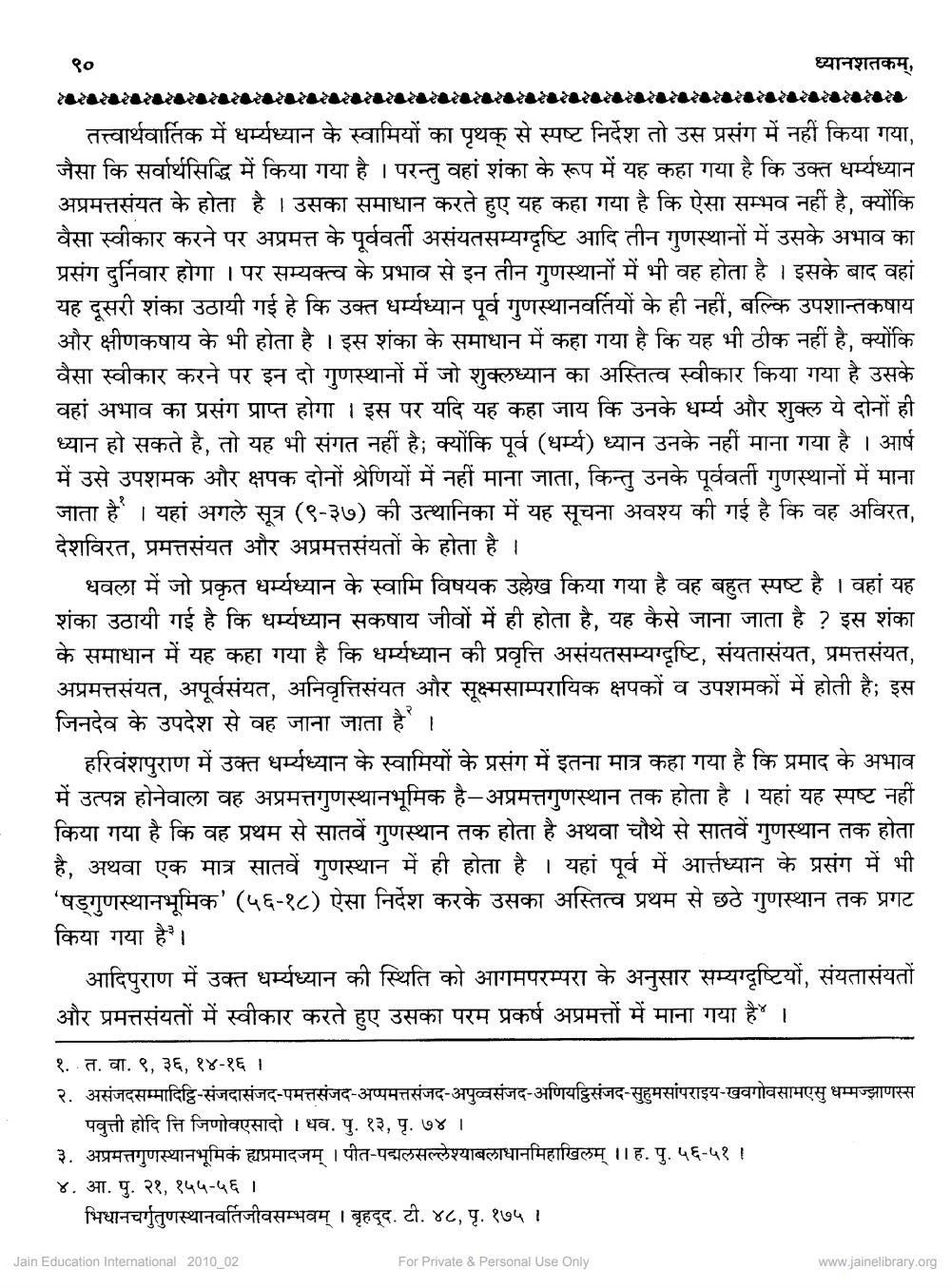________________
९०
ध्यानशतकम्,
तत्त्वार्थवार्तिक में धर्म्यध्यान के स्वामियों का पृथक् से स्पष्ट निर्देश तो उस प्रसंग में नहीं किया गया, जैसा कि सर्वार्थसिद्धि में किया गया है । परन्तु वहां शंका के रूप में यह कहा गया है कि उक्त धर्म्यध्यान अप्रमत्तसंयत के होता है । उसका समाधान करते हुए यह कहा गया है कि ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंकि वैसा स्वीकार करने पर अप्रमत्त के पूर्ववर्ती असंयतसम्यग्दृष्टि आदि तीन गुणस्थानों में उसके अभाव का प्रसंग दुर्निवार होगा । पर सम्यक्त्व के प्रभाव से इन तीन गुणस्थानों में भी वह होता है । इसके बाद वहां यह दूसरी शंका उठायी गई है कि उक्त धर्म्यध्यान पूर्व गुणस्थानवर्तियों के ही नहीं, बल्कि उपशान्तकषाय और क्षीणकषाय के भी होता है । इस शंका के समाधान में कहा गया है कि यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वैसा स्वीकार करने पर इन दो गुणस्थानों में जो शुक्लध्यान का अस्तित्व स्वीकार किया गया है उसके वहां अभाव का प्रसंग प्राप्त होगा । इस पर यदि यह कहा जाय कि उनके धर्म्य और शुक्ल ये दोनों ही ध्यान हो सकते है, तो यह भी संगत नहीं है; क्योंकि पूर्व (धर्म्य) ध्यान उनके नहीं माना गया है । आर्ष में उसे उपशमक और क्षपक दोनों श्रेणियों में नहीं माना जाता, किन्तु उनके पूर्ववर्ती गुणस्थानों में माना जाता है । यहां अगले सूत्र (९-३७) की उत्थानिका में यह सूचना अवश्य की गई है कि वह अविरत, देशविरत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतों के होता है ।
धवला में जो प्रकृत धर्म्यध्यान के स्वामि विषयक उल्लेख किया गया है वह बहुत स्पष्ट है । वहां यह शंका उठायी गई है कि धर्म्यध्यान सकषाय जीवों में ही होता है, यह कैसे जाना जाता है ? इस शंका के समाधान में यह कहा गया है कि धर्म्यध्यान की प्रवृत्ति असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वसंयत, अनिवृत्तिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपकों व उपशमकों में होती है। इस जिनदेव के उपदेश से वह जाना जाता है । __ हरिवंशपुराण में उक्त धर्म्यध्यान के स्वामियों के प्रसंग में इतना मात्र कहा गया है कि प्रमाद के अभाव में उत्पन्न होनेवाला वह अप्रमत्तगुणस्थानभूमिक है-अप्रमत्तगुणस्थान तक होता है । यहां यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह प्रथम से सातवें गुणस्थान तक होता है अथवा चौथे से सातवें गुणस्थान तक होता है, अथवा एक मात्र सातवें गुणस्थान में ही होता है । यहां पूर्व में आर्त्तध्यान के प्रसंग में भी 'षड्गुणस्थानभूमिक' (५६-१८) ऐसा निर्देश करके उसका अस्तित्व प्रथम से छठे गुणस्थान तक प्रगट किया गया है।
आदिपुराण में उक्त धर्म्यध्यान की स्थिति को आगमपरम्परा के अनुसार सम्यग्दृष्टियों, संयतासंयतों और प्रमत्तसंयतों में स्वीकार करते हुए उसका परम प्रकर्ष अप्रमत्तों में माना गया है ।
१. त. वा. ९, ३६, १४-१६ । २. असंजदसम्मादिट्ठि-संजदासंजद-पमत्तसंजद-अप्पमत्तसंजद-अपव्वसंजद-अणियट्ठिसंजद-सुहमसांपराइय-खवगोवसामएस धम्मज्झाणस्स ___पवुत्ती होदि त्ति जिणोवएसादो । धव. पु. १३, पृ. ७४ ।। ३. अप्रमत्तगुणस्थानभूमिकं ह्यप्रमादजम् । पीत-पद्मलसल्लेश्याबलाधानमिहाखिलम् ।। ह. पु. ५६-५१ । ४. आ. पु. २१, १५५-५६ ।
भिधानचर्गुतुणस्थानवर्तिजीवसम्भवम् । बृहद्द. टी. ४८, पृ. १७५ ।
Jain Education International 2010_02
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org