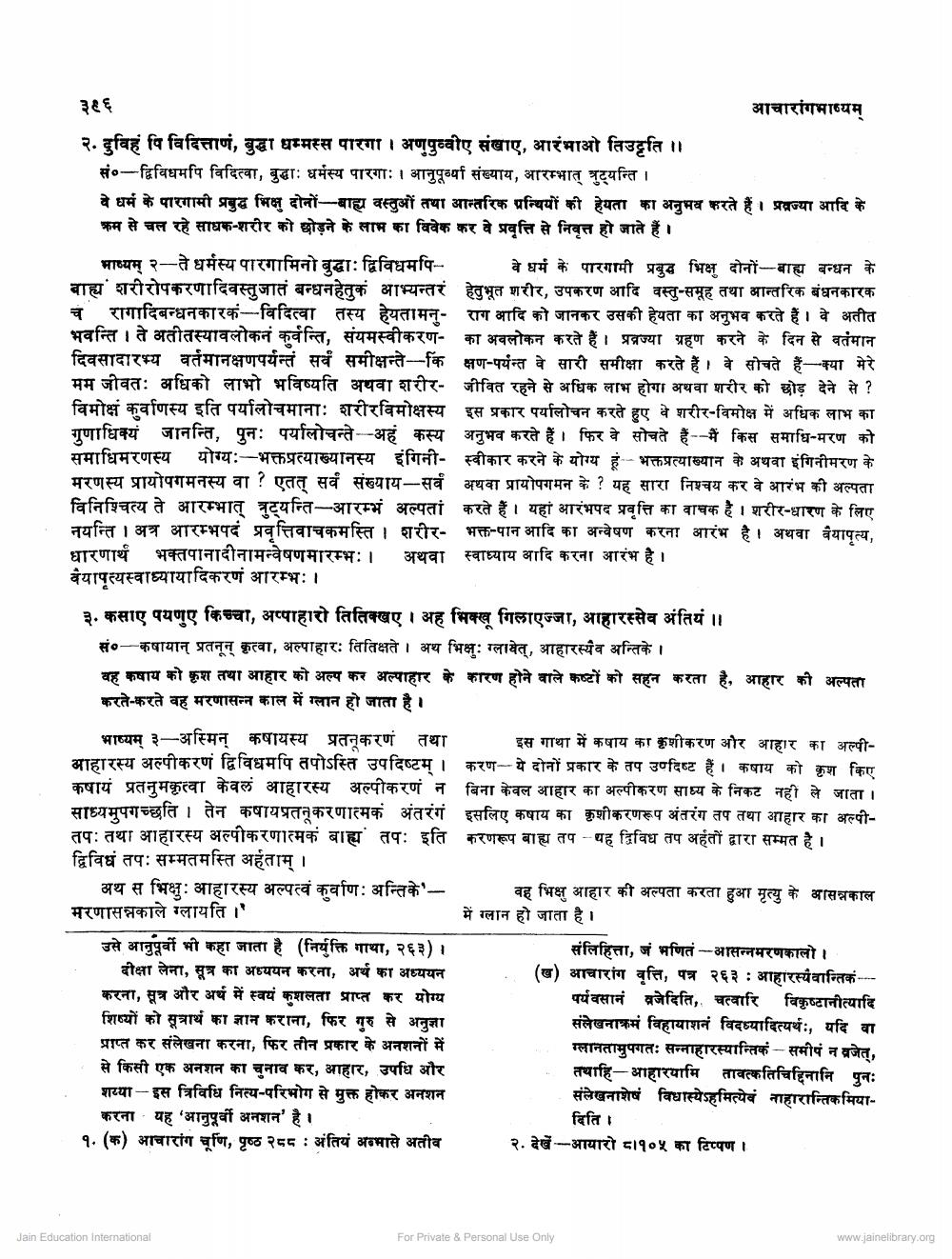________________
३६६
आचारांगभाष्यम् २. दुविहं पि विदित्ताणं, बुद्धा धम्मस्स पारगा। अणुपुवीए संखाए, आरंभाओ तिउति ॥ सं०-द्विविधमपि विदित्वा, बुद्धाः धर्मस्य पारगाः । आनुपूर्दा संख्याय, आरम्भात् त्रुट्यन्ति । वे धर्म के पारगामी प्रबुद्ध भिक्षु दोनों-बाह्य वस्तुओं तथा आन्तरिक प्रन्थियों की हेयता का अनुभव करते हैं। प्रव्रज्या आदि के क्रम से चल रहे साधक-शरीर को छोड़ने के लाभ का विवेक कर वे प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाते हैं।
भाष्यम् २–ते धर्मस्य पारगामिनो बुद्धाः द्विविधमपि- वे धर्म के पारगामी प्रबुद्ध भिक्षु दोनों-बाह्य बन्धन के बाह्य शरीरोपकरणादिवस्तुजातं बन्धनहेतुकं आभ्यन्तरं हेतुभूत शरीर, उपकरण आदि वस्तु-समूह तथा आन्तरिक बंधनकारक च रागादिबन्धनकारक-विदित्वा तस्य हेयतामनु- राग आदि को जानकर उसकी हेयता का अनुभव करते हैं। वे अतीत भवन्ति । ते अतीतस्यावलोकनं कुर्वन्ति, संयमस्वीकरण- का अवलोकन करते हैं। प्रव्रज्या ग्रहण करने के दिन से वर्तमान दिवसादारभ्य वर्तमानक्षणपर्यन्तं सर्व समीक्षन्ते-कि क्षण-पर्यन्त वे सारी समीक्षा करते हैं। वे सोचते हैं- क्या मेरे मम जीवतः अधिको लाभो भविष्यति अथवा शरीर- जीवित रहने से अधिक लाभ होगा अथवा शरीर को छोड़ देने से ? विमोक्षं कुर्वाणस्य इति पर्यालोचमानाः शरीरविमोक्षस्य इस प्रकार पर्यालोचन करते हुए वे शरीर-विमोक्ष में अधिक लाभ का गुणाधिक्यं जानन्ति, पुन: पर्यालोचन्ते-अहं कस्य अनुभव करते हैं। फिर वे सोचते हैं-मैं किस समाधि-मरण को समाधिमरणस्य योग्य:-भक्तप्रत्याख्यानस्य इंगिनी- स्वीकार करने के योग्य हूं- भक्तप्रत्याख्यान के अथवा इंगिनीमरण के मरणस्य प्रायोपगमनस्य वा? एतत् सर्वं संख्याय-सर्व अथवा प्रायोपगमन के ? यह सारा निश्चय कर वे आरंभ की अल्पता विनिश्चित्य ते आरम्भात् त्रुट्यन्ति-आरम्भं अल्पतां करते हैं। यहां आरंभपद प्रवृत्ति का वाचक है । शरीर-धारण के लिए नयन्ति । अत्र आरम्भपदं प्रवृत्तिवाचकमस्ति । शरीर- भक्त-पान आदि का अन्वेषण करना आरंभ है। अथवा वैयापृत्य, धारणार्थ भक्तपानादीनामन्वेषणमारम्भः। अथवा स्वाध्याय आदि करना आरंभ है। वैयापत्यस्वाध्यायादिकरणं आरम्भः । ३. कसाए पयणुए किच्चा, अप्पाहारो तितिक्खए । अह भिक्खू गिलाएज्जा, आहारस्सेव अंतियं ।। सं०-कषायान प्रतनून् कृत्वा, अल्पाहारः तितिक्षते । अथ भिक्षुः ग्लादेत्, आहारस्यैव अन्तिके । वह कषाय को कृश तथा आहार को अल्प कर अल्पाहार के कारण होने वाले कष्टों को सहन करता है, आहार की अल्पता करते-करते वह मरणासन्न काल में ग्लान हो जाता है।
भाष्यम् ३–अस्मिन् कषायस्य प्रतनकरणं तथा इस गाथा में कषाय का कृशीकरण और आहार का अल्पीआहारस्य अल्पीकरणं द्विविधमपि तपोऽस्ति उपदिष्टम् । करण-ये दोनों प्रकार के तप उदिष्ट हैं। कषाय को कृश किए कषायं प्रतनुमकृत्वा केवलं आहारस्य अल्पीकरणं न बिना केवल आहार का अल्पीकरण साध्य के निकट नहीं ले जाता। साध्यमुपगच्छति । तेन कषायप्रतनुकरणात्मक अंतरंगं इसलिए कषाय का कृशीकरणरूप अंतरंग तप तथा आहार का अल्पीतपः तथा आहारस्य अल्पीकरणात्मकं बाह्य तपः इति करणरूप बाह्य तप - यह द्विविध तप अर्हतों द्वारा सम्मत है । द्विविधं तपः सम्मतमस्ति अर्हताम् ।
अथ स भिक्षुः आहारस्य अल्पत्वं कुर्वाणः अन्तिके'- वह भिक्षु आहार की अल्पता करता हुआ मृत्यु के आसन्नकाल मरणासन्नकाले ग्लायति ।।
में ग्लान हो जाता है। उसे आनुपूर्वी भी कहा जाता है (नियुक्ति गाथा, २६३)।
संलिहित्ता, जं भणितं-आसन्नमरणकालो।। दीक्षा लेना, सूत्र का अध्ययन करना, अर्थ का अध्ययन (ख) आचारांग वृत्ति, पत्र २६३ : आहारस्यैवान्तिक---- करना, सूत्र और अर्थ में स्वयं कुशलता प्राप्त कर योग्य
पर्यवसानं व्रजेदिति, चत्वारि विकृष्टानीत्यादि शिष्यों को सूत्रार्थ का ज्ञान कराना, फिर गुरु से अनुज्ञा
संलेखनाक्रमं विहायाशनं विदध्यादित्यर्थः, यदि वा प्राप्त कर संलेखना करना, फिर तीन प्रकार के अनशनों में
ग्लानतामुपगतः सन्नाहारस्यान्तिक-समीपं न व्रजेत्, से किसी एक अनशन का चुनाव कर, आहार, उपधि और
तथाहि-आहारयामि तावत्कतिचिद्दिनानि पुनः शय्या- इस त्रिविधि नित्य-परिभोग से मुक्त होकर अनशन
संलेखनाशेषं विधास्येऽहमित्येवं नाहारान्तिकमियाकरना यह 'आनुपूर्वी अनशन' है।
दिति। १. (क) आचारांग चूणि, पृष्ठ २८८ : अंतियं अम्भासे अतीव २.देखें-आयारो ८।१०५ का टिप्पण ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org