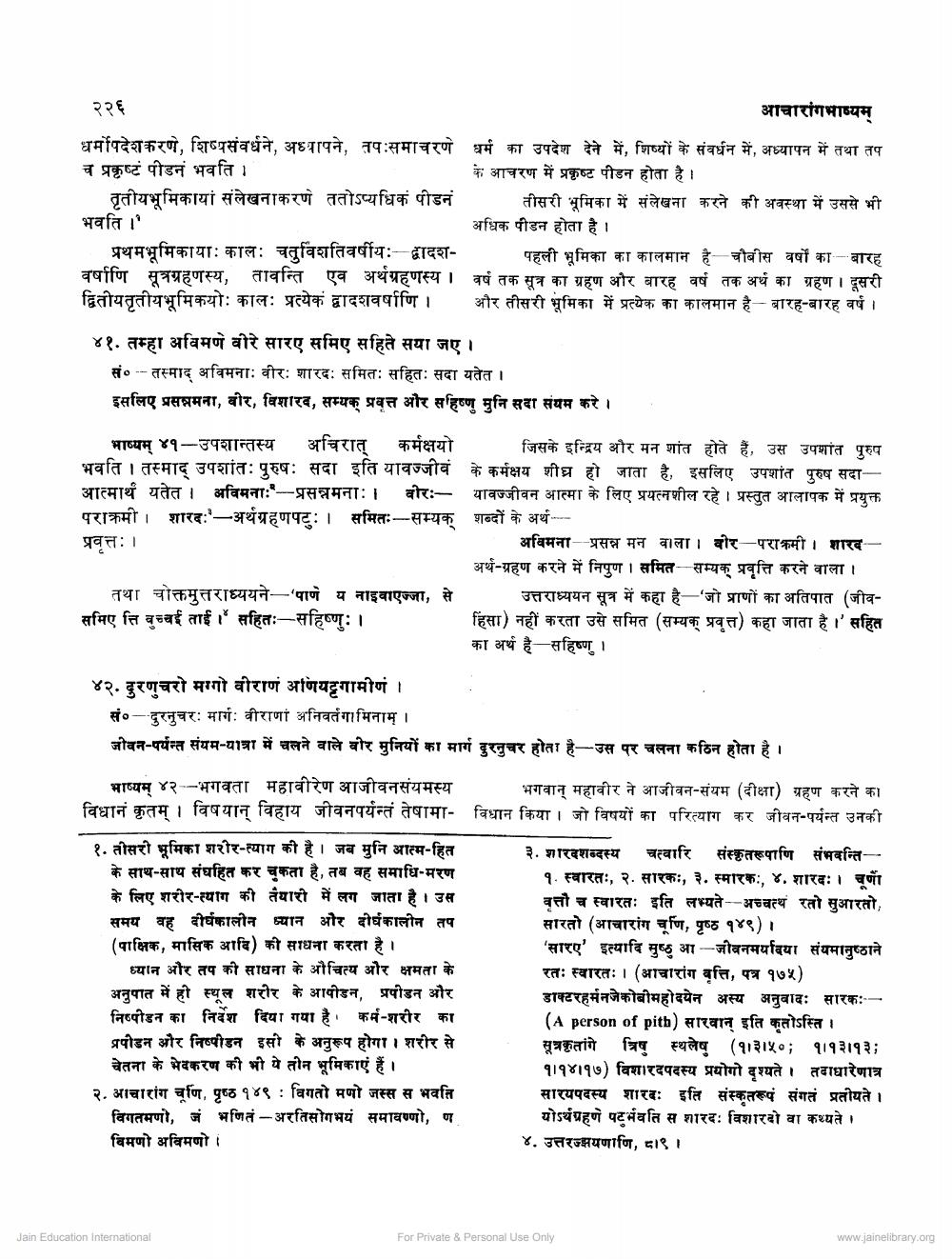________________
२२६
आचारांगभाष्यम् धर्मोपदेशकरणे, शिष्यसंवर्धने, अध्यापने, तपःसमाचरणे धर्म का उपदेश देने में, शिष्यों के संवर्धन में, अध्यापन में तथा तप च प्रकृष्टं पीडनं भवति ।
__ के आचरण में प्रकृष्ट पीडन होता है। तृतीयभूमिकायां संलेखनाकरणे ततोऽप्यधिक पीडनं तीसरी भूमिका में संलेखना करने की अवस्था में उससे भी भवति ।
अधिक पीडन होता है। प्रथमभूमिकायाः काल: चतुविशतिवर्षीयः द्वादश- पहली भूमिका का कालमान है-चौबीस वर्षों का-बारह वर्षाणि सूत्रग्रहणस्य, तावन्ति एव अर्थग्रहणस्य। वर्ष तक सूत्र का ग्रहण और बारह वर्ष तक अर्थ का ग्रहण । दूसरी द्वितीयतृतीयभूमिकयोः कालः प्रत्येक द्वादशवर्षाणि। और तीसरी भूमिका में प्रत्येक का कालमान है- बारह-बारह वर्ष ।
४१. तम्हा अविमणे वीरे सारए समिए सहिते सया जए। सं० -- तस्माद् अविमनाः वीरः शारदः समितः सहितः सदा यतेत । इसलिए प्रसन्नमना, वीर, विशारद, सम्यक् प्रवृत्त और सहिष्णु मुनि सदा संयम करे।
भाष्यम् ४१-उपशान्तस्य अचिरात् कर्मक्षयो जिसके इन्द्रिय और मन शांत होते हैं, उस उपशांत पुरुष भवति । तस्माद उपशांतः पुरुषः सदा इति यावज्जीवं के कर्मक्षय शीघ्र हो जाता है, इसलिए उपशांत पुरुष सदाआत्मार्थं यतेत । अविमनाः-प्रसन्नमनाः। वीरः- यावज्जीवन आत्मा के लिए प्रयत्नशील रहे । प्रस्तुत आलापक में प्रयुक्त पराक्रमी। शारदः'-अर्थग्रहणपटुः । समितः--सम्यक् शब्दों के अर्थ ---- प्रवृत्तः।
अविमना प्रसन्न मन वाला। वीर-पराक्रमी। शारद
अर्थ-ग्रहण करने में निपुण । समित–सम्यक् प्रवृत्ति करने वाला। तथा चोक्तमुत्तराध्ययने–'पाणे य नाइवाएज्जा, से उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है-'जो प्राणों का अतिपात (जीवसमिए ति बुच्चई ताई। सहितः-सहिष्णुः ।
हिंसा) नहीं करता उसे समित (सम्यक् प्रवृत्त) कहा जाता है।' सहित का अर्थ है–सहिष्णु ।
४२. दुरणुचरो मग्गो वीराणं अणियट्रगामीणं । सं०-दुरनुचरः मार्गः वीराणां अनिवर्तगामिनाम् । जीवन-पर्यन्त संयम-यात्रा में चलने वाले वीर मुनियों का मार्ग दुरनुचर होता है-उस पर चलना कठिन होता है ।
भाष्यम ४२-भगवता महावीरेण आजीवनसंयमस्य भगवान् महावीर ने आजीवन-संयम (दीक्षा) ग्रहण करने का विधानं कतम । विषयान विहाय जीवनपर्यन्तं तेषामा- विधान किया। जो विषयों का परित्याग कर जीवन-पर्यन्त उनकी
-
१. तीसरी भूमिका शरीर-त्याग की है। जब मुनि आत्म-हित
के साथ-साथ संघहित कर चुकता है, तब वह समाधि-मरण के लिए शरीर-त्याग की तैयारी में लग जाता है । उस समय वह दीर्घकालीन ध्यान और दीर्घकालीन तप (पाक्षिक, मासिक आदि) की साधना करता है।
ध्यान और तप की साधना के औचित्य और क्षमता के अनुपात में ही स्थूल शरीर के आपीडन, प्रपीडन और निष्पीडन का निर्देश दिया गया है। कर्म-शरीर का प्रपीडन और निष्पीडन इसी के अनुरूप होगा। शरीर से
चेतना के भेदकरण की भी ये तीन भूमिकाएं हैं। २. आचारांग चूणि, पृष्ठ १४९ : विगतो मणो जस्स स भवति विगतमणो, जं भणितं -अरतिसोगभयं समावण्णो, ण विमणो अविमणो।
३. शारदशब्दस्य चत्वारि संस्कृतरूपाणि संभवन्ति
१. स्वारतः, २. सारकः, ३. स्मारकः, ४. शारदः। चूर्णी वत्तौ च स्वारतः इति लभ्यते--अच्चत्य रतो सुआरतो, सारतो (आचारांग चूणि, पृष्ठ १४९)। 'सारए' इत्यादि मुष्ठ आ-जीवनमर्यादया संयमानुष्ठाने रतः स्वारतः । (आचारांग वृत्ति, पत्र १७५) डाक्टरहर्मनजेकोबीमहोदयेन अस्य अनुवादः सारकः-- (A person of pith) सारवान् इति कृतोऽस्ति । सूत्रकृतांगे त्रिषु स्थलेषु (१।३।५०; १।१३।१३, १।१४।१७) विशारदपदस्य प्रयोगो दृश्यते। तवाधारेणात्र सारयपदस्य शारदः इति संस्कृतरूपं संगतं प्रतीयते।
योऽर्थग्रहणे पटुर्भवति स शारदः विशारदो वा कथ्यते । ४. उत्तरज्झयणाणि, ८९ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org