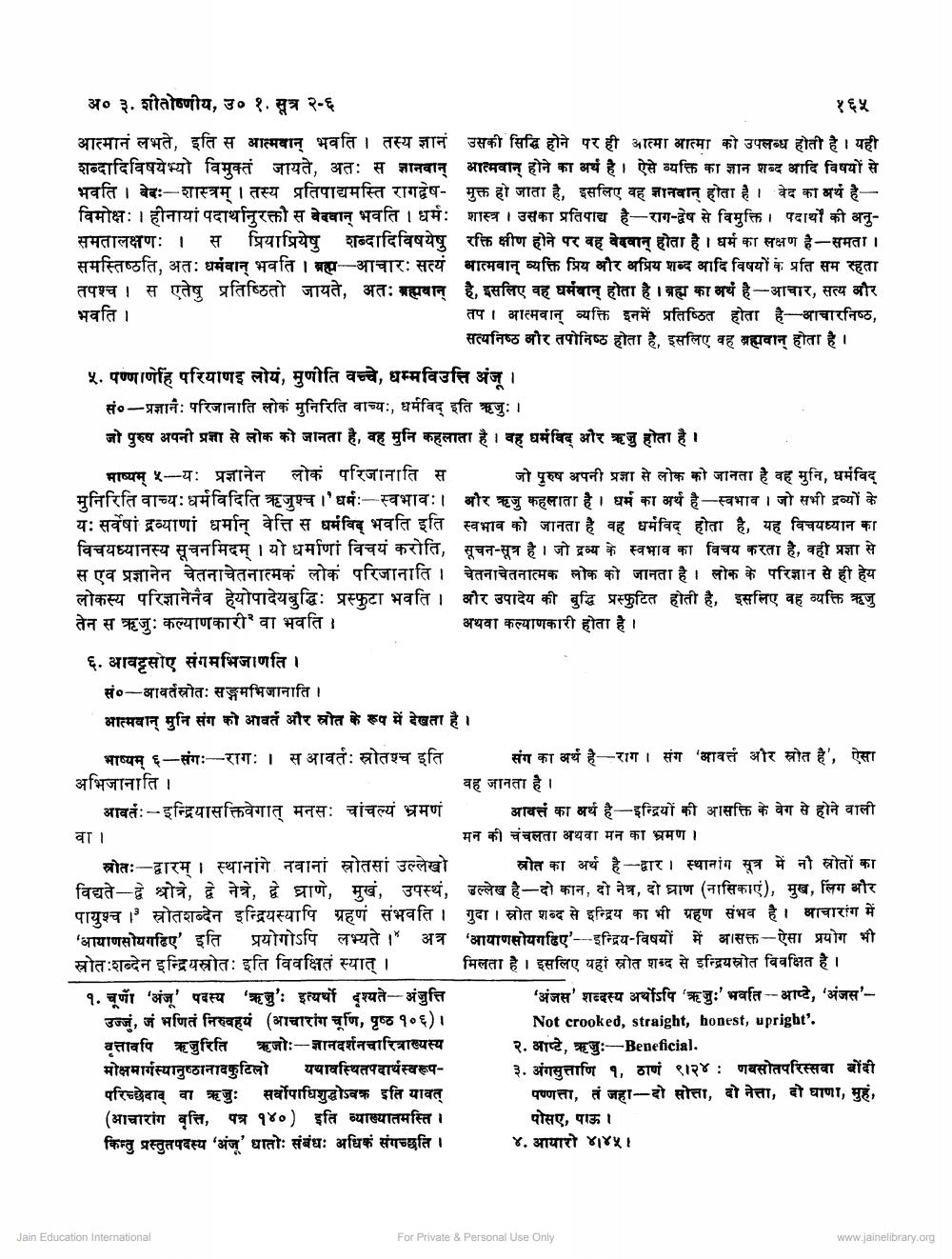________________
अ० ३. शीतोष्णीय, उ० १. सूत्र २०६
आत्मानं लभते इति स आत्मवान् भवति । तस्य ज्ञानं शब्दादिविषयेभ्यो विमुक्र्त जायते, अतः स ज्ञानवान् भवति । वेब:- शास्त्रम् । तस्य प्रतिपाद्यमस्ति रागद्वेष विमोक्षः । हीनायां पदार्थानुरक्तौ स वेदवान् भवति । धर्मः समतालक्षणः । स प्रियाप्रियेषु शब्दादिविषयेषु समस्तिष्ठति, अतः धर्मवान् भवति । ब्रह्म-आचारः सत्यं तपश्च । स एतेषु प्रतिष्ठितो जायते, अतः ब्रह्मवान् भवति ।
५. पण हि परियाणा लोयं, मुनीति बच्चे, धम्मविउत्ति अंजू । सं० - प्रज्ञानः परिजानाति लोकं मुनिरिति वाच्यः, धर्मविद् इति ऋजुः ।
जो पुरुष अपनी प्रज्ञा से लोक को जानता है, यह मुनि कहलाता है। वह धर्मविद और ऋतु होता है।
भाष्यम् ५ - यः प्रज्ञानेन लोकं परिजानाति स मुनिरिति वाच्यः धर्मविदिति ऋजुश्च ।' धर्मः - स्वभावः । यः सर्वेषां द्रव्याणां धर्मान् वेत्ति स धर्मवित् भवति इति विचयध्यानस्य सूचनमिदम् । यो धर्माणां विचयं करोति, स एव प्रज्ञानेन चेतनाचेतनात्मकं लोकं परिजानाति । लोकस्य परिज्ञानेनैव हेयोपादेयबुद्धिः प्रस्फुटा भवति । तेन स ऋजु कल्याणकारी' वा भवति ।
स्रोतः- द्वारम् । स्थानांगे नवानां स्रोतसां उल्लेखो विद्यते – द्वे श्रोत्रे, द्वे नेत्रे, द्वे घ्राणे, मुखं उपस्थं, पायुश्च । स्रोतशब्देन इन्द्रियस्यापि ग्रहणं संभवति । 'आयाणसोयगढिए' इति प्रयोगोऽपि लभ्यते ।" अत्र स्रोतः शब्देन इन्द्रियस्रोतः इति विवक्षितं स्यात् ।
१६५ उसकी सिद्धि होने पर ही आत्मा आत्मा को उपलब्ध होती है । यही आत्मवान् होने का अर्थ है। ऐसे व्यक्ति का ज्ञान शब्द आदि विषयों से मुक्त हो जाता है, इसलिए वह ज्ञानवान होता है। वेद का अर्थ हैशास्त्र । उसका प्रतिपाद्य है - राग-द्वेष से विमुक्ति । पदार्थों की अनुरक्ति क्षीण होने पर वह वेदवान् होता है। धर्म का सक्षम है-समता मात्मवान् व्यक्ति प्रिय और अत्रिय शब्द आदि विषयों के प्रति सम रहता है, इसलिए वह धर्मवान् होता है । ब्रह्म का अर्थ है - आचार, सत्य और तप । आत्मवान् व्यक्ति इनमें प्रतिष्ठित होता है- आचारनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ होता है, इसलिए वह ब्रह्मवान् होता है ।
६. आवसोए संगमभिजाणति ।
सं० - आवर्तस्रोतः सङ्गमभिजानाति ।
आत्मवान् मुनि संग को आवर्त और स्रोत के रूप में देखता है। भाष्यम् ६ – संगः-- रागः । स आवर्तः स्रोतश्च इति अभिजानाति ।
आवर्त इन्द्रियासक्तिवेगात् मनसः चांचल्यं भ्रमण
वा ।
१. चूणा 'अंजू' पदस्य 'ऋजु' इत्यर्थो दृश्यते-- अंजुत्ति उज्जुं, जं भणितं निश्वयं ( आचारांग चूर्णि, पृष्ठ १०६ ) । वृत्तावधि ऋतुरिति ऋजो:- ज्ञानदर्शनचारित्राख्यस्य मोक्षमार्गस्यानुष्ठानाकुटिलो यथावस्थितपदार्थ स्वरूपपरिषदान् वा ऋः सर्वोपाधिशुद्धोऽयक इति यावत् ( आचारांग वृति पत्र १४० ) इति व्याख्यातमस्ति । किन्तु प्रस्तुतपदस्य 'अंजू' धातोः संबंध अधिक संगति ।
Jain Education International
जो पुरुष 'अपनी प्रज्ञा से लोक को जानता है वह मुनि, धर्मविद् और ऋजु कहलाता है। धर्म का अर्थ है – स्वभाव । जो सभी द्रव्यों के स्वभाव को जानता है वह धर्मविद होता है, यह विचपध्यान का सूचन-सूत्र है । जो द्रव्य के स्वभाव का विचय करता है, वही प्रज्ञा से चेतनाचेतनात्मक लोक को जानता है । लोक के परिज्ञान से ही हे और उपादेय की बुद्धि प्रस्फुटित होती है, इसलिए वह व्यक्ति ऋजु अथवा कल्याणकारी होता है।
संग का अर्थ है- राग संग 'आवर्त और स्रोत है', ऐसा वह जानता है ।
आवतं का अर्थ है - इन्द्रियों की आसक्ति के वेग से होने वाली मन की चंचलता अथवा मन का भ्रमण ।
स्रोत का अर्थ है -द्वार स्थानांग सूत्र में नौ स्रोतों का उल्लेख है - दो कान, दो नेत्र, दो घ्राण (नासिकाएं), मुख, लिंग और गुदा स्रोत शब्द से इन्द्रिय का भी ग्रहण संभव है। आचारांग में 'आयाणसोयगढिए ' --- इन्द्रिय विषयों में आसक्त - ऐसा प्रयोग भी मिलता है। इसलिए यहां स्रोत शब्द से इन्द्रियस्रोत विवक्षित है ।
'अंजस' शब्दस्य अर्थोऽपि ऋजुः' अर्थात आप्टे, 'मंजस'Not crooked, straight, honest, upright'. २. आप्टे, ऋजु :- Beneficial.
३. अंगसुत्ताणि १, ठाणं ९२४ : णवसोतपरिस्सवा बोंदी पण्णत्ता, तं जहा- दो सोत्ता, दो नेत्ता, दो घाणा, मुहं, पोसए, पाऊ ।
४. आयारो ४ । ४५ ।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org