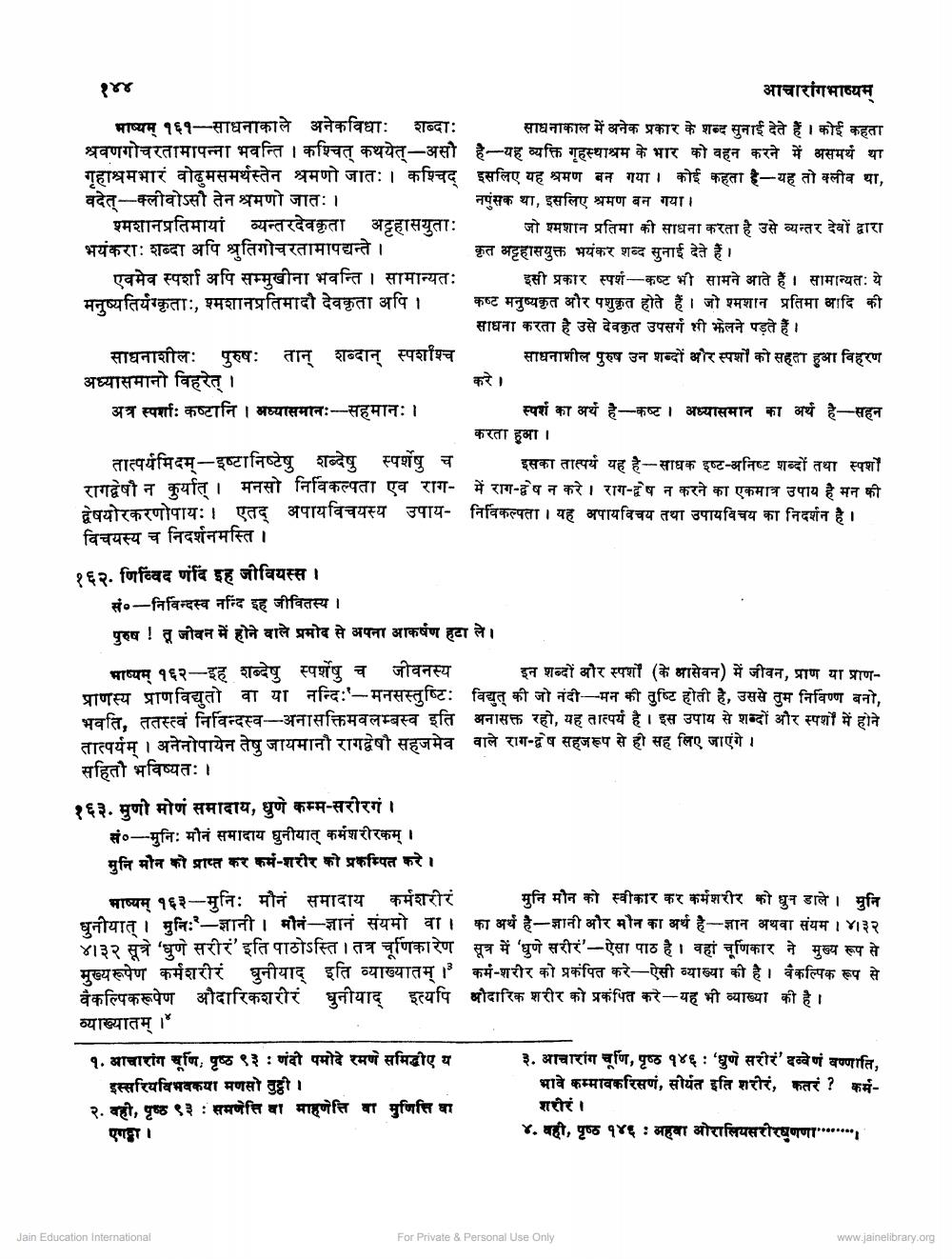________________
न
आचारांगभाष्यम् भाष्यम् १६१-साधनाकाले अनेकविधाः शब्दाः साधनाकाल में अनेक प्रकार के शब्द सुनाई देते हैं । कोई कहता श्रवणगोचरतामापन्ना भवन्ति । कश्चित् कथयेत्-असौ है-यह व्यक्ति गृहस्थाश्रम के भार को वहन करने में असमर्थ था गहाश्रमभारं वोढमसमर्थस्तेन श्रमणो जातः । कश्चिद् इसलिए यह श्रमण बन गया। कोई कहता है-यह तो क्लीव था, वदेत्-क्लीवोऽसौ तेन श्रमणो जातः ।
नपुंसक था, इसलिए श्रमण बन गया। श्मशानप्रतिमायां व्यन्तरदेवकृता अट्टहासयुताः जो श्मशान प्रतिमा की साधना करता है उसे व्यन्तर देवों द्वारा भयंकराः शब्दा अपि श्रुतिगोचरतामापद्यन्ते।
कृत अट्टहासयुक्त भयंकर शब्द सुनाई देते हैं। ___ एवमेव स्पर्शा अपि सम्मुखीना भवन्ति । सामान्यतः इसी प्रकार स्पर्श-कष्ट भी सामने आते हैं। सामान्यतः ये मनुष्यतिर्यग्कृताः, श्मशानप्रतिमादौ देवकृता अपि । कष्ट मनुष्यकृत और पशुकृत होते हैं। जो श्मशान प्रतिमा आदि की
साधना करता है उसे देवकृत उपसर्ग भी झेलने पड़ते हैं। साधनाशीलः पुरुषः तान् शब्दान् स्पश्चि साधनाशील पुरुष उन शब्दों और स्पर्शो को सहता हुआ विहरण अध्यासमानो विहरेत् ।
करे। अत्र स्पर्शाः कष्टानि । मध्यासमानः-सहमानः ।
स्पर्श का अर्थ है-कष्ट । अध्यासमान का अर्थ है-सहन
करता हुआ। तात्पर्यमिदम्-इष्टानिष्टेषु शब्देषु स्पर्शेषु च इसका तात्पर्य यह है-साधक इष्ट-अनिष्ट शब्दों तथा स्पर्शी रागद्वेषौ न कुर्यात । मनसो निविकल्पता एव राग- में राग-द्वेष न करे । राग-द्वेष न करने का एकमात्र उपाय है मन की देखोरकरणोपायः। एतद अपायविचयस्य उपाय- निर्विकल्पता। यह अपाय विचय तथा उपायविचय का निदर्शन है। विचयस्य च निदर्शनमस्ति । १६२. णिव्विद दि इह जीवियस्स।
सं०-निविन्दस्व नन्दि इह जीवितस्य । पुरुष ! तू जीवन में होने वाले प्रमोद से अपना आकर्षण हटा ले।
भाष्यम १६२-इह शब्देषु स्पर्शेषु च जीवनस्य इन शब्दों और स्पों (के मासेवन) में जीवन, प्राण या प्राणप्राणस्य प्राणविद्युतो वा या नन्दिः-मनसस्तुष्टिः विद्युत् की जो नंदी-मन की तुष्टि होती है, उससे तुम निविण्ण बनो, भवति. ततस्त्वं निविन्दस्व-अनासक्तिमवलम्बस्व इति अनासक्त रहो, यह तात्पर्य है । इस उपाय से शब्दों और स्पों में होने तात्पर्यम् । अनेनोपायेन तेषु जायमानौ रागद्वेषौ सहजमेव वाले राग-द्वेष सहजरूप से ही सह लिए जाएंगे। सहितौ भविष्यतः। १६३. मुणी मोणं समादाय, धुणे कम्म-सरीरगं ।
सं०--मुनिः मौनं समादाय धुनीयात् कर्मशरीरकम् । मुनि मौन को प्राप्त कर कर्म-शरीर को प्रकम्पित करे।
भाष्यम १६३-मुनिः मौनं समादाय कर्मशरीरं मुनि मौन को स्वीकार कर कर्मशरीर को धुन डाले। मुनि धनीयात । मुनिः-ज्ञानी। मौनं-ज्ञानं संयमो वा। का अर्थ है-ज्ञानी और मौन का अर्थ है-ज्ञान अथवा संयम । ४।३२ ४।३२ सत्रे 'धूणे सरीरं' इति पाठोऽस्ति । तत्र चूर्णिकारेण सूत्र में 'धुणे सरीरं'-ऐसा पाठ है। वहां चूर्णिकार ने मुख्य रूप से मुख्यरूपेण कर्मशरीरं धुनीयाद् इति व्याख्यातम्। कर्म-शरीर को प्रकंपित करे-ऐसी व्याख्या की है। वैकल्पिक रूप से वैकल्पिकरूपेण औदारिकशरीरं धुनीयाद् इत्यपि औदारिक शरीर को प्रकंपित करे-यह भी व्याख्या की है। व्याख्यातम् । १. आचारांग चूणि, पृष्ठ ९३ : गंदी पमोदे रमणे समितीए य ३. आचारांग चूणि, पृष्ठ १४६ : 'धुणे सरीरं' दम्वेणं वण्णाति, इस्सरियविभवकया मणसो तुट्ठी।।
भावे कम्मावकरिसणं, सीर्यत इति शरीरं, कतरं? कर्म२. वही, पृष्ठ ९३ : समणेत्ति वा माहणेत्ति वा मुणिति वा
शरीरं। एगा ।
४. वही, पृष्ठ १४६ : महवा ओरालियसरीरघुणणा.......।
Jain Education international
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org