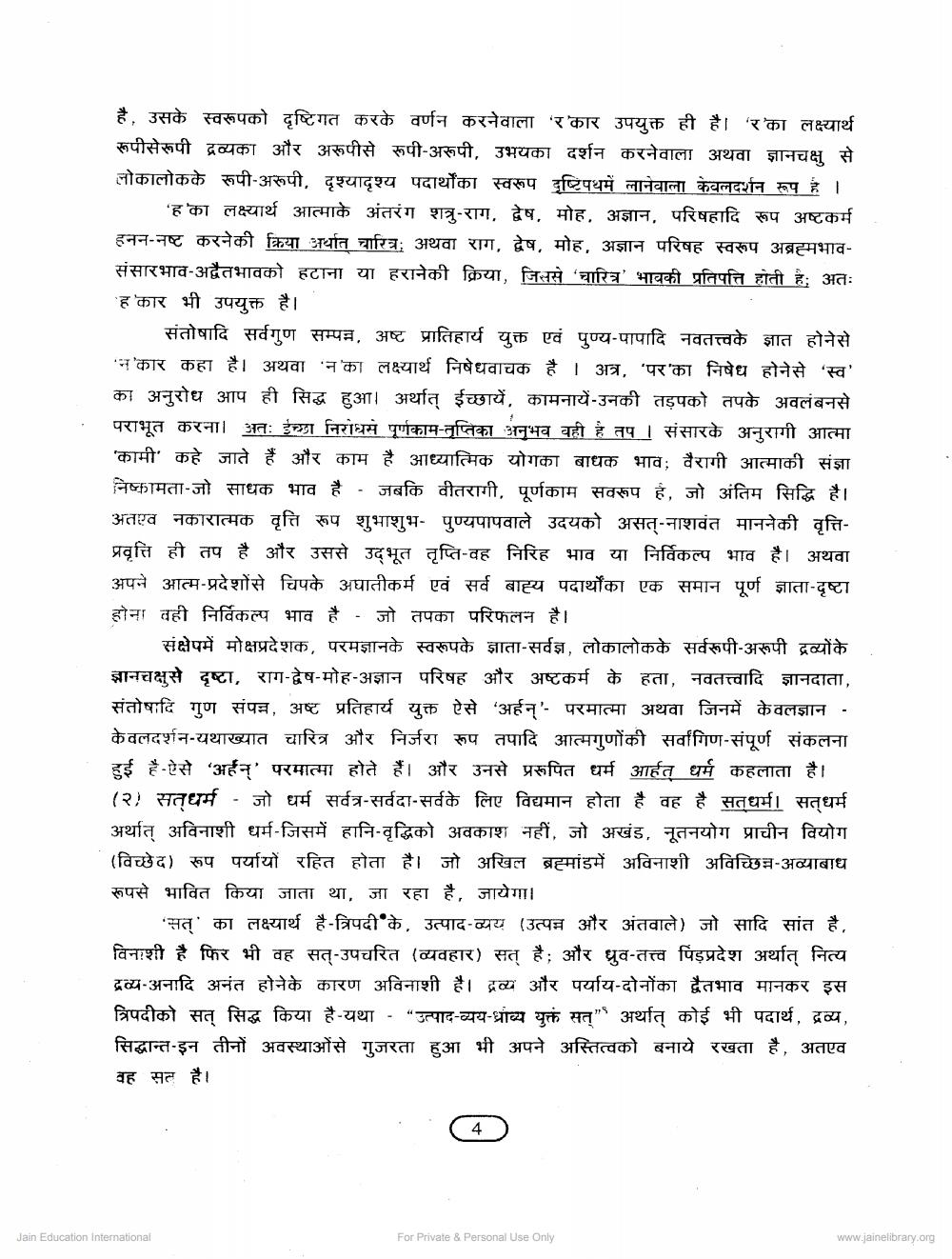________________
है, उसके स्वरूपको दृष्टिगत करके वर्णन करनेवाला 'रकार उपयुक्त ही है। 'रका लक्ष्यार्थ रूपीसेरूपी द्रव्यका और अरूपीसे रूपी अरूपी उभयका दर्शन करनेवाला अथवा ज्ञानचक्षु से लोकालोकके रूपी अरूपी, दृश्यादृश्य पदार्थोंका स्वरूप दृष्टिपथमें लानेवाला केवलदर्शन रूप है ।
'ह'का लक्ष्यार्थ आत्माके अंतरंग शत्रु-राग, द्वेष, मोह, अज्ञान परिषहादि रूप अष्टकर्म हनन नष्ट करने की क्रिया अर्थात चारित्र अथवा राग, द्वेष, मोह, अज्ञान परिषह स्वरूप अब्रह्मभावसंसारभाव अद्वैतभावको हटाना या हरानेकी क्रिया, जिससे 'चारित्र' भावकी प्रतिपत्ति होती है अतः हकार भी उपयुक्त है।
संतोषादि सर्वगुण सम्पन्न अष्ट प्रातिहार्य युक्त एवं पुण्य-पापादि नवतत्त्वके ज्ञात होनेसे 'न'कार कहा है। अथवा न का लक्ष्यार्थ निषेधवाचक है । अत्र 'पर'का निषेध होनेसे 'स्व' का अनुरोध आप ही सिद्ध हुआ । अर्थात् ईच्छायें, कामनायें उनकी तड़पको तपके अवलंबनसे पराभूत करना। अतः ईच्छा निरोधसे पूर्णकाम-तृप्तिका अनुभव वही हे तप संसारके अनुरागी आत्मा 'कामी' कहे जाते हैं और काम है आध्यात्मिक योगका बाधक भाव वैरागी आत्माकी संज्ञा निष्कामता जो साधक भाव है जबकि वीतरागी, पूर्णकाम सवरूप है, जो अंतिम सिद्धि है। अतश्व नकारात्मक वृत्ति रूप शुभाशुभ पुण्यपापवाले उदयको असत् नाशवंत माननेकी वृत्तिप्रवृत्ति ही तप है और उससे उद्भूत तृप्ति वह निरिह भाव या निर्विकल्प भाव है अथवा अपने आत्म प्रदेशों से चिपके अघातीकर्म एवं सर्व बाह्य पदार्थोंका एक समान पूर्ण ज्ञाता दृष्टा होना नहीं निर्विकल्प भाव है जो तपका परिफलन है।
"
संक्षेपमें मोक्षप्रदेशक, परमज्ञानके स्वरूपके ज्ञाता सर्वज्ञ, लोकालोकके सर्वरूपी अरूपी द्रव्यों के ज्ञानचक्षुसे दृष्टा, राग-द्वेष- मोह-अज्ञान परिषह और अष्टकर्म के हता, नवतत्त्वादि ज्ञानदाता, संतोषादि गुण संपन्न, अष्ट प्रतिहार्य युक्त ऐसे 'अर्हन्'- परमात्मा अथवा जिनमें केवलज्ञान केवलदर्शन यथाख्यात चारित्र और निर्जरा रूप तपादि आत्मगुणोंकी सर्वांगिण संपूर्ण संकलना हुई है - ऐसे 'अन्' परमात्मा होते हैं। और उनसे प्ररूपित धर्म आर्हत् धर्म कहलाता है। (२) सत्धर्म जो धर्म सर्वत्र सर्वदा सर्वके लिए विद्यमान होता है वह है सत्धर्म। सत्धर्म अर्थात् अविनाशी धर्म- जिसमें हानि-वृद्धिको अवकाश नहीं, जो अखंड, नूतनयोग प्राचीन वियोग (विच्छेद) रूप पर्यायों रहित होता है। जो अखिल ब्रह्मांडमें अविनाशी अविच्छिन्न अव्याबाध रूपसे भावित किया जाता था, जा रहा है, जायेगा ।
Jain Education International
'सत्' का लक्ष्यार्थ है - त्रिपदी के उत्पाद-व्यय ( उत्पन्न और अंतवाले) जो सादि सांत है, विनाशी है फिर भी वह सत् - उपचरित (व्यवहार) सत् है; और ध्रुव-तत्त्व पिंड़प्रदेश अर्थात् नित्य द्रव्य अनादि अनंत होनेके कारण अविनाशी है। द्रव्य और पर्याय दोनोंका द्वैतभाव मानकर इस त्रिपदीको सत् सिद्ध किया है यथा- "उत्पाद व्यय प्राच्य युक्तं सत्" अर्थात् कोई भी पदार्थ, द्रव्य, सिद्धान्त- इन तीनों अवस्थाओंसे गुजरता हुआ भी अपने अस्तित्वको बनाये रखता है, अतएव वह सत है।
4
·
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org