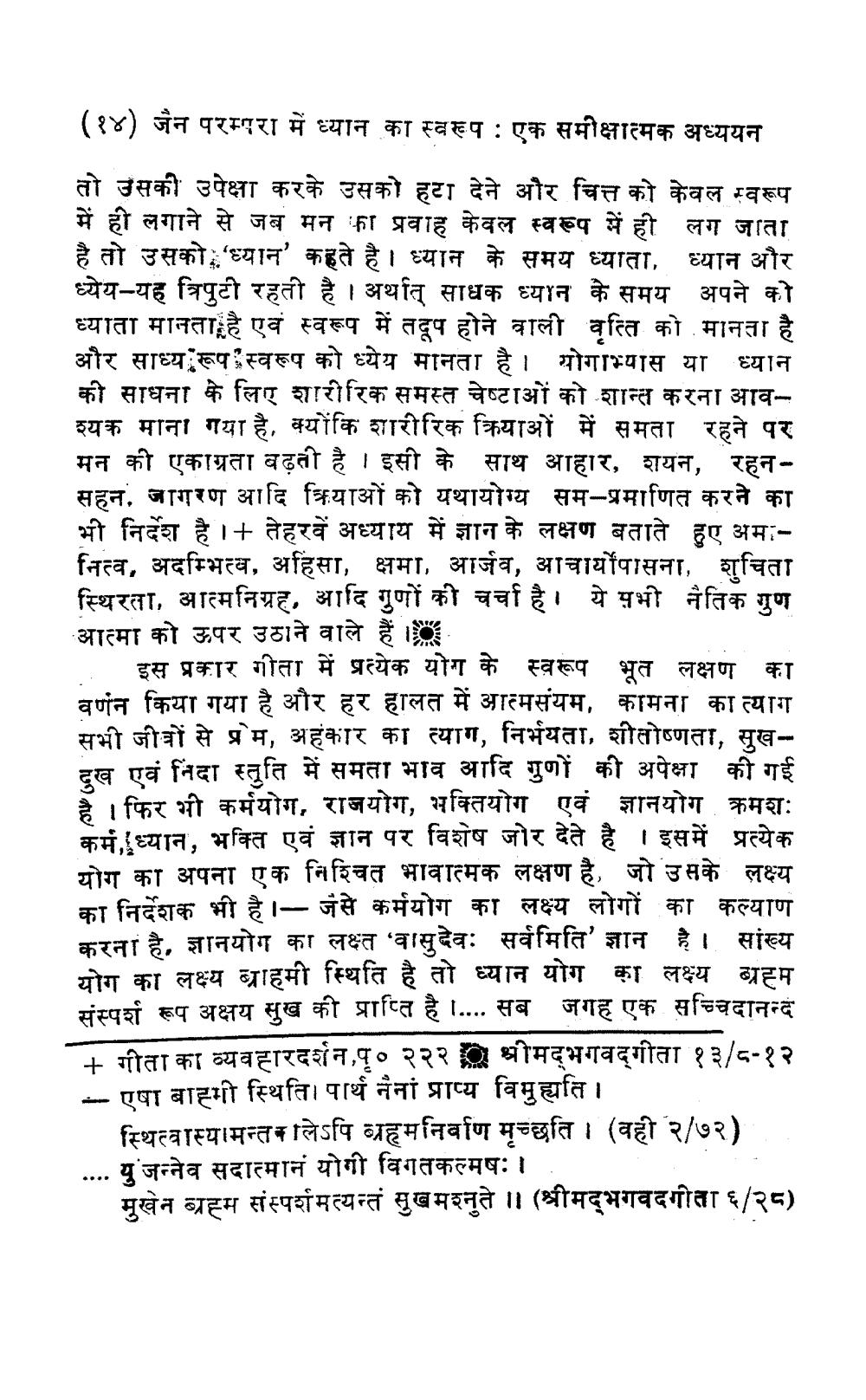________________
(१४) जैन परम्परा में ध्यान का स्वरूप : एक समीक्षात्मक अध्ययन
तो उसकी उपेक्षा करके उसको हटा देने और चित्त को केवल स्वरूप में ही लगाने से जब मन का प्रवाह केवल स्वरूप में ही लग जाता है तो उसको 'ध्यान' कहते है। ध्यान के समय ध्याता, ध्यान और ध्येय-यह त्रिपुटी रहती है । अर्थात् साधक ध्यान के समय अपने को ध्याता मानता है एवं स्वरूप में तदूप होने वाली वृत्ति को मानता है और साध्य रूप स्वरूप को ध्येय मानता है। योगाभ्यास या ध्यान की साधना के लिए शारीरिक समस्त चेष्टाओं को शान्त करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि शारीरिक क्रियाओं में समता रहने पर मन की एकाग्रता बढ़ती है । इसी के साथ आहार, शयन, रहनसहन, जागरण आदि क्रियाओं को यथायोग्य सम-प्रमाणित करने का भी निर्देश है।+ तेहरवें अध्याय में ज्ञान के लक्षण बताते हुए अमःनित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षमा, आर्जव, आचार्योपासना, शुचिता स्थिरता, आत्मनिग्रह, आदि गुणों की चर्चा है। ये सभी नैतिक गुण आत्मा को ऊपर उठाने वाले हैं ।
इस प्रकार गीता में प्रत्येक योग के स्वरूप भूत लक्षण का वर्णन किया गया है और हर हालत में आत्मसंयम, कामना का त्याग सभी जीवों से प्रेम, अहंकार का त्याग, निर्भयता, शीतोष्णता, सुखदुख एवं निंदा स्तुति में समता भाव आदि गुणों की अपेक्षा की गई
फिर भी कर्मयोग, राजयोग, भक्तियोग एवं ज्ञानयोग क्रमशः कर्म, ध्यान, भक्ति एवं ज्ञान पर विशेष जोर देते है । इसमें प्रत्येक योग का अपना एक निश्चित भावात्मक लक्षण है, जो उसके लक्ष्य का निर्देशक भी है।- जैसे कर्मयोग का लक्ष्य लोगों का कल्याण करना है, ज्ञानयोग का लक्ष्त 'वासुदेवः सर्वमिति' ज्ञान है। सांख्य योग का लक्ष्य प्राहमी स्थिति है तो ध्यान योग का लक्ष्य अहम संस्पर्श रूप अक्षय सुख की प्राप्ति है ।.... सब जगह एक सच्चिदानन्द + गीता का व्यवहारदर्शन,पृ० २२२ । श्रीमद्भगवद्गीता १३/८-१२ -- एषा बाह्मी स्थिति। पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।
स्थित्वास्यामन्तमलेिऽपि अहम निर्वाण मृच्छति । (वही २/७२). .... युजन्नेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः ।
मुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ।। (श्रीमद्भगवदगीता ६/२८)