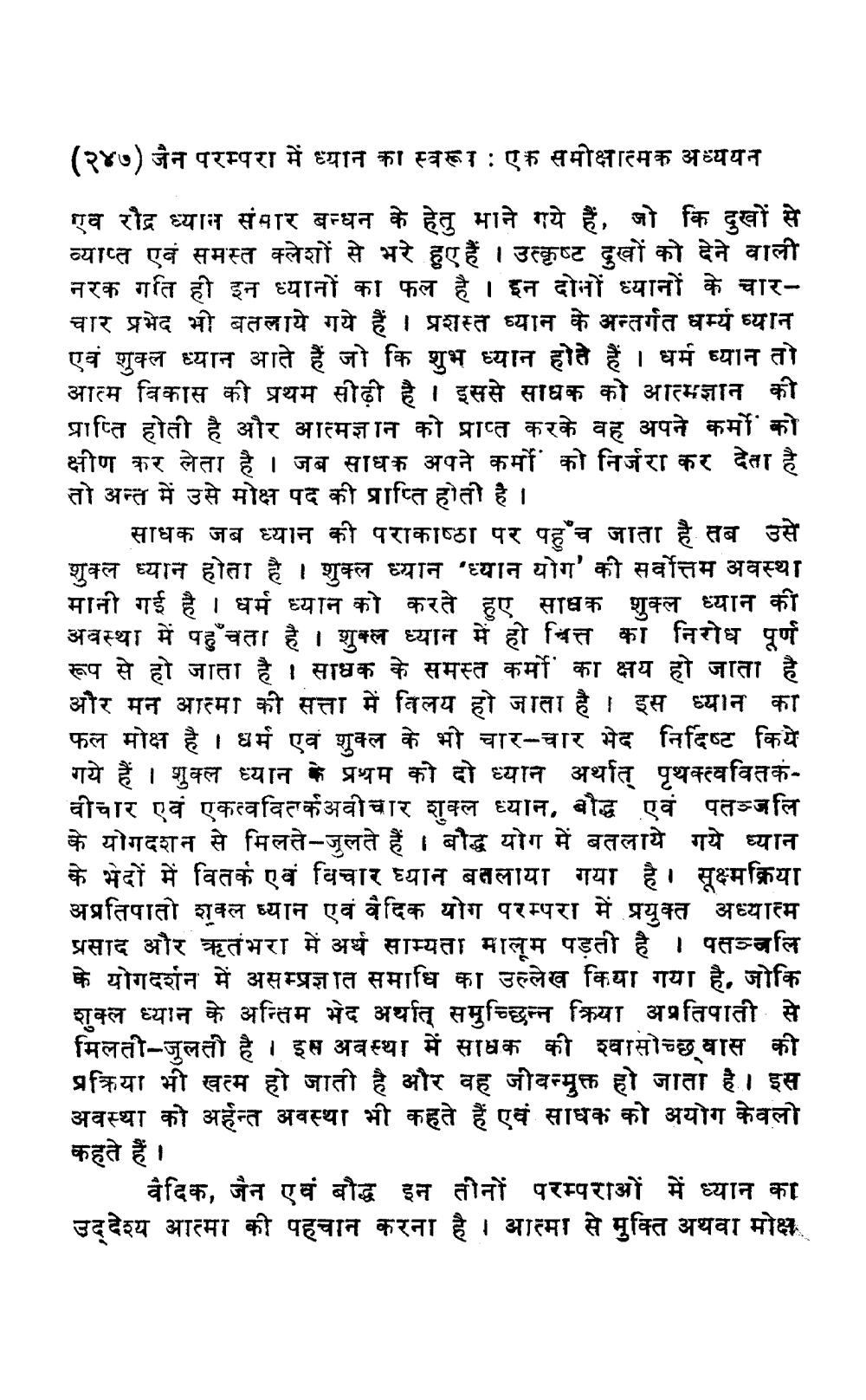________________
(२४७) जैन परम्परा में ध्यान का स्वरूप : एक समीक्षात्मक अध्ययन
एव रौद्र ध्यान संसार बन्धन के हेतु माने गये हैं, जो कि दुखों से व्याप्त एवं समस्त क्लेशों से भरे हुए हैं । उत्कृष्ट दुखों को देने वाली नरक गति ही इन ध्यानों का फल है । इन दोनों ध्यानों के चारचार प्रभेद भी बतलाये गये हैं । प्रशस्त ध्यान के अन्तर्गत धर्म्य ध्यान एवं शुक्ल ध्यान आते हैं जो कि शुभ ध्यान होते हैं । धर्म ध्यान तो आत्म विकास की प्रथम सीढ़ी है । इससे साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्मज्ञान को प्राप्त करके वह अपने कर्मों को क्षीण कर लेता है । जब साधक अपने कर्मों को निर्जरा कर देता है तो अन्त में उसे मोक्ष पद की प्राप्ति होती है ।
साधक जब ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है तब उसे शुक्ल ध्यान होता है । शुक्ल ध्यान "ध्यान योग' की सर्वोत्तम अवस्था मानी गई है । धर्म ध्यान को करते हुए साधक शुक्ल ध्यान की अवस्था में पहुँचता है । शुक्ल ध्यान में हो वित्त का निरोध पूर्ण रूप से हो जाता है । साधक के समस्त कर्मो का क्षय हो जाता है और मन आत्मा की सत्ता में विलय हो जाता है । इस ध्यान का फल मोक्ष है । धर्म एवं शुक्ल के भी चार-चार भेद निर्दिष्ट किये गये हैं । शुक्ल ध्यान के प्रथम को दो ध्यान अर्थात् पृथक्त्ववितकंवीचार एवं एकत्ववितर्कअवीचार शुक्ल ध्यान, बौद्ध एवं पतञ्जलि के योगदशन से मिलते-जुलते हैं । बौद्ध योग में बतलाये गये ध्यान के भेदों में वितर्क एवं विचार ध्यान बतलाया गया है। सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान एवं वैदिक योग परम्परा में प्रयुक्त अध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा में अर्थ साम्यता मालूम पड़ती है । पतञ्जलि के योगदर्शन में असम्प्रज्ञात समाधि का उल्लेख किया गया है, जोकि शुक्ल ध्यान के अन्तिम भेद अर्थात् समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती से मिलती-जुलती है । इस अवस्था में साधक की श्वासोच्छ् वास की प्रक्रिया भी खत्म हो जाती है और वह जीवन्मुक्त हो जाता है । इस अवस्था को अर्हन्त अवस्था भी कहते हैं एवं साधक को अयोग केवलो कहते हैं । वैदिक, जैन एवं बौद्ध इन तीनों परम्पराओं में ध्यान का उद्देश्य आत्मा की पहचान करना है । आत्मा से मुक्ति अथवा मोक्ष