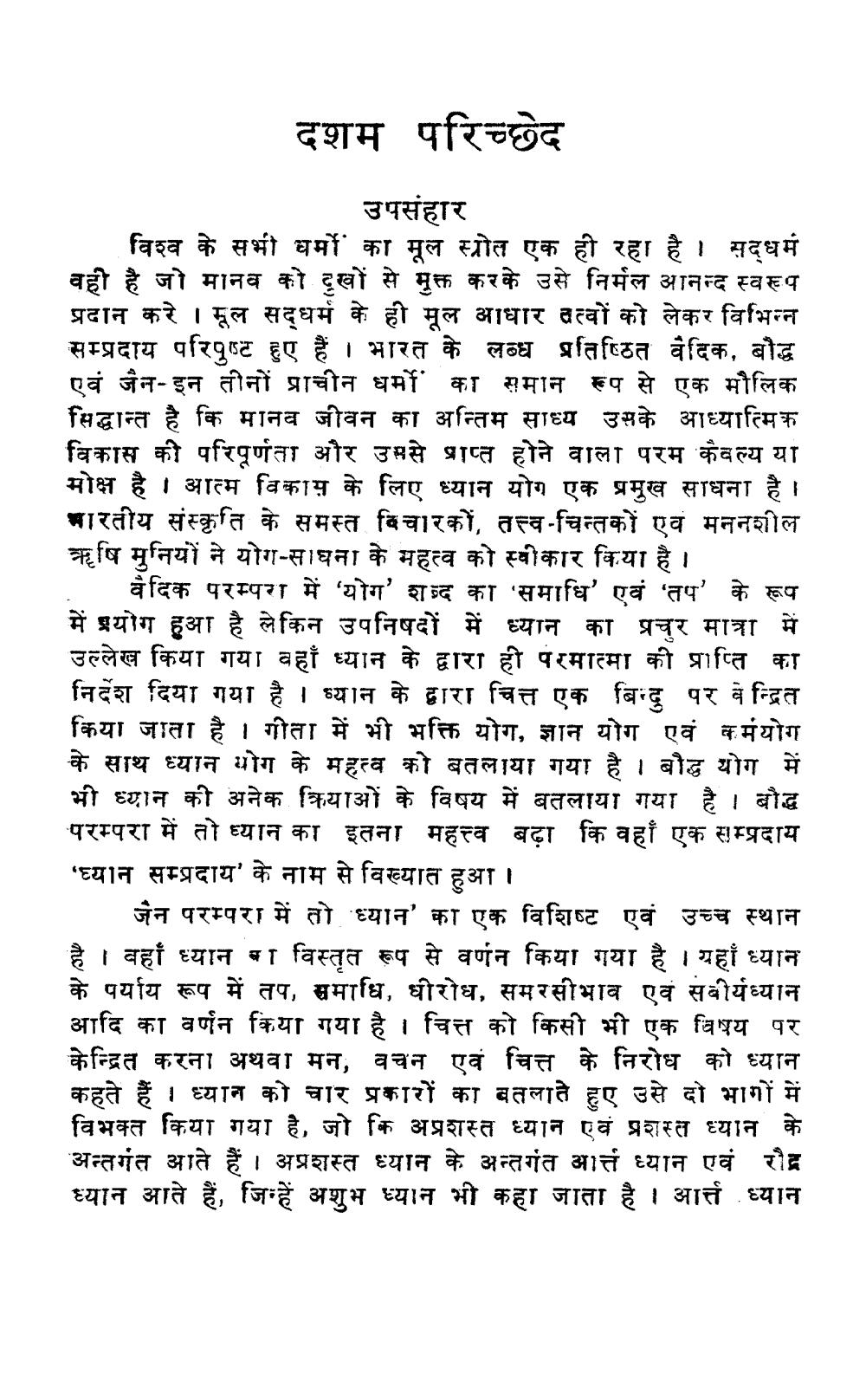________________
दशम परिच्छेद
उपसंहार विश्व के सभी धर्मों का मूल स्त्रोत एक ही रहा है। सद्धमं वही है जो मानव को दुखों से मुक्त करके उसे निर्मल आनन्द स्वरूप प्रदान करे । मूल सद्धर्म के ही मूल आधार तत्वों को लेकर विभिन्न सम्प्रदाय परिपूष्ट हुए हैं । भारत के लब्ध प्रतिष्ठित वैदिक, बौद्ध एवं जैन- इन तीनों प्राचीन धर्मो का समान रूप से एक मौलिक सिद्धान्त है कि मानव जीवन का अन्तिम साध्य उसके आध्यात्मिक विकास की परिपूर्णता और उससे प्राप्त होने वाला परम कैवल्य या मोक्ष है । आत्म विकास के लिए ध्यान योग एक प्रमुख साधना है। भारतीय संस्कृति के समस्त विचारकों, तत्त्व-चिन्तकों एवं मननशील ऋषि मुनियों ने योग-साधना के महत्व को स्वीकार किया है। . वैदिक परम्परा में 'योग' शब्द का 'समाधि' एवं 'तप' के रूप में प्रयोग हुआ है लेकिन उपनिषदों में ध्यान का प्रचुर मात्रा में उल्लेख किया गया वहाँ ध्यान के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति का निर्देश दिया गया है । ध्यान के द्वारा चित्त एक बिन्दु पर वेन्द्रित किया जाता है । गीता में भी भक्ति योग, ज्ञान योग एवं कर्मयोग के साथ ध्यान योग के महत्व को बतलाया गया है । बौद्ध योग में भी ध्यान की अनेक क्रियाओं के विषय में बतलाया गया है। बौद्ध परम्परा में तो ध्यान का इतना महत्त्व बढ़ा कि वहाँ एक सम्प्रदाय 'ध्यान सम्प्रदाय' के नाम से विख्यात हुआ।
__ जैन परम्परा में तो ध्यान' का एक विशिष्ट एवं उच्च स्थान है । वहाँ ध्यान का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है । यहाँ ध्यान के पर्याय रूप में तप, समाधि, धीरोध, समरसीभाव एवं सबीर्यध्यान आदि का वर्णन किया गया है । चित्त को किसी भी एक विषय पर केन्द्रित करना अथवा मन, वचन एवं चित्त के निरोध को ध्यान कहते हैं । ध्यान को चार प्रकारों का बतलाते हुए उसे दो भागों में विभक्त किया गया है, जो कि अप्रशस्त ध्यान एवं प्रशस्त ध्यान के अन्तर्गत आते हैं। अप्रशस्त ध्यान के अन्तर्गत आत ध्यान एवं रौद्र ध्यान आते हैं, जिन्हें अशुभ ध्यान भी कहा जाता है । आर्त ध्यान