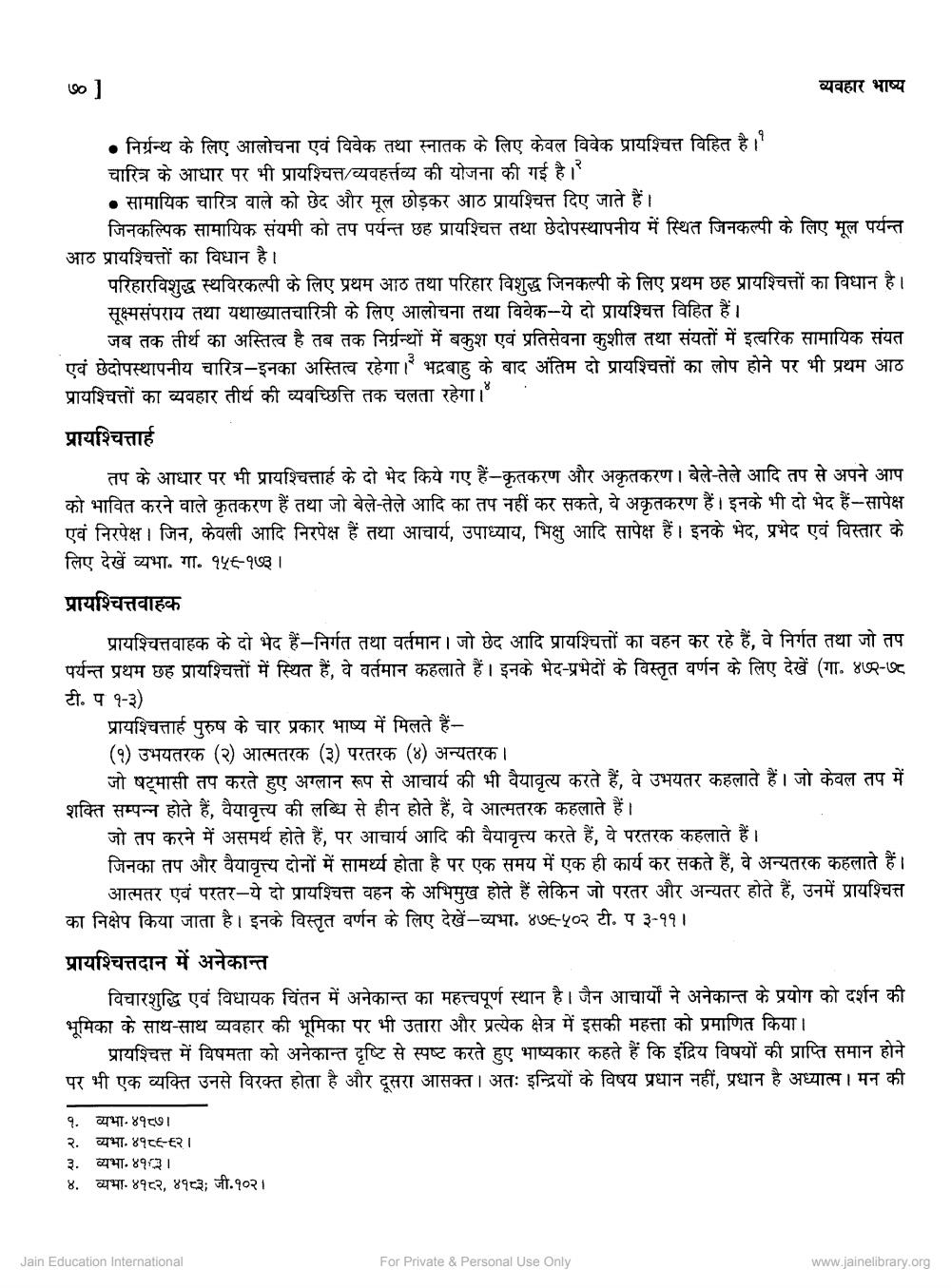________________
७]
व्यवहार भाष्य
• निर्ग्रन्थ के लिए आलोचना एवं विवेक तथा स्नातक के लिए केवल विवेक प्रायश्चित्त विहित है।' चारित्र के आधार पर भी प्रायश्चित्त/व्यवहर्त्तव्य की योजना की गई है। • सामायिक चारित्र वाले को छेद और मूल छोड़कर आठ प्रायश्चित्त दिए जाते हैं।
जिनकल्पिक सामायिक संयमी को तप पर्यन्त छह प्रायश्चित्त तथा छेदोपस्थापनीय में स्थित जिनकल्पी के लिए मूल पर्यन्त आठ प्रायश्चित्तों का विधान है।
परिहारविशुद्ध स्थविरकल्पी के लिए प्रथम आठ तथा परिहार विशुद्ध जिनकल्पी के लिए प्रथम छह प्रायश्चित्तों का विधान है। सूक्ष्मसंपराय तथा यथाख्यातचारित्री के लिए आलोचना तथा विवेक-ये दो प्रायश्चित्त विहित हैं।
जब तक तीर्थ का अस्तित्व है तब तक निर्ग्रन्थों में बकुश एवं प्रतिसेवना कुशील तथा संयतों में इत्वरिक सामायिक संयत एवं छेदोपस्थापनीय चारित्र-इनका अस्तित्व रहेगा। भद्रबाहु के बाद अंतिम दो प्रायश्चित्तों का लोप होने पर भी प्रथम आठ प्रायश्चित्तों का व्यवहार तीर्थ की व्यवच्छित्ति तक चलता रहेगा।
प्रायश्चित्ताह
तप के आधार पर भी प्रायश्चित्ताह के दो भेद किये गए हैं-कृतकरण और अकृतकरण। बेले-तेले आदि तप से अपने आप को भावित करने वाले कृतकरण हैं तथा जो बेले-तेले आदि का तप नहीं कर सकते, वे अकृतकरण हैं। इनके भी दो भेद हैं-सापेक्ष एवं निरपेक्ष। जिन, केवली आदि निरपेक्ष हैं तथा आचार्य, उपाध्याय, भिक्षु आदि सापेक्ष हैं। इनके भेद, प्रभेद एवं विस्तार के लिए देखें व्यभा. गा. १५६-१७३ ।
प्रायश्चित्तवाहक
प्रायश्चित्तवाहक के दो भेद हैं-निर्गत तथा वर्तमान। जो छेद आदि प्रायश्चित्तों का वहन कर रहे हैं, वे निर्गत तथा जो तप पर्यन्त प्रथम छह प्रायश्चित्तों में स्थित हैं, वे वर्तमान कहलाते हैं। इनके भेद-प्रभेदों के विस्तृत वर्णन के लिए देखें (गा. ४७२-७ टी. प १-३)
प्रायश्चित्तार्ह पुरुष के चार प्रकार भाष्य में मिलते हैं(१) उभयतरक (२) आत्मतरक (३) परतरक (४) अन्यतरक।
जो षट्मासी तप करते हुए अग्लान रूप से आचार्य की भी वैयावृत्य करते हैं, वे उभयतर कहलाते हैं। जो केवल तप में शक्ति सम्पन्न होते हैं, वैयावृत्त्य की लब्धि से हीन होते हैं, वे आत्मतरक कहलाते हैं।
जो तप करने में असमर्थ होते हैं, पर आचार्य आदि की वैयावृत्त्य करते हैं, वे परतरक कहलाते हैं। जिनका तप और वैयावृत्त्य दोनों में सामर्थ्य होता है पर एक समय में एक ही कार्य कर सकते हैं, वे अन्यतरक कहलाते हैं।
आत्मतर एवं परतर-ये दो प्रायश्चित्त वहन के अभिमुख होते हैं लेकिन जो परतर और अन्यतर होते हैं, उनमें प्रायश्चित्त का निक्षेप किया जाता है। इनके विस्तृत वर्णन के लिए देखें-व्यभा. ४७६-५०२ टी. प ३-११ । प्रायश्चित्तदान में अनेकान्त
विचारशुद्धि एवं विधायक चिंतन में अनेकान्त का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जैन आचार्यों ने अनेकान्त के प्रयोग को दर्शन की भूमिका के साथ-साथ व्यवहार की भूमिका पर भी उतारा और प्रत्येक क्षेत्र में इसकी महत्ता को प्रमाणित किया।
प्रायश्चित्त में विषमता को अनेकान्त दृष्टि से स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि इंद्रिय विषयों की प्राप्ति समान होने पर भी एक व्यक्ति उनसे विरक्त होता है और दूसरा आसक्त। अतः इन्द्रियों के विषय प्रधान नहीं, प्रधान है अध्यात्म। मन की
१. व्यभा-४१८७। २. व्यभा.४१८६-६२। ३. व्यभा-४१२। ४. व्यभा. ४१८२, ४१५३; जी.१०२।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org