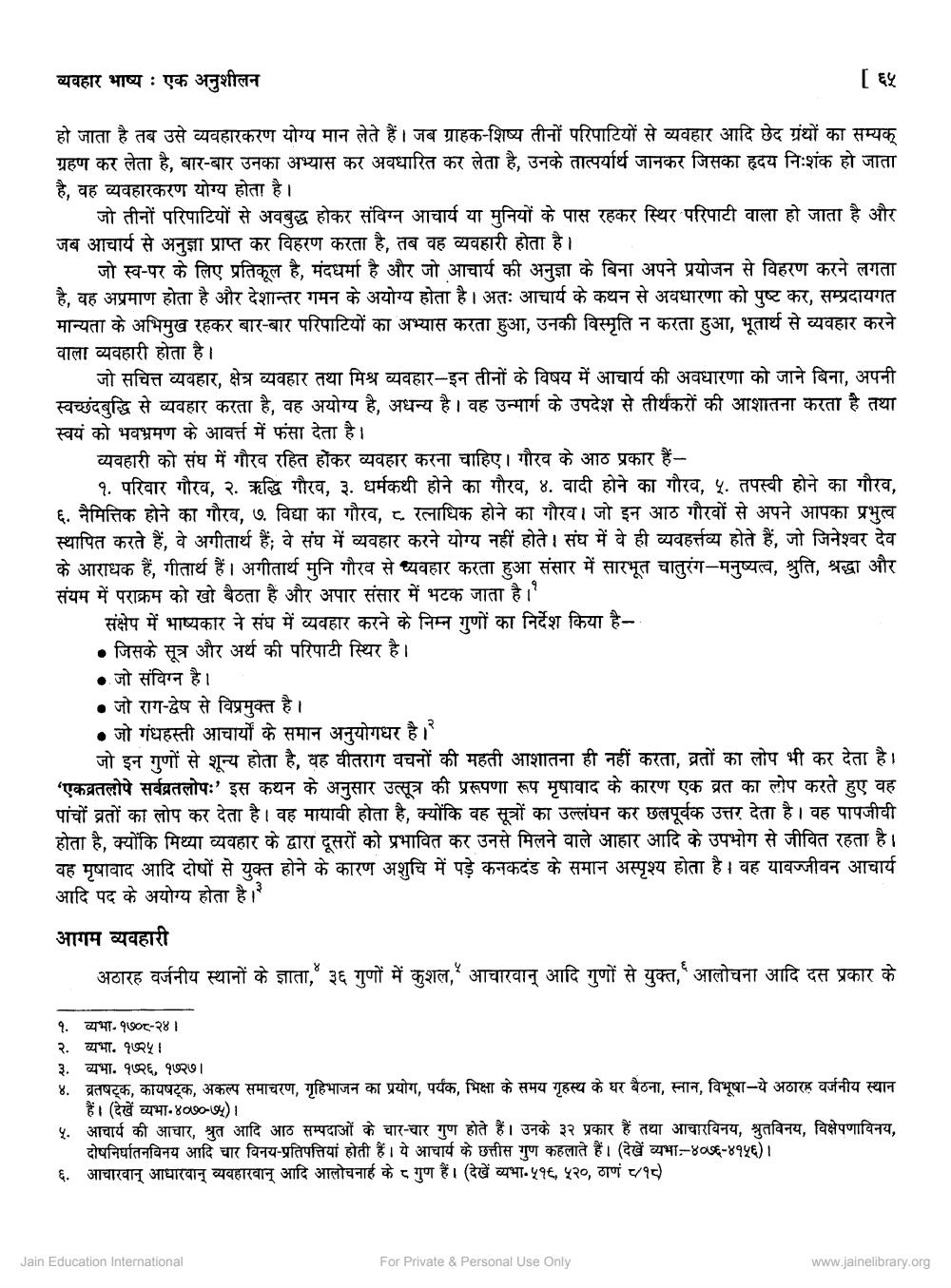________________
व्यवहार भाष्य एक अनुशीलन
[ ६५
हो जाता है तब उसे व्यवहारकरण योग्य मान लेते हैं। जब ग्राहक- शिष्य तीनों परिपाटियों से व्यवहार आदि छेद ग्रंथों का सम्यक् ग्रहण कर लेता है, बार-बार उनका अभ्यास कर अवधारित कर लेता है, उनके तात्पर्यार्थ जानकर जिसका हृदय निःशंक हो जाता है, वह व्यवहारकरण योग्य होता है।
जो तीनों परिपाटियों से अवबुद्ध होकर संविग्न आचार्य या मुनियों के पास रहकर स्थिर परिपाटी वाला हो जाता है और जब आचार्य से अनुज्ञा प्राप्त कर विहरण करता है, तब वह व्यवहारी होता है।
जो स्व-पर के लिए प्रतिकूल है, मंदधर्मा है और जो आचार्य की अनुज्ञा के बिना अपने प्रयोजन से विहरण करने लगता है, वह अप्रमाण होता है और देशान्तर गमन के अयोग्य होता है। अतः आचार्य के कथन से अवधारणा को पुष्ट कर, सम्प्रदायगत मान्यता के अभिमुख रहकर बार-बार परिपाटियों का अभ्यास करता हुआ, उनकी विस्मृति न करता हुआ, भूतार्थ से व्यवहार करने वाला व्यवहारी होता है ।
जो सचित्त व्यवहार, क्षेत्र व्यवहार तथा मिश्र व्यवहार इन तीनों के विषय में आचार्य की अवधारणा को जाने बिना, अपनी स्वच्छंदबुद्धि से व्यवहार करता है, वह अयोग्य है, अधन्य है वह उन्मार्ग के उपदेश से तीर्थकरों की आशातना करता है तथा स्वयं को भवभ्रमण के आवर्त में फंसा देता है।
व्यवहारी को संघ में गौरव रहित होकर व्यवहार करना चाहिए। गौरव के आठ प्रकार हैं
१. परिवार गौरव, २. ऋद्धि गौरव ३. धर्मकथी होने का गौरव, ४. दादी होने का गौरव ५ तपस्वी होने का गौरव, ६. नैमित्तिक होने का गौरव, ७ विद्या का गौरव ८ रत्नाधिक होने का गौरव जो इन आठ गौरवों से अपने आपका प्रभुत्व स्थापित करते हैं, वे अगीतार्थ हैं; वे संघ में व्यवहार करने योग्य नहीं होते । संघ में वे ही व्यवहर्त्तव्य होते हैं, जो जिनेश्वर देव के आराधक हैं, गीतार्थ हैं। अगीतार्थ मुनि गौरव से व्यवहार करता हुआ संसार में सारभूत चातुरंग – मनुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा और संयम में पराक्रम को खो बैठता हैं और अपार संसार में भटक जाता है।'
संक्षेप में भाष्यकार ने संघ में व्यवहार करने के निम्न गुणों का निर्देश किया है
•
जिसके सूत्र और अर्थ की परिपाटी स्थिर है।
• जो संविग्न है।
• जो राग-द्वेष से विप्रमुक्त है।
• जो गंधहस्ती आचार्यों के समान अनुयोगधर है।
जो इन गुणों से शून्य होता है, वह वीतराग वचनों की महती आशातना ही नहीं करता, व्रतों का लोप भी कर देता है। 'एकव्रतलोपे सर्वव्रतलोपः इस कथन के अनुसार उत्सूत्र की प्ररूपणा रूप मृषावाद के कारण एक व्रत का लोप करते हुए वह पांचों व्रतों का लोप कर देता है। वह मायावी होता है, क्योंकि वह सूत्रों का उल्लंघन कर छलपूर्वक उत्तर देता है। वह पापजीवी होता है, क्योंकि मिथ्या व्यवहार के द्वारा दूसरों को प्रभावित कर उनसे मिलने वाले आहार आदि के उपभोग से जीवित रहता है। यह मृषावाद आदि दोषों से युक्त होने के कारण अशुचि में पड़े कनकदंड के समान अस्पृश्य होता है वह यावज्जीवन आचार्य आदि पद के अयोग्य होता है।
आगम व्यवहारी
अठारह वर्जनीय स्थानों के ज्ञाता, ३६ गुणों में कुशल, आचारवान् आदि गुणों से युक्त, ' आलोचना आदि दस प्रकार के
१. व्यभा. १७०८-२४ ।
२. व्यभा. १७२५ ।
३. व्यभा. १७२६, १७२७ ।
४. व्रतषट्क, कायषट्क, अकल्प समाचरण, गृहिभाजन का प्रयोग, पर्यंक, भिक्षा के समय गृहस्थ के घर बैठना, स्नान, विभूषा - ये अठारह वर्जनीय स्थान हैं। (देखें व्यभा• ४०७०-७५) ।
५. आचार्य की आचार, भुत आदि आठ सम्पदाओं के चार-चार गुण होते हैं। उनके ३२ प्रकार हैं तथा आचारविनय, श्रुतविनय, विक्षेपणाविनय, दोषनिर्घातनविनय आदि चार विनय-प्रतिपत्तियां होती हैं। ये आचार्य के छत्तीस गुण कहलाते हैं। (देखें व्यभा-- ४०७६ - ४१५६) ।
६. आचारवान् आधारवान् व्यवहारवान् आदि आलोचनाई के ८ गुण हैं। (देखें व्यभा. ५१६, ५२०, ठाणं ८/१८)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org