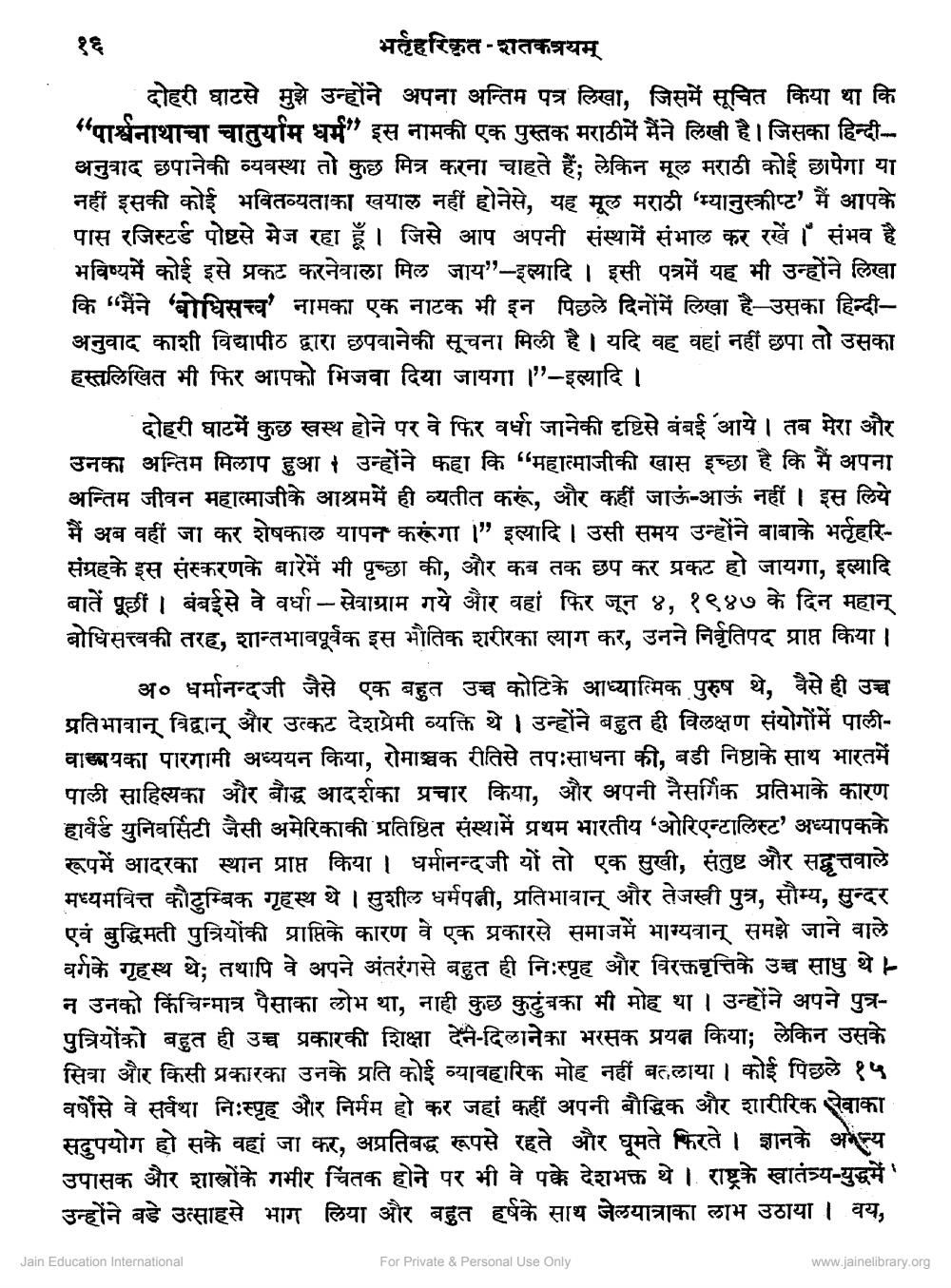________________
भर्तृहरिकृत - शतकत्रयम्
दोहरी घाटसे मुझे उन्होंने अपना अन्तिम पत्र लिखा, जिसमें सूचित किया था कि “पार्श्वनाथाचा चातुर्याम धर्म" इस नामकी एक पुस्तक मराठीमें मैंने लिखी है। जिसका हिन्दी --- अनुवाद छपानेकी व्यवस्था तो कुछ मित्र करना चाहते हैं; लेकिन मूल मराठी कोई छापेगा या नहीं इसकी कोई भवितव्यताका खयाल नहीं होनेसे, यह मूल मराठी 'म्यानुस्क्रीप्ट' मैं आपके पास रजिस्टर्ड पोष्टसे मेज रहा हूँ । जिसे आप अपनी संस्थामें संभाल कर रखें। संभव है भविष्य में कोई इसे प्रकट करनेवाला मिल जाय" - इत्यादि । इसी पत्रमें यह भी उन्होंने लिखा कि "मैंने 'बोधिसत्त्व' नामका एक नाटक भी इन पिछले दिनोंमें लिखा है-उसका हिन्दीअनुवाद काशी विद्यापीठ द्वारा छपवानेकी सूचना मिली है । यदि वह वहां नहीं छपा तो उसका हस्तलिखित भी फिर आपको भिजवा दिया जायगा । " - इत्यादि ।
१६
दोहरी घाटमें कुछ स्वस्थ होने पर वे फिर वर्धा जानेकी दृष्टिसे बंबई आये । तब मेरा और उनका अन्तिम मिलाप हुआ । उन्होंने कहा कि "महात्माजीकी खास इच्छा है कि मैं अपना अन्तिम जीवन महात्माजीके आश्रम में ही व्यतीत करूं, और कहीं जाऊं - आऊं नहीं । इस लिये मैं अब वहीं जा कर शेषकाल यापन करूंगा ।" इत्यादि । उसी समय उन्होंने बाबाके भर्तृहरि - संग्रहके इस संस्करणके बारेमें भी पृच्छा की, और कब तक छप कर प्रकट हो जायगा, इत्यादि बातें पूछीं । बंबई से वे वर्धा - सेवाग्राम गये और वहां फिर जून ४, १९४७ के दिन महान् बोधिसत्त्वकी तरह, शान्तभावपूर्वक इस भौतिक शरीरका त्याग कर, उनने निर्वृतिपद प्राप्त किया ।
अ० धर्मानन्दजी जैसे एक बहुत उच्च कोटिके आध्यात्मिक पुरुष थे, वैसे ही उच्च प्रतिभावान् विद्वान् और उत्कट देशप्रेमी व्यक्ति थे । उन्होंने बहुत ही विलक्षण संयोगों में पालीवाङ्मयका पारगामी अध्ययन किया, रोमाञ्चक रीतिसे तपःसाधना की, बडी निष्ठाके साथ भारत में पाली साहित्यका और बौद्ध आदर्शका प्रचार किया, और अपनी नैसर्गिक प्रतिभाके कारण हार्वर्ड युनिवर्सिटी जैसी अमेरिकाकी प्रतिष्ठित संस्था में प्रथम भारतीय 'ओरिएन्टालिस्ट' अध्यापकके रूपमें आदरका स्थान प्राप्त किया । धर्मानन्दजी यों तो एक सुखी, संतुष्ट और सद्वृत्तवाले मध्यमवित्त कौटुम्बिक गृहस्थ थे । सुशील धर्मपत्नी, प्रतिभावान् और तेजखी पुत्र, सौम्य, सुन्दर एवं बुद्धिमती पुत्रियोंकी प्राप्तिके कारण वे एक प्रकारसे समाजमें भाग्यवान् समझे जाने वाले वर्ग गृहस्थ थे; तथापि वे अपने अंतरंगसे बहुत ही निःस्पृह और विरक्तवृत्तिके उच्च साधु थे । - न उनको किंचिन्मात्र पैसाका लोभ था, नाही कुछ कुटुंबका भी मोह था । उन्होंने अपने पुत्रपुत्रियोंको बहुत ही उच्च प्रकारकी शिक्षा देने - दिलाने का भरसक प्रयत्न किया; लेकिन उसके सिवा और किसी प्रकारका उनके प्रति कोई व्यावहारिक मोह नहीं बतलाया । कोई पिछले १५ वर्षोंसे वे सर्वथा निःस्पृह और निर्मम हो कर जहां कहीं अपनी बौद्धिक और शारीरिक सेवाका सदुपयोग हो सके वहां जा कर, अप्रतिबद्ध रूपसे रहते और घूमते फिरते । ज्ञानके अन्य उपासक और शास्त्रोंके गभीर चिंतक होने पर भी वे पक्के देशभक्त थे । राष्ट्रके स्वातंत्र्य युद्धमें ' उन्होंने बड़े उत्साह से भाग लिया और बहुत हर्षके साथ जेलयात्राका लाभ उठाया । वय,
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org