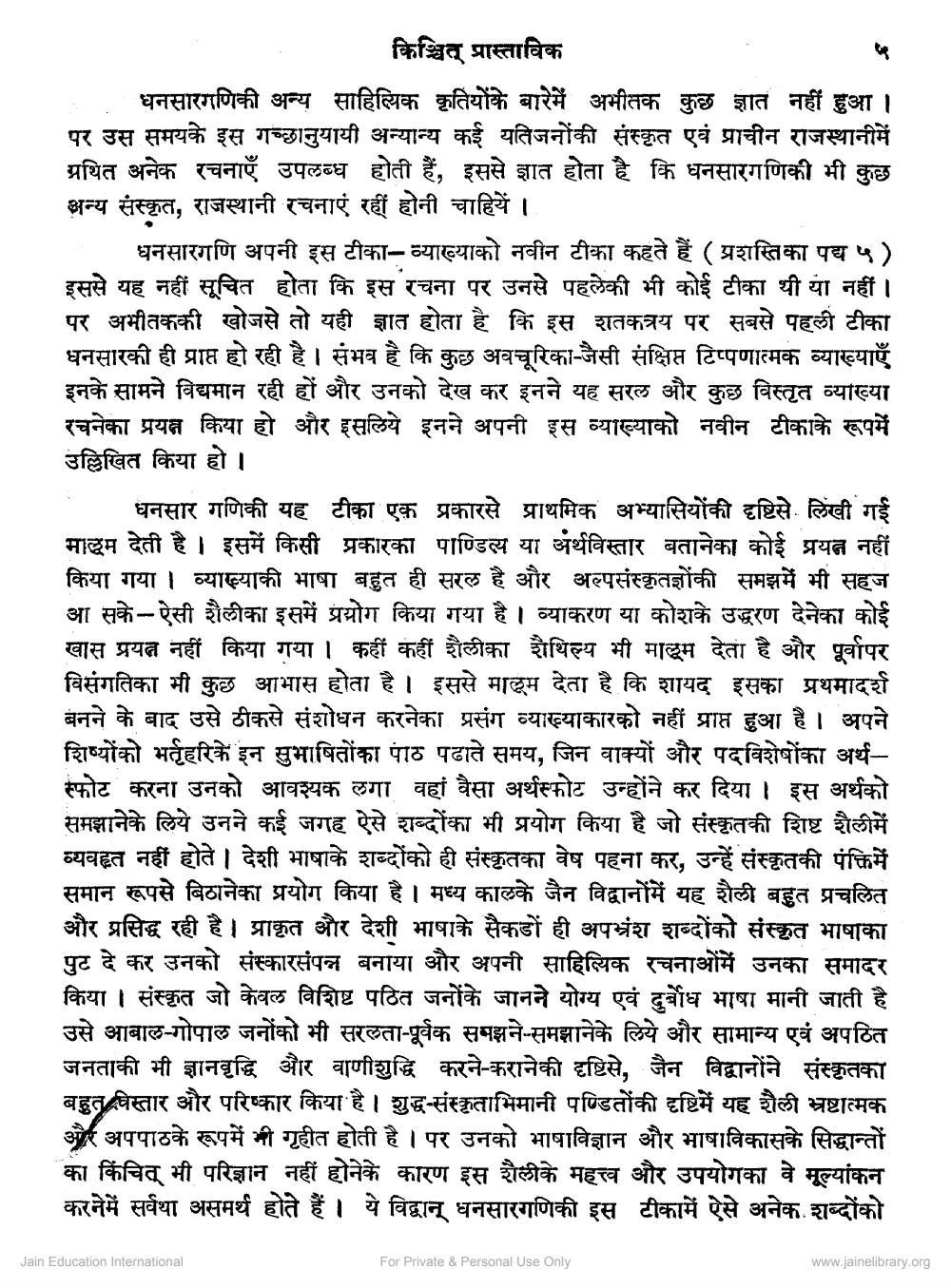________________
किञ्चित् प्रास्ताविक धनसारगणिकी अन्य साहित्यिक कृतियोंके बारेमें अभीतक कुछ ज्ञात नहीं हुआ। पर उस समयके इस गच्छानुयायी अन्यान्य कई यतिजनोंकी संस्कृत एवं प्राचीन राजस्थानीमें ग्रथित अनेक रचनाएँ उपलब्ध होती हैं, इससे ज्ञात होता है कि धनसारगणिकी भी कुछ अन्य संस्कृत, राजस्थानी रचनाएं रहीं होनी चाहिये ।
धनसारगणि अपनी इस टीका- व्याख्याको नवीन टीका कहते हैं (प्रशस्तिका पद्य ५) इससे यह नहीं सूचित होता कि इस रचना पर उनसे पहलेकी भी कोई टीका थी या नहीं। पर अभीतककी खोजसे तो यही ज्ञात होता है कि इस शतकत्रय पर सबसे पहली टीका धनसारकी ही प्राप्त हो रही है। संभव है कि कुछ अवचूरिका-जैसी संक्षिप्त टिप्पणात्मक व्याख्याएँ इनके सामने विद्यमान रही हों और उनको देख कर इनने यह सरल और कुछ विस्तृत व्याख्या रचनेका प्रयन किया हो और इसलिये इनने अपनी इस व्याख्याको नवीन टीकाके रूपमें उल्लिखित किया हो।
धनसार गणिकी यह टीका एक प्रकारसे प्राथमिक अभ्यासियोंकी दृष्टिसे लिखी गई मालूम देती है। इसमें किसी प्रकारका पाण्डित्य या अर्थविस्तार बतानेका कोई प्रयत्न नहीं किया गया। व्याख्याकी भाषा बहुत ही सरल है और अल्पसंस्कृतज्ञोंकी समझमें भी सहज आ सके-ऐसी शैलीका इसमें प्रयोग किया गया है। व्याकरण या कोशके उद्धरण देनेका कोई खास प्रयत्न नहीं किया गया । कहीं कहीं शैलीका शैथिल्य भी मालूम देता है और पूर्वापर विसंगतिका भी कुछ आभास होता है। इससे मालूम देता है कि शायद इसका प्रथमादर्श बनने के बाद उसे ठीकसे संशोधन करनेका प्रसंग व्याख्याकारको नहीं प्राप्त हुआ है। अपने शिष्योंको भर्तृहरिके इन सुभाषितोंका पाठ पढाते समय, जिन वाक्यों और पदविशेषोंका अर्थस्फोट करना उनको आवश्यक लगा वहां वैसा अर्थस्फोट उन्होंने कर दिया। इस अर्थको समझानेके लिये उनने कई जगह ऐसे शब्दोंका भी प्रयोग किया है जो संस्कृतकी शिष्ट शैलीमें व्यवहृत नहीं होते। देशी भाषाके शब्दोंको ही संस्कृतका वेष पहना कर, उन्हें संस्कृतकी पंक्तिमें समान रूपसे बिठानेका प्रयोग किया है। मध्य कालके जैन विद्वानोंमें यह शैली बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध रही है। प्राकृत और देशी भाषाके सैकडों ही अपभ्रंश शब्दोंको संस्कृत भाषाका पुट दे कर उनको संस्कारसंपन्न बनाया और अपनी साहित्यिक रचनाओंमें उनका समादर किया । संस्कृत जो केवल विशिष्ट पठित जनोंके जानने योग्य एवं दुर्बोध भाषा मानी जाती है उसे आबाल-गोपाल जनोंको भी सरलता-पूर्वक समझने-समझानेके लिये और सामान्य एवं अपठित जनताकी भी ज्ञानवृद्धि और वाणीशुद्धि करने-करानेकी दृष्टिसे, जैन विद्वानोंने संस्कृतका बहुत विस्तार और परिष्कार किया है। शुद्ध-संस्कृताभिमानी पण्डितोंकी दृष्टि में यह शैली भ्रष्टात्मक और अपपाठके रूपमें भी गृहीत होती है । पर उनको भाषाविज्ञान और भाषाविकासके सिद्धान्तों का किंचित् भी परिज्ञान नहीं होनेके कारण इस शैलीके महत्त्व और उपयोगका वे मूल्यांकन करनेमें सर्वथा असमर्थ होते हैं। ये विद्वान् धनसारगणिकी इस टीकामें ऐसे अनेक शब्दोंको
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org