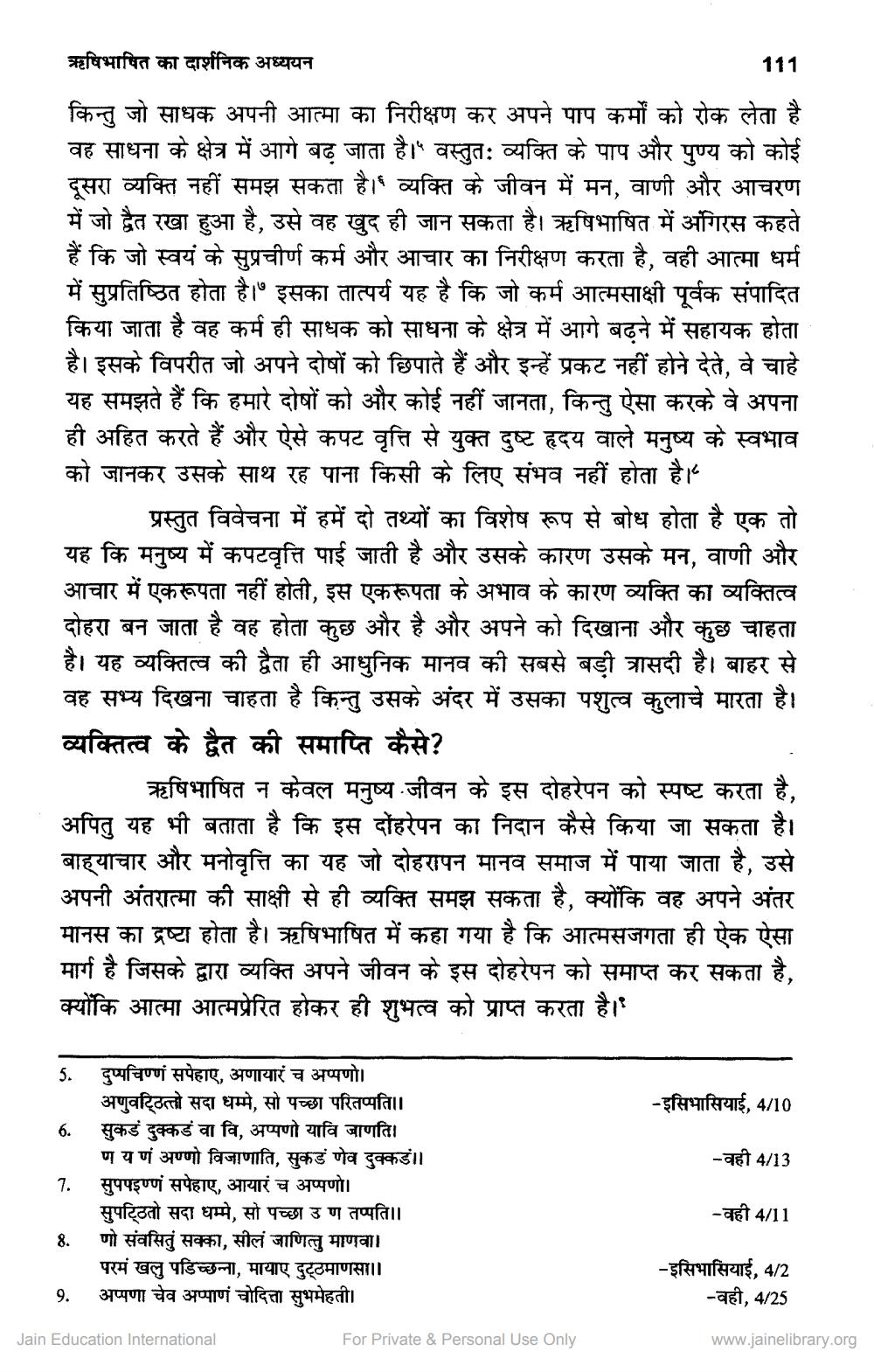________________
ऋषिभाषित का दार्शनिक अध्ययन
111
किन्तु जो साधक अपनी आत्मा का निरीक्षण कर अपने पाप कर्मों को रोक लेता है। वह साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है । " वस्तुतः व्यक्ति के पाप और पुण्य को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता है।' व्यक्ति के जीवन में मन, वाणी और आचरण में जो द्वैत रखा हुआ है, उसे वह खुद ही जान सकता है। ऋषिभाषित में अंगिरस कहते हैं कि जो स्वयं के सुप्रचीर्ण कर्म और आचार का निरीक्षण करता है, वही आत्मा धर्म में सुप्रतिष्ठित होता है।" इसका तात्पर्य यह है कि जो कर्म आत्मसाक्षी पूर्वक संपादित किया जाता है वह कर्म ही साधक को साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायक होता है । इसके विपरीत जो अपने दोषों को छिपाते हैं और इन्हें प्रकट नहीं होने देते, वे चाहे यह समझते हैं कि हमारे दोषों को और कोई नहीं जानता, किन्तु ऐसा करके वे अपना ही अहित करते हैं और ऐसे कपट वृत्ति से युक्त दुष्ट हृदय वाले मनुष्य के स्वभाव को जानकर उसके साथ रह पाना किसी के लिए संभव नहीं होता है । "
प्रस्तुत विवेचना में हमें दो तथ्यों का विशेष रूप से बोध होता है एक तो यह कि मनुष्य में कपटवृत्ति पाई जाती है और उसके कारण उसके मन, वाणी और आचार में एकरूपता नहीं होती, इस एकरूपता के अभाव के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व दोहरा बन जाता है वह होता कुछ और है और अपने को दिखाना और कुछ चाहता है । यह व्यक्तित्व की द्वैता ही आधुनिक मानव की सबसे बड़ी त्रासदी है। बाहर से वह सभ्य दिखना चाहता है किन्तु उसके अंदर में उसका पशुत्व कुलाचे मारता है। व्यक्तित्व के द्वैत की समाप्ति कैसे ?
ऋषिभाषित न केवल मनुष्य जीवन के इस दोहरेपन को स्पष्ट करता है, अपितु यह भी बताता है कि इस दोहरेपन का निदान कैसे किया जा सकता है। बाह्याचार और मनोवृत्ति का यह जो दोहरापन मानव समाज में पाया जाता है, उसे अपनी अंतरात्मा की साक्षी से ही व्यक्ति समझ सकता है, क्योंकि वह अपने अंतर मानस का द्रष्टा होता है। ऋषिभाषित में कहा गया है कि आत्मसजगता ही ऐक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के इस दोहरेपन को समाप्त कर सकता है, क्योंकि आत्मा आत्मप्रेरित होकर ही शुभत्व को प्राप्त करता है । "
5. दुष्पचिणं सपेहाए, अणायारं च अप्पणो ।
6.
7.
8.
9.
अणुवट्ठितो सदा धम्मे, सो पच्छा परितप्पति।। सुकडं दुक्कडं वा वि, अप्पणो यावि जाणति । ण णं अण्णो विजाणाति, सुकडं णेव दुक्कडं ॥ सुपपइण्णं सपेहाए, आयारं च अप्पणो । सुपट्ठितो सदा धम्मे, सो पच्छा उ ण तप्पति ।।
संवसितुं सक्का, सीलं जाणित्तु माणवा । परमं खलु पडिच्छन्ना, मायाए दुट्ठमाणसा ।। अप्पणा चेव अप्पाणं चोदित्ता सुभमेहती।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
- इसिभासियाई, 4 / 10
-वही 4/13 -वही 4/11
- इसिभासियाई, 4/2 -वही, 4/25 www.jainelibrary.org