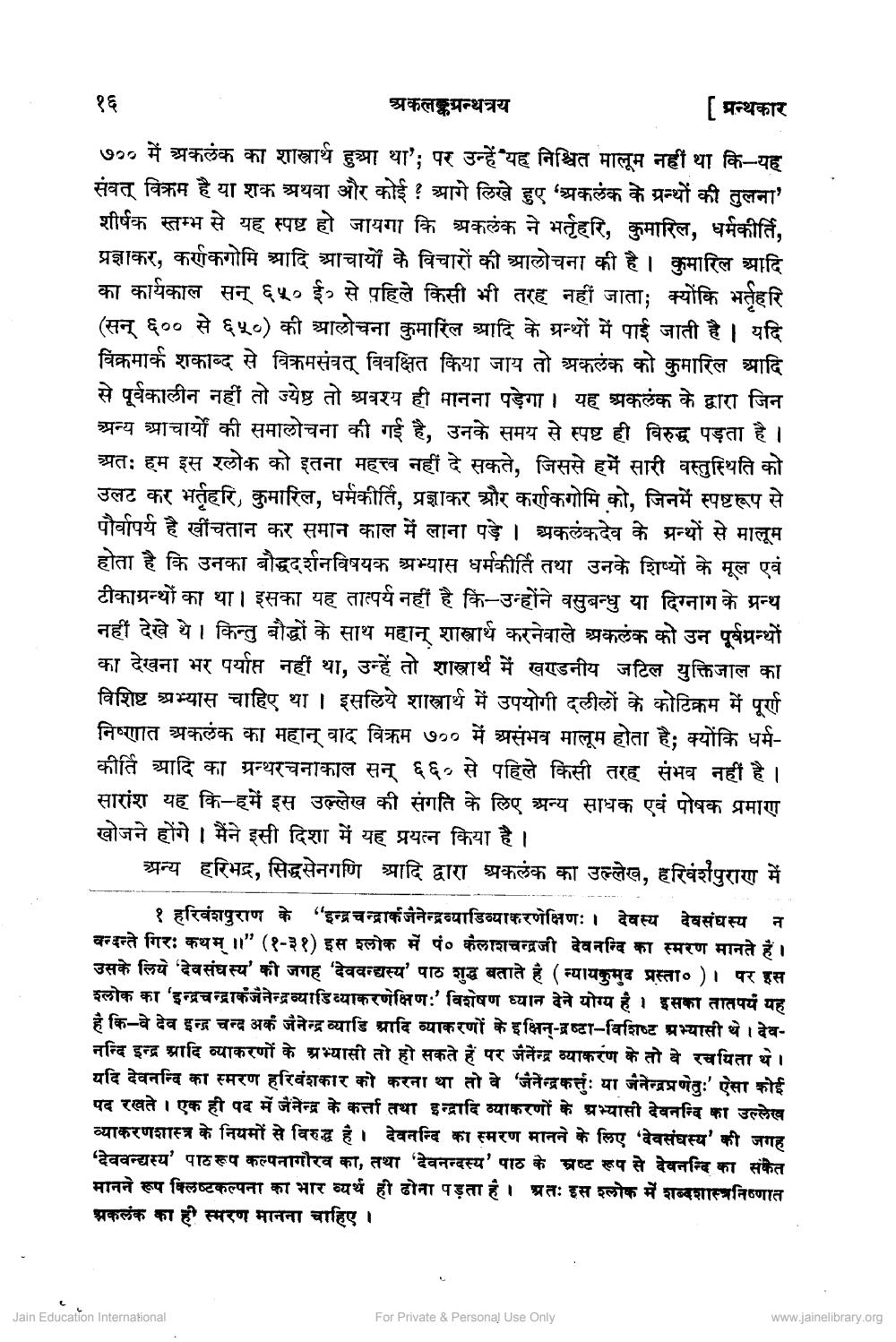________________
अकलङ्कग्रन्थत्रय
[प्रन्थकार
७२० में अकलंक का शास्त्रार्थ हुआ था'; पर उन्हें यह निश्चित मालूम नहीं था कि यह संवत् विक्रम है या शक अथवा और कोई ? आगे लिखे हुए 'अकलंक के ग्रन्थों की तुलना' शीर्षक स्तम्भ से यह स्पष्ट हो जायगा कि अकलंक ने भर्तृहरि, कुमारिल, धर्मकीर्ति, प्रज्ञाकर, कर्णकगोमि आदि आचार्यों के विचारों की आलोचना की है। कुमारिल आदि का कार्यकाल सन् ६५० ई. से पहिले किसी भी तरह नहीं जाता; क्योंकि भर्तृहरि (सन् ६०० से ६५०) की आलोचना कुमारिल आदि के ग्रन्थों में पाई जाती है । यदि विक्रमार्क शकाब्द से विक्रमसंवत् विवक्षित किया जाय तो अकलंक को कुमारिल आदि से पूर्वकालीन नहीं तो ज्येष्ठ तो अवश्य ही मानना पड़ेगा। यह अकलंक के द्वारा जिन अन्य आचार्यों की समालोचना की गई है, उनके समय से स्पष्ट ही विरुद्ध पड़ता है । अतः हम इस श्लोक को इतना महत्त्व नहीं दे सकते, जिससे हमें सारी वस्तुस्थिति को उलट कर भर्तृहरि, कुमारिल, धर्मकीर्ति, प्रज्ञाकर और कर्णकगोमि को, जिनमें स्पष्ट रूप से पौर्वापर्य है खींचतान कर समान काल में लाना पड़े। अकलंकदेव के ग्रन्थों से मालूम होता है कि उनका बौद्धदर्शनविषयक अभ्यास धर्मकीर्ति तथा उनके शिष्यों के मूल एवं टीकाग्रन्थों का था। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उन्होंने वसुबन्धु या दिग्नाग के ग्रन्थ नहीं देखे थे। किन्तु बौद्धों के साथ महान् शास्त्रार्थ करनेवाले अकलंक को उन पूर्वग्रन्थों का देखना भर पर्याप्त नहीं था, उन्हें तो शास्त्रार्थ में खण्डनीय जटिल युक्तिजाल का विशिष्ट अभ्यास चाहिए था। इसलिये शास्त्रार्थ में उपयोगी दलीलों के कोटिक्रम में पूर्ण निष्णात अकलंक का महान् वाद विक्रम ७०० में असंभव मालूम होता है; क्योंकि धर्मकीर्ति आदि का ग्रन्थरचनाकाल सन् ६६० से पहिले किसी तरह संभव नहीं है । सारांश यह कि हमें इस उल्लेख की संगति के लिए अन्य साधक एवं पोषक प्रमाण खोजने होंगे । मैंने इसी दिशा में यह प्रयत्न किया है।
अन्य हरिभद्र, सिद्धसेनगणि आदि द्वारा अकलंक का उल्लेख, हरिवंशपुराण में
१ हरिवंशपुराण के “इन्द्रचन्द्रार्कजैनेन्द्रव्याडिव्याकरणेक्षिणः। देवस्य देवसंघस्य न वन्दन्ते गिरः कथम ॥" (१-३१) इस श्लोक में पं० कैलाशचन्द्रजी देवनन्दि का स्मरण मानते हैं। उसके लिये 'देवसंघस्य' की जगह 'देववन्द्यस्य' पाठ शुद्ध बताते है (न्यायकुमुद प्रस्ता० )। पर इस श्लोक का 'इन्द्रचन्द्राकंजैनेन्द्रव्याडिव्याकरणक्षिण:' विशेषण ध्यान देने योग्य है। इसका तातपर्य यह है कि-वे देव इन्द्र चन्द अकं जैनेन्द्र व्याडि प्रादि व्याकरणों के इक्षिन-द्रष्टा-विशिष्ट अभ्यासी थे। देव
इन्द्र आदि व्याकरणों के अभ्यासी तो हो सकते हैं पर जैनेन्द्र व्याकरण के तो वे रचयिता थे। यदि देवनन्दि का स्मरण हरिवंशकार को करना था तो वे 'जैनेन्द्रकर्तुः या जैनेन्द्रप्रणेतुः' ऐसा कोई पद रखते। एक ही पद में जैनेन्द्र के कर्ता तथा इन्द्रादि व्याकरणों के अभ्यासी देवनन्दि का उल्लेख व्याकरणशास्त्र के नियमों से विरुद्ध है। देवनन्दि का स्मरण मानने के लिए 'देवसंघस्य' की जगह 'देववन्द्यस्य' पाठरूप कल्पनागौरव का, तथा 'देवनन्दस्य' पाठ के स्रष्ट रूप से देवनन्दि का संकेत मानने रूप क्लिष्टकल्पना का भार व्यर्थ ही ढोना पड़ता है। अतः इस श्लोक में शब्दशास्त्रनिष्णात अकलंक का ही स्मरण मानना चाहिए।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org