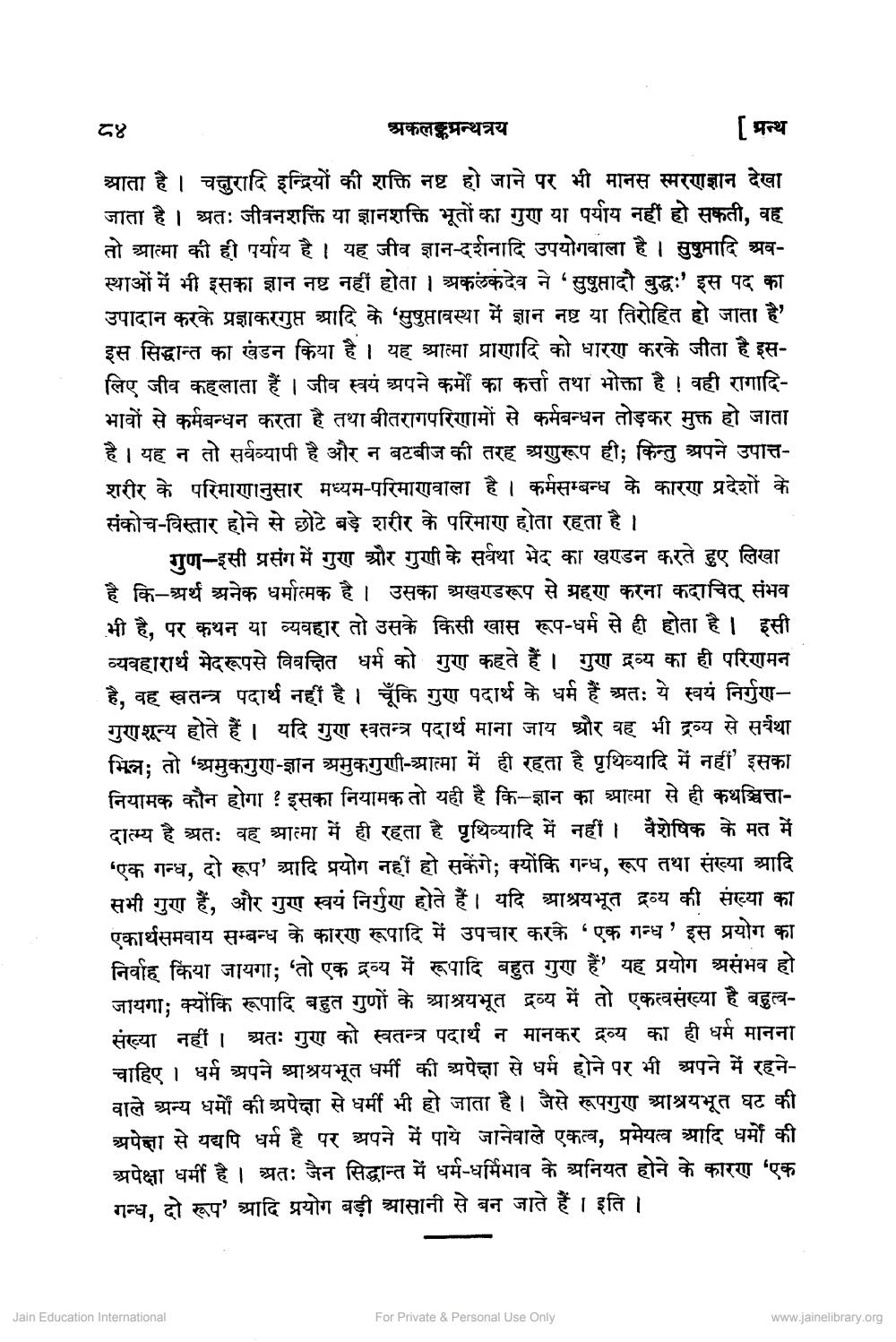________________
८४ अकलङ्कप्रन्थत्रय
[प्रन्थ आता है । चक्षुरादि इन्द्रियों की शक्ति नष्ट हो जाने पर भी मानस स्मरणज्ञान देखा जाता है । अतः जीवनशक्ति या ज्ञानशक्ति भूतों का गुण या पर्याय नहीं हो सकती, वह तो आत्मा की ही पर्याय है। यह जीव ज्ञान-दर्शनादि उपयोगवाला है। सुषुप्तादि अवस्थाओं में भी इसका ज्ञान नष्ट नहीं होता । अकलंकदेव ने ‘सुषुप्तादौ बुद्धः' इस पद का उपादान करके प्रज्ञाकरगुप्त आदि के 'सुषुप्तावस्था में ज्ञान नष्ट या तिरोहित हो जाता है' इस सिद्धान्त का खंडन किया है । यह आत्मा प्राणादि को धारण करके जीता है इसलिए जीव कहलाता हैं । जीव स्वयं अपने कर्मों का कर्ता तथा भोक्ता है ! वही रागादिभावों से कर्मबन्धन करता है तथा बीतरागपरिणामों से कर्मबन्धन तोड़कर मुक्त हो जाता है । यह न तो सर्वव्यापी है और न बटबीज की तरह अणुरूप ही; किन्तु अपने उपात्तशरीर के परिमाणानुसार मध्यम-परिमाणवाला है। कर्मसम्बन्ध के कारण प्रदेशों के संकोच-विस्तार होने से छोटे बड़े शरीर के परिमाण होता रहता है ।
गुण-इसी प्रसंग में गुण और गुणी के सर्वथा भेद का खण्डन करते हुए लिखा है कि-अर्थ अनेक धर्मात्मक है। उसका अखण्डरूप से ग्रहण करना कदाचित् संभव भी है, पर कथन या व्यवहार तो उसके किसी खास रूप-धर्म से ही होता है। इसी व्यवहारार्थ भेदरूपसे विवक्षित धर्म को गुण कहते हैं। गुण द्रव्य का ही परिणमन है, वह खतन्त्र पदार्थ नहीं है । चूंकि गुण पदार्थ के धर्म हैं अतः ये स्वयं निर्गुणगुणशून्य होते हैं। यदि गुण स्वतन्त्र पदार्थ माना जाय और वह भी द्रव्य से सर्वथा भिन्न; तो 'अमुकगुण-ज्ञान अमुकगुणी-आत्मा में ही रहता है पृथिव्यादि में नहीं' इसका नियामक कौन होगा ? इसका नियामक तो यही है कि-ज्ञान का आत्मा से ही कथञ्चित्तादात्म्य है अतः वह आत्मा में ही रहता है पृथिव्यादि में नहीं। वैशेषिक के मत में 'एक गन्ध, दो रूप' आदि प्रयोग नहीं हो सकेंगे; क्योंकि गन्ध, रूप तथा संख्या आदि सभी गुण हैं, और गुण स्वयं निर्गुण होते हैं। यदि आश्रयभूत द्रव्य की संख्या का एकार्थसमवाय सम्बन्ध के कारण रूपादि में उपचार करके 'एक गन्ध' इस प्रयोग का निर्वाह किया जायगा; 'तो एक द्रव्य में रूपादि बहुत गुण हैं' यह प्रयोग असंभव हो जायगा; क्योंकि रूपादि बहुत गुणों के आश्रयभूत द्रव्य में तो एकत्वसंख्या है बहुत्वसंख्या नहीं। अतः गुण को स्वतन्त्र पदार्थ न मानकर द्रव्य का ही धर्म मानना चाहिए। धर्म अपने आश्रयभूत धर्मी की अपेक्षा से धर्म होने पर भी अपने में रहनेवाले अन्य धर्मों की अपेक्षा से धर्मी भी हो जाता है। जैसे रूपगुण आश्रयभूत घट की अपेक्षा से यद्यपि धर्म है पर अपने में पाये जानेवाले एकत्व, प्रमेयत्व आदि धर्मों की अपेक्षा धर्मी है । अतः जैन सिद्धान्त में धर्म-धर्मिभाव के अनियत होने के कारण 'एक गन्ध, दो रूप' आदि प्रयोग बड़ी आसानी से बन जाते हैं । इति ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org