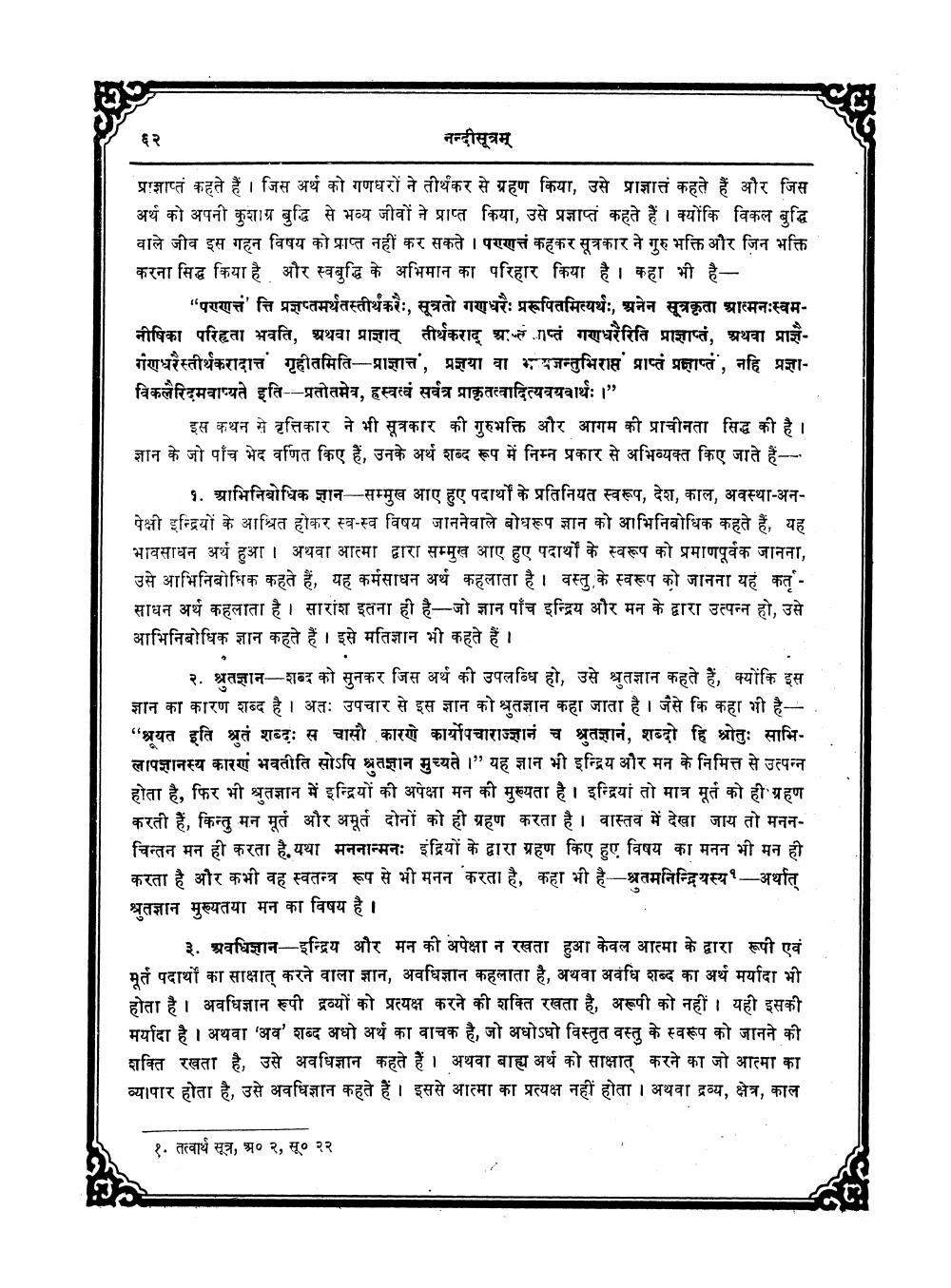________________
नन्दीसूत्रम्
प्राशाप्तं कहते हैं। जिस अर्थ को गणधरों ने तीर्थंकर से ग्रहण किया, उसे प्राज्ञातं कहते हैं और जिस अर्थ को अपनी कुशाग्र बुद्धि से भव्य जीवों ने प्राप्त किया, उसे प्रज्ञाप्तं कहते हैं। क्योंकि विकल बुद्धि वाले जीव इस गहन विषय को प्राप्त नहीं कर सकते । पण्णत्तं कहकर सुत्रकार ने गुरु भक्ति और जिन भक्ति करना सिद्ध किया है और स्वबुद्धि के अभिमान का परिहार किया है। कहा भी है
"पण्णत्त' त्ति प्रज्ञप्तमर्थतस्तीर्थकरैः, सूत्रतो गणधरैः प्ररूपितमित्यर्थः, अनेन सूत्रकृता प्रात्मनःस्वमनीषिका परिहृता भवति, अथवा प्राज्ञात् तीर्थकराद् प्रा. गप्तं गणधरैरिति प्राज्ञाप्त, अथवा प्राज्ञैगंणधरैस्तीर्थकरादात्तं गृहीतमिति-प्राज्ञात्त, प्रज्ञया वा भयजन्तुभिराप्त प्राप्त प्रज्ञाप्तं, नहि प्रज्ञाविकलैरिदमवाप्यते इति--प्रतोतमेव, ह्रस्वत्वं सर्वत्र प्राकृतत्वादित्यवयवार्थः ।"
इस कथन से वृत्तिकार ने भी सूत्रकार की गुरुभक्ति और आगम की प्राचीनता सिद्ध की है। ज्ञान के जो पाँच भेद वणित किए हैं, उनके अर्थ शब्द रूप में निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किए जाते हैं
१. प्राभिनिबोधिक ज्ञान-सम्मुख आए हए पदार्थों के प्रतिनियत स्वरूप, देश, काल, अवस्था-अनपेक्षी इन्द्रियों के आश्रित होकर स्व-स्व विषय जाननेवाले बोधरूप ज्ञान को आभिनिबोधिक कहते हैं, यह भावसाधन अर्थ हुआ। अथवा आत्मा द्वारा सम्मुख आए हुए पदार्थों के स्वरूप को प्रमाणपूर्वक जानना, उसे आभिनिबोधिक कहते हैं, यह कर्मसाधन अर्थ कहलाता है। वस्तु के स्वरूप को जानना यहं कर्तृ - साधन अर्थ कहलाता है। सारांश इतना ही है जो ज्ञान पाँच इन्द्रिय और मन के द्वारा उत्पन्न हो, उसे आभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं । इसे मतिज्ञान भी कहते हैं ।
२. श्रुतज्ञान-शब्द को सुनकर जिस अर्थ की उपलब्धि हो, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान का कारण शब्द है । अतः उपचार से इस ज्ञान को श्रुतज्ञान कहा जाता है। जैसे कि कहा भी है"श्रयत इति श्रुतं शब्दः स चासौ कारणे कार्योपचाराज्ज्ञानं च श्रुतज्ञानं, शब्दो हि श्रोतुः साभिलापज्ञानस्य कारणं भवतीति सोऽपि श्रुतज्ञान मुच्यते ।" यह ज्ञान भी इन्द्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है, फिर भी श्रुतज्ञान में इन्द्रियों की अपेक्षा मन की मुख्यता है । इन्द्रियां तो मात्र मूर्त को ही ग्रहण करती हैं, किन्तु मन मूर्त और अमूर्त दोनों को ही ग्रहण करता है। वास्तव में देखा जाय तो मननचिन्तन मन ही करता है. यथा मननान्मनः इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए विषय का मनन भी मन ही करता है और कभी वह स्वतन्त्र रूप से भी मनन करता है, कहा भी है-श्रतमनिन्द्रियस्य–अर्थात श्रुतज्ञान मुख्यतया मन का विषय है।
३. अवधिज्ञान-इन्द्रिय और मन की अपेक्षा न रखता हुआ केवल आत्मा के द्वारा रूपी एवं मुर्त पदार्थों का साक्षात् करने वाला ज्ञान, अवधिज्ञान कहलाता है, अथवा अवधि शब्द का अर्थ मर्यादा भी होता है। अवधिज्ञान रूपी द्रव्यों को प्रत्यक्ष करने की शक्ति रखता है, अरूपी को नहीं। यही इसकी मर्यादा है। अथवा 'अव' शब्द अधो अर्थ का वाचक है, जो अधोऽधो विस्तृत वस्तु के स्वरूप को जानने की शक्ति रखता है, उसे अवधिज्ञान कहते हैं। अथवा बाह्य अर्थ को साक्षात् करने का जो आत्मा का व्यापार होता है, उसे अवधिज्ञान कहते हैं। इससे आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता । अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल
१. तत्वार्थ सूत्र, अ० २, सू० २२