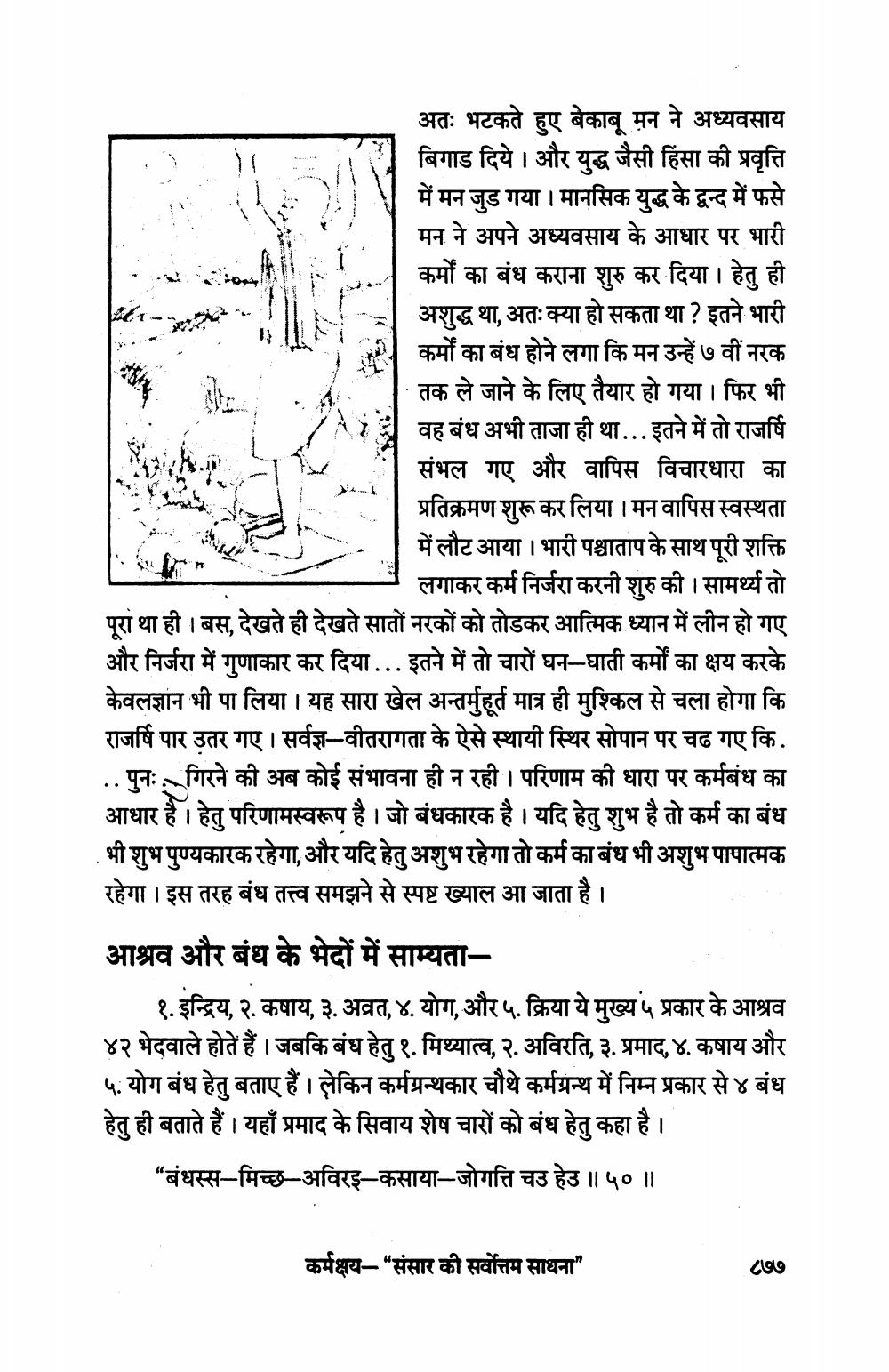________________
अतः भटकते हुए बेकाबू मन ने अध्यवसाय बिगाड दिये । और युद्ध जैसी हिंसा की प्रवृत्ति में मन जुड गया । मानसिक युद्ध के द्वन्द में फसे मन ने अपने अध्यवसाय के आधार पर भारी कर्मों का बंध कराना शुरु कर दिया। हेतु ही अशुद्ध था, अतः क्या हो सकता था ? इतने भारी कर्मों का बंध होने लगा कि मन उन्हें ७ वीं नरक तक ले जाने के लिए तैयार हो गया । फिर भी वह बंध अभी ताजा ही था.... . इतने में तो राजर्षि संभल गए और वापिस विचारधारा का प्रतिक्रमण शुरू कर लिया । मन वापिस स्वस्थता में लौट आया । भारी पश्चाताप के साथ पूरी शक्ति लगाकर कर्म निर्जरा करनी शुरु की। सामर्थ्य तो पूरा था ही । बस, देखते ही देखते सातों नरकों को तोडकर आत्मिक ध्यान में लीन हो गए और निर्जरा में गुणाकार कर दिया... इतने में तो चारों घन-घाती कर्मों का क्षय करके केवलज्ञान भी पा लिया । यह सारा खेल अन्तर्मुहूर्त मात्र ही मुश्किल से चला होगा कि राजर्षि पार उतर गए । सर्वज्ञ - वीतरागता के ऐसे स्थायी स्थिर सोपान पर चढ गए कि . . पुनः गिरने की अब कोई संभावना ही न रही । परिणाम की धारा पर कर्मबंध का आधार है । हेतु परिणामस्वरूप है । जो बंधकारक है । यदि हेतु शुभ है तो कर्म का बंध भी शुभ पुण्यकारक रहेगा, और यदि हेतु अशुभ रहेगा तो कर्म का बंध भी अशुभ पापात्मक रहेगा । इस तरह बंध तत्त्व समझने से स्पष्ट ख्याल आ जाता है ।
आश्रव और बंध के भेदों में साम्यता
१. इन्द्रिय, २. कषाय, ३. अव्रत, ४. योग, और ५. क्रिया ये मुख्य ५ प्रकार के आश्रव ४२ भेदवाले होते हैं । जबकि बंध हेतु १. मिथ्यात्व, २ . अविरति, ३. प्रमाद, ४. कषाय और ५. योग बंध हेतु बताए हैं। लेकिन कर्मग्रन्थकार चौथे कर्मग्रन्थ में निम्न प्रकार से ४ बंध हेतु ही बताते हैं । यहाँ प्रमाद के सिवाय शेष चारों को बंध हेतु कहा है ।
1
“बंधस्स - मिच्छ— अविरइ - कसाया - जोगत्ति चउ हेउ ॥ ५० ॥
कर्मक्षय- "संसार की सर्वोत्तम साधना "
८७७