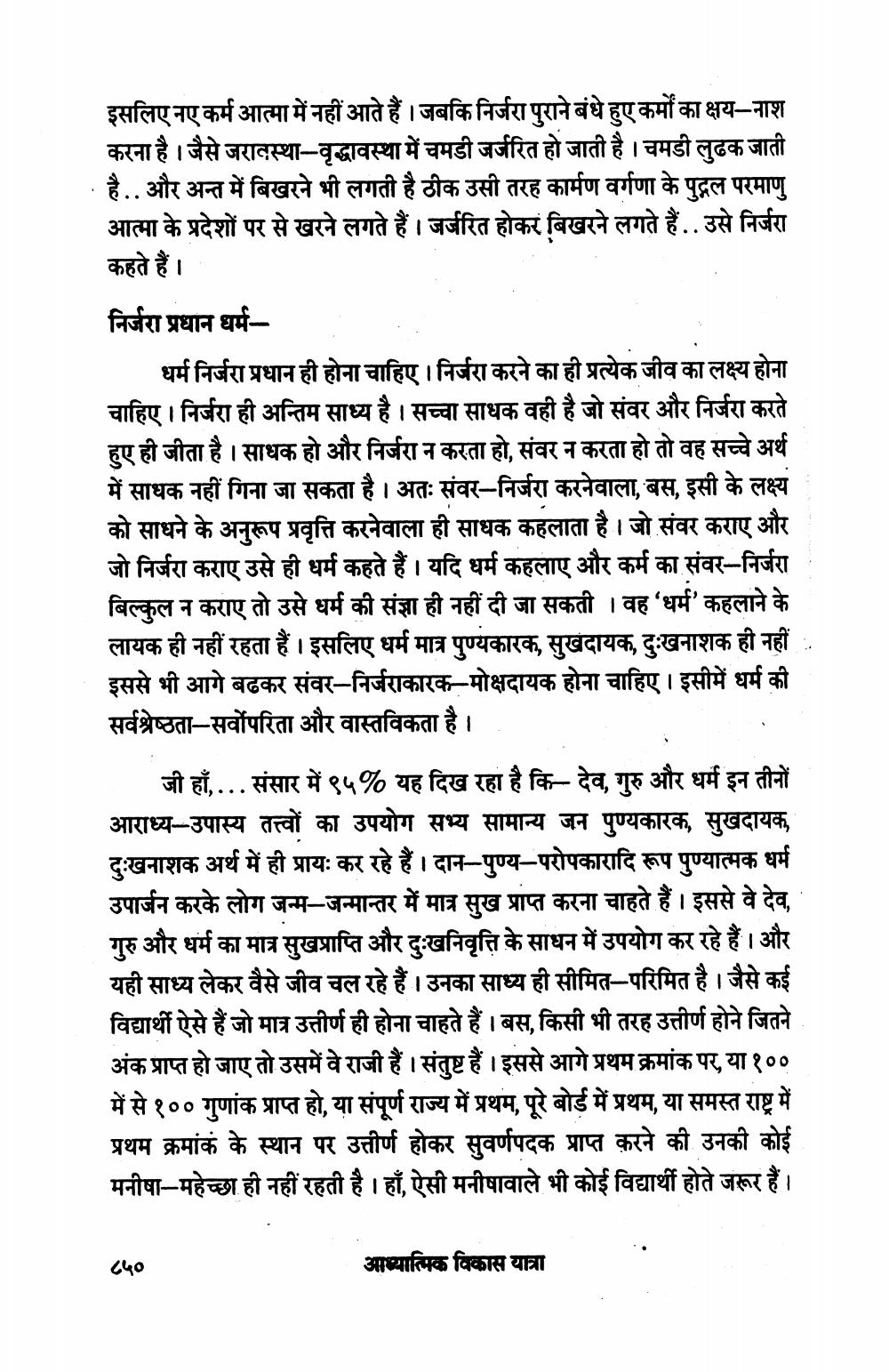________________
इसलिए नए कर्म आत्मा में नहीं आते हैं। जबकि निर्जरा पुराने बंधे हुए कर्मों का क्षय-नाश करना है । जैसे जरावस्था-वृद्धावस्था में चमडी जर्जरित हो जाती है । चमडी लुढक जाती है..और अन्त में बिखरने भी लगती है ठीक उसी तरह कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा के प्रदेशों पर से खरने लगते हैं। जर्जरित होकर बिखरने लगते हैं.. उसे निर्जरा कहते हैं। निर्जरा प्रधान धर्म
धर्म निर्जरा प्रधान ही होना चाहिए । निर्जरा करने का ही प्रत्येक जीव का लक्ष्य होना चाहिए । निर्जरा ही अन्तिम साध्य है । सच्चा साधक वही है जो संवर और निर्जरा करते हुए ही जीता है । साधक हो और निर्जरा न करता हो, संवर न करता हो तो वह सच्चे अर्थ में साधक नहीं गिना जा सकता है। अतः संवर-निर्जरा करनेवाला, बस, इसी के लक्ष्य को साधने के अनुरूप प्रवृत्ति करनेवाला ही साधक कहलाता है । जो संवर कराए और जो निर्जरा कराए उसे ही धर्म कहते हैं। यदि धर्म कहलाए और कर्म का संवर-निर्जरा बिल्कुल न कराए तो उसे धर्म की संज्ञा ही नहीं दी जा सकती । वह 'धर्म' कहलाने के लायक ही नहीं रहता हैं । इसलिए धर्म मात्र पुण्यकारक, सुखदायक, दुःखनाशक ही नहीं इससे भी आगे बढकर संवर-निर्जराकारक-मोक्षदायक होना चाहिए । इसीमें धर्म की सर्वश्रेष्ठता-सर्वोपरिता और वास्तविकता है।
जी हाँ, ... संसार में ९५% यह दिख रहा है कि- देव, गुरु और धर्म इन तीनों आराध्य-उपास्य तत्त्वों का उपयोग सभ्य सामान्य जन पुण्यकारक, सुखदायक, दुःखनाशक अर्थ में ही प्रायः कर रहे हैं। दान-पुण्य-परोपकारादि रूप पुण्यात्मक धर्म उपार्जन करके लोग जन्म-जन्मान्तर में मात्र सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इससे वे देव, गुरु और धर्म का मात्र सुखप्राप्ति और दुःखनिवृत्ति के साधन में उपयोग कर रहे हैं । और यही साध्य लेकर वैसे जीव चल रहे हैं। उनका साध्य ही सीमित-परिमित है । जैसे कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो मात्र उत्तीर्ण ही होना चाहते हैं । बस, किसी भी तरह उत्तीर्ण होने जितने अंक प्राप्त हो जाए तो उसमें वे राजी हैं । संतुष्ट हैं । इससे आगे प्रथम क्रमांक पर, या १०० में से १०० गुणांक प्राप्त हो, या संपूर्ण राज्य में प्रथम, पूरे बोर्ड में प्रथम, या समस्त राष्ट्र में प्रथम क्रमांक के स्थान पर उत्तीर्ण होकर सुवर्णपदक प्राप्त करने की उनकी कोई मनीषा-महेच्छा ही नहीं रहती है । हाँ, ऐसी मनीषावाले भी कोई विद्यार्थी होते जरूर हैं।
८५०
आध्यात्मिक विकास यात्रा