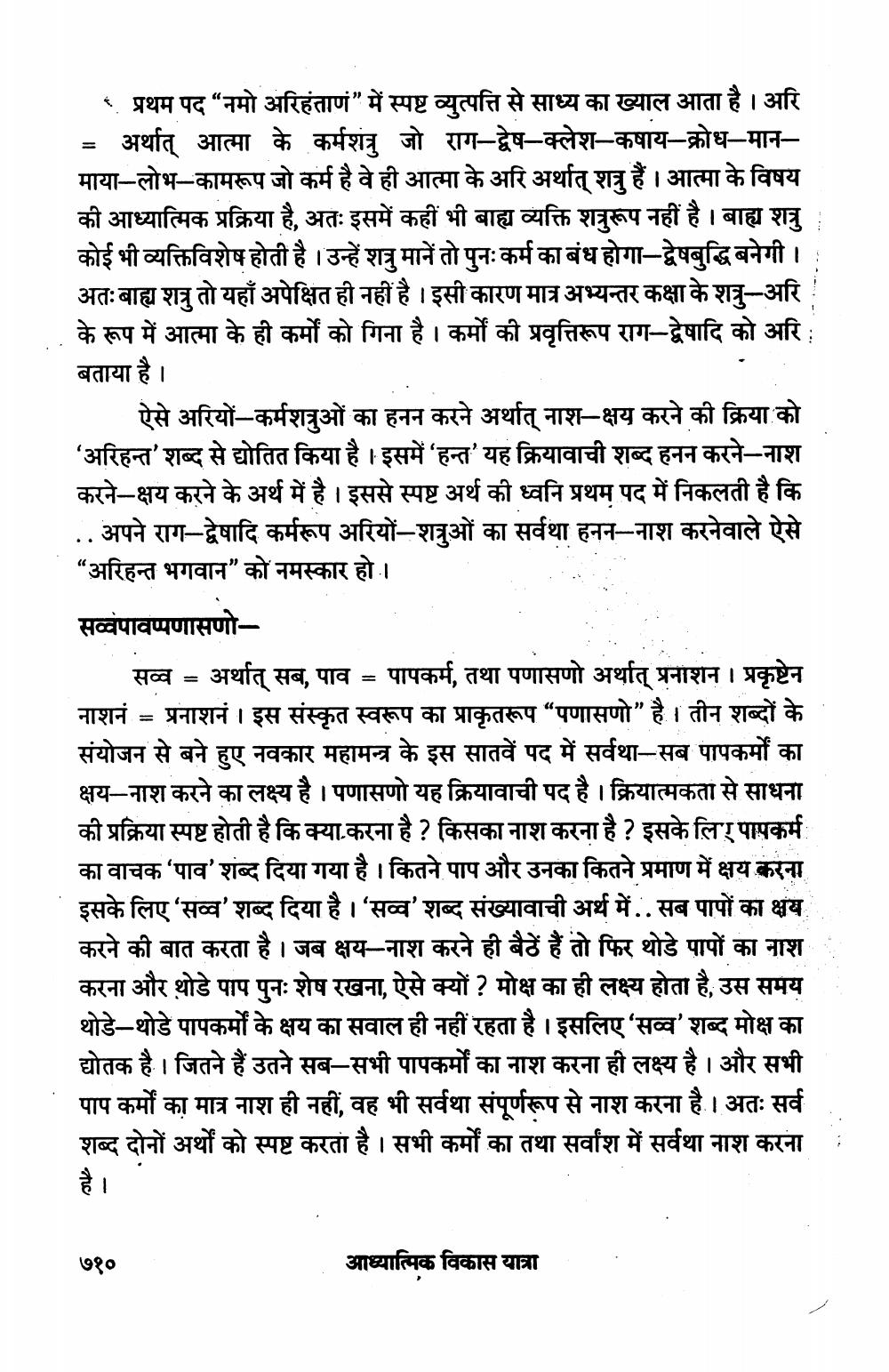________________
• प्रथम पद “नमो अरिहंताणं" में स्पष्ट व्युत्पत्ति से साध्य का ख्याल आता है । अरि = अर्थात् आत्मा के कर्मशत्रु जो राग-द्वेष-क्लेश-कषाय-क्रोध-मानमाया-लोभ-कामरूप जो कर्म है वे ही आत्मा के अरि अर्थात् शत्रु हैं । आत्मा के विषय की आध्यात्मिक प्रक्रिया है, अतः इसमें कहीं भी बाह्य व्यक्ति शत्रुरूप नहीं है । बाह्य शत्रु कोई भी व्यक्तिविशेष होती है । उन्हें शत्रु मानें तो पुनः कर्म का बंध होगा-द्वेषबुद्धि बनेगी। अतः बाह्य शत्रु तो यहाँ अपेक्षित ही नहीं है । इसी कारण मात्र अभ्यन्तर कक्षा के शत्रु-अरि के रूप में आत्मा के ही कर्मों को गिना है । कर्मों की प्रवृत्तिरूप राग-द्वेषादि को अरि : बताया है।
___ऐसे अरियों-कर्मशत्रुओं का हनन करने अर्थात् नाश-क्षय करने की क्रिया को 'अरिहन्त' शब्द से द्योतित किया है । इसमें हन्त' यह क्रियावाची शब्द हनन करने-नाश करने-क्षय करने के अर्थ में है । इससे स्पष्ट अर्थ की ध्वनि प्रथम पद में निकलती है कि .. अपने राग-द्वेषादि कर्मरूप अरियों-शत्रुओं का सर्वथा हनन-नाश करनेवाले ऐसे “अरिहन्त भगवान” को नमस्कार हो। सव्वंपावप्पणासणो
___ सव्व = अर्थात् सब, पाव = पापकर्म, तथा पणासणो अर्थात् प्रनाशन । प्रकृष्टेन नाशनं = प्रनाशनं । इस संस्कृत स्वरूप का प्राकृतरूप “पणासणो" है। तीन शब्दों के संयोजन से बने हुए नवकार महामन्त्र के इस सातवें पद में सर्वथा-सब पापकर्मों का क्षय-नाश करने का लक्ष्य है । पणासणो यह क्रियावाची पद है । क्रियात्मकता से साधना की प्रक्रिया स्पष्ट होती है कि क्या करना है ? किसका नाश करना है ? इसके लिए पापकर्म का वाचक ‘पाव' शब्द दिया गया है । कितने पाप और उनका कितने प्रमाण में क्षय करना इसके लिए 'सव्व' शब्द दिया है। 'सव्व' शब्द संख्यावाची अर्थ में..सब पापों का क्षय करने की बात करता है । जब क्षय-नाश करने ही बैठे हैं तो फिर थोडे पापों का नाश करना और थोडे पाप पुनः शेष रखना, ऐसे क्यों? मोक्ष का ही लक्ष्य होता है, उस समय थोडे-थोडे पापकर्मों के क्षय का सवाल ही नहीं रहता है । इसलिए 'सव्व' शब्द मोक्ष का द्योतक है । जितने हैं उतने सब-सभी पापकर्मों का नाश करना ही लक्ष्य है । और सभी पाप कर्मों का मात्र नाश ही नहीं, वह भी सर्वथा संपूर्णरूप से नाश करना है । अतः सर्व शब्द दोनों अर्थों को स्पष्ट करता है । सभी कर्मों का तथा सर्वांश में सर्वथा नाश करना
७१०
आध्यात्मिक विकास यात्रा