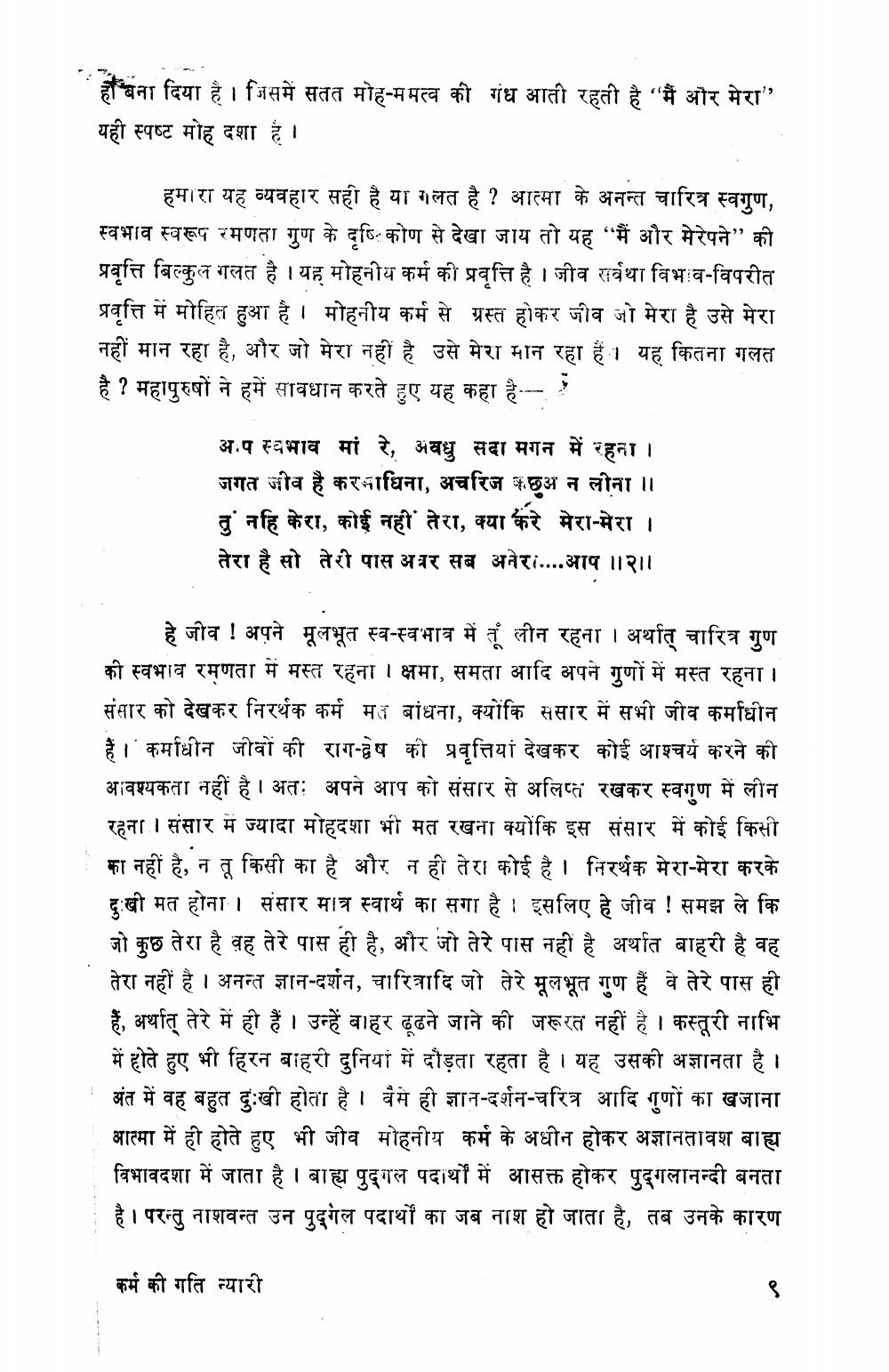________________
ही बना दिया है । जिसमें सतत मोह-ममत्व की गंध आती रहती है “मैं और मेरा' यही स्पष्ट मोह दशा है।
हमारा यह व्यवहार सही है या गलत है ? आत्मा के अनन्त चारित्र स्वगुण, स्वभाव स्वरूप रमणता गुण के दृष्:ि कोण से देखा जाय तो यह “मैं और मेरेपने" की प्रवृत्ति बिल्कुल गलत है । यह मोहनीय कर्म की प्रवृत्ति है । जीव सर्वथा विभाव-विपरीत प्रवृत्ति में मोहित हुआ है । मोहनीय कर्म से ग्रस्त होकर जीव जो मेरा है उसे मेरा नहीं मान रहा है, और जो मेरा नहीं है उसे मेरा मान रहा हैं । यह कितना गलत है ? महापुरुषों ने हमें सावधान करते हुए यह कहा है.--.
अ.प स्वभाव मां रे, अवधु सदा मगन में रहना । जगत जीव है करमाधिना, अचरिज कछुअ न लीना ।। तु नहि केरा, कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा-मेरा । तेरा है सो तेरी पास अवर सब अनेर....आप ॥२।।
हे जीव ! अपने मूलभूत स्व-स्वभाव में तूं लीन रहना । अर्थात् चारित्र गुण की स्वभाव रमणता में मस्त रहना । क्षमा, समता आदि अपने गुणों में मस्त रहना। संसार को देखकर निरर्थक कर्म मत बांधना, क्योंकि संसार में सभी जीव कर्माधीन हैं। कर्माधीन जीवों की राग-द्वेष की प्रवृत्तियां देखकर कोई आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है । अतः अपने आप को संसार से अलिप्त रखकर स्वगुण में लीन रहना । संसार में ज्यादा मोहदशा भी मत रखना क्योंकि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, न तू किसी का है और न ही तेरा कोई है। निरर्थक मेरा-मेरा करके दुःखी मत होना। संसार मात्र स्वार्थ का सगा है। इसलिए हे जीव ! समझ ले कि जो कुछ तेरा है वह तेरे पास ही है, और जो तेरे पास नहीं है अर्थात बाहरी है वह तेरा नहीं है । अनन्त ज्ञान-दर्शन, चारित्रादि जो तेरे मूलभूत गुण हैं वे तेरे पास ही हैं, अर्थात् तेरे में ही हैं। उन्हें बाहर ढूढने जाने की जरूरत नहीं है । कस्तूरी नाभि में होते हुए भी हिरन बाहरी दुनियां में दौड़ता रहता है । यह उसकी अज्ञानता है। अंत में वह बहुत दुःखी होता है । वैसे ही ज्ञान-दर्शन-चरित्र आदि गुणों का खजाना आत्मा में ही होते हुए भी जीव मोहनीय कर्म के अधीन होकर अज्ञानतावश बाह्य विभावदशा में जाता है । बाह्य पुद्गल पदार्थों में आसक्त होकर पुद्गलानन्दी बनता है । परन्तु नाशवन्त उन पुद्गल पदार्थों का जब नाश हो जाता है, तब उनके कारण
कर्म की गति न्यारी