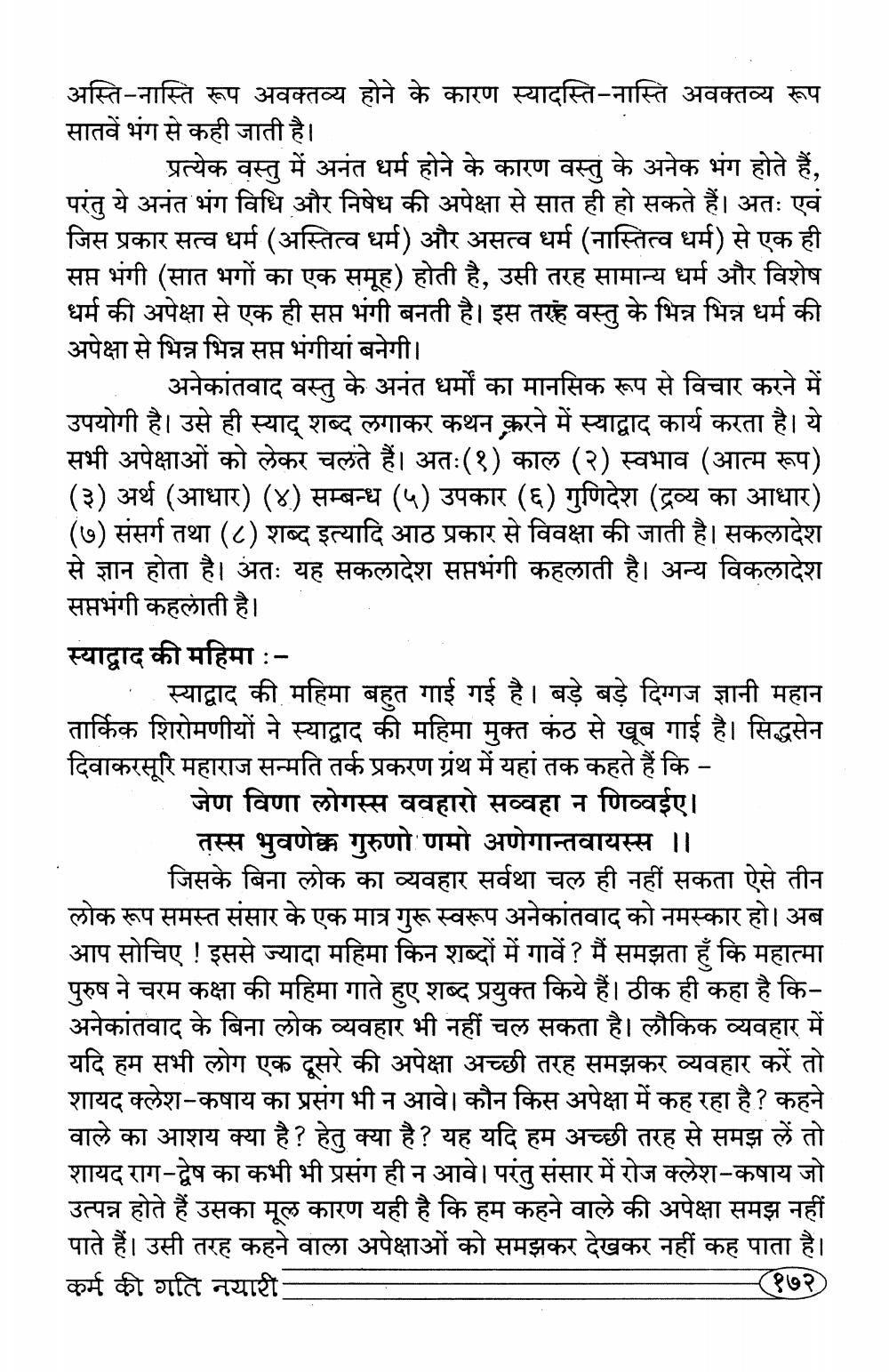________________
अस्ति-नास्ति रूप अवक्तव्य होने के कारण स्यादस्ति-नास्ति अवक्तव्य रूप सातवें भंग से कही जाती है।
प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म होने के कारण वस्तु के अनेक भंग होते हैं, परंतु ये अनंत भंग विधि और निषेध की अपेक्षा से सात ही हो सकते हैं। अतः एवं जिस प्रकार सत्व धर्म (अस्तित्व धर्म) और असत्व धर्म (नास्तित्व धर्म) से एक ही सप्त भंगी (सात भगों का एक समूह) होती है, उसी तरह सामान्य धर्म और विशेष धर्म की अपेक्षा से एक ही सप्त भंगी बनती है। इस तरह वस्तु के भिन्न भिन्न धर्म की अपेक्षा से भिन्न भिन्न सप्त भंगीयां बनेगी।
___ अनेकांतवाद वस्तु के अनंत धर्मों का मानसिक रूप से विचार करने में उपयोगी है। उसे ही स्याद् शब्द लगाकर कथन करने में स्याद्वाद कार्य करता है। ये सभी अपेक्षाओं को लेकर चलते हैं। अतः (१) काल (२) स्वभाव (आत्म रूप) (३) अर्थ (आधार) (४) सम्बन्ध (५) उपकार (६) गुणिदेश (द्रव्य का आधार) (७) संसर्ग तथा (८) शब्द इत्यादि आठ प्रकार से विवक्षा की जाती है। सकलादेश से ज्ञान होता है। अतः यह सकलादेश सप्तभंगी कहलाती है। अन्य विकलादेश सप्तभंगी कहलाती है। स्याद्वाद की महिमा :
__ स्याद्वाद की महिमा बहुत गाई गई है। बड़े बड़े दिग्गज ज्ञानी महान तार्किक शिरोमणीयों ने स्याद्वाद की महिमा मुक्त कंठ से खूब गाई है। सिद्धसेन दिवाकरसूरि महाराज सन्मति तर्क प्रकरण ग्रंथ में यहां तक कहते हैं कि -
जेण विणा लोगस्स ववहारो सव्वहा न णिव्वईए।
तस्स भुवणेक्क गुरुणो णमो अणेगान्तवायस्स ।।
जिसके बिना लोक का व्यवहार सर्वथा चल ही नहीं सकता ऐसे तीन लोक रूप समस्त संसार के एक मात्र गुरू स्वरूप अनेकांतवाद को नमस्कार हो। अब आप सोचिए ! इससे ज्यादा महिमा किन शब्दों में गावें? मैं समझता हूँ कि महात्मा पुरुष ने चरम कक्षा की महिमा गाते हुए शब्द प्रयुक्त किये हैं। ठीक ही कहा है किअनेकांतवाद के बिना लोक व्यवहार भी नहीं चल सकता है। लौकिक व्यवहार में यदि हम सभी लोग एक दूसरे की अपेक्षा अच्छी तरह समझकर व्यवहार करें तो शायद क्लेश-कषाय का प्रसंग भी न आवे। कौन किस अपेक्षा में कह रहा है? कहने वाले का आशय क्या है ? हेतु क्या है? यह यदि हम अच्छी तरह से समझ लें तो शायद राग-द्वेष का कभी भी प्रसंग ही न आवे। परंतु संसार में रोज क्लेश-कषाय जो उत्पन्न होते हैं उसका मूल कारण यही है कि हम कहने वाले की अपेक्षा समझ नहीं पाते हैं। उसी तरह कहने वाला अपेक्षाओं को समझकर देखकर नहीं कह पाता है। कर्म की गति नयारी
(१७२)