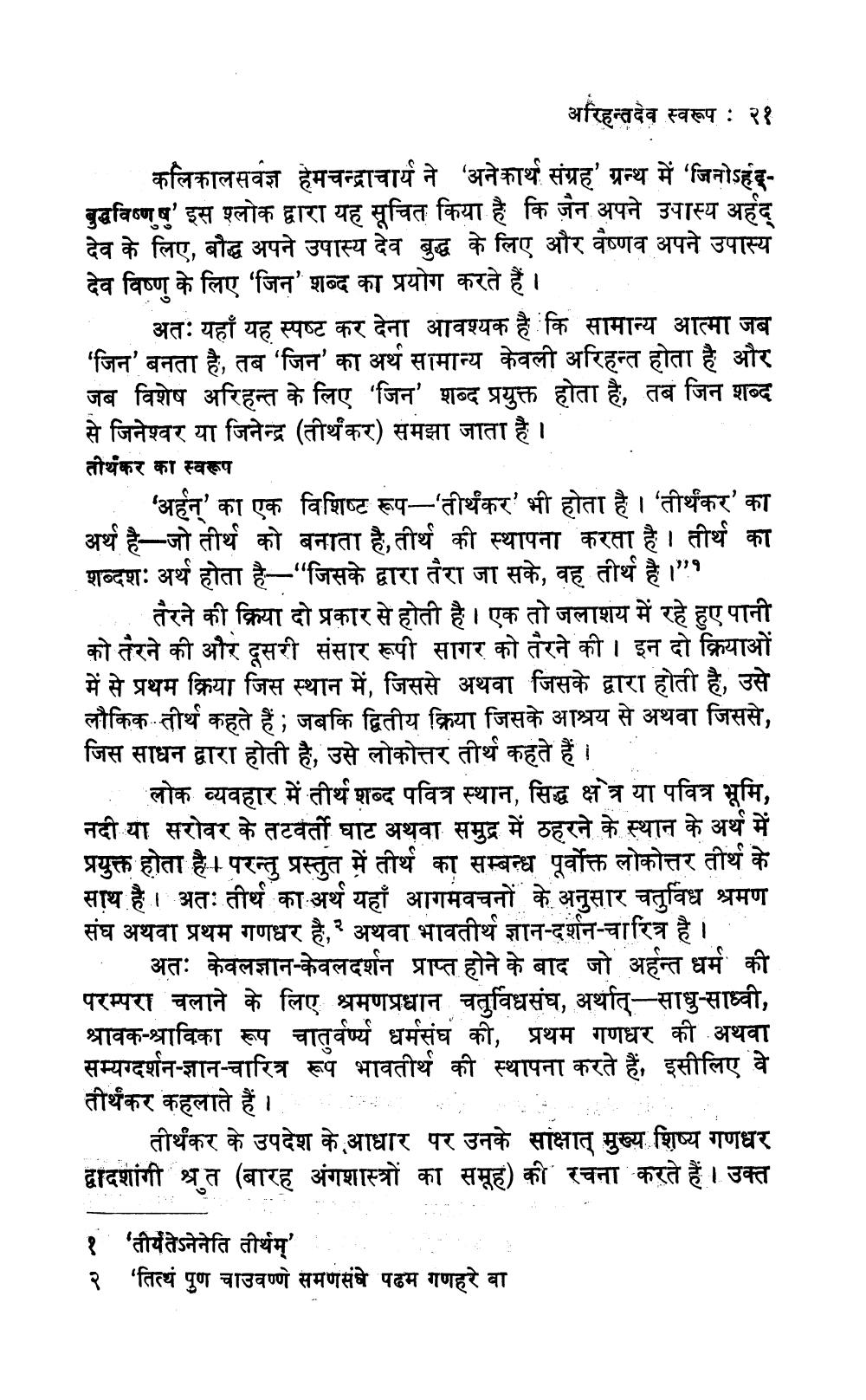________________
अरिहन्तदेव स्वरूप : २१
कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य ने 'अनेकार्थ संग्रह ' ग्रन्थ में 'जिनोऽहंदूबुद्धविष्णषु' इस श्लोक द्वारा यह सूचित किया है कि जैन अपने उपास्य अर्हद् देव के लिए, बौद्ध अपने उपास्य देव बुद्ध के लिए और वैष्णव अपने उपास्य देव विष्णु के लिए 'जिन' शब्द का प्रयोग करते हैं ।
अतः यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सामान्य आत्मा जब 'जिन' बनता है, तब 'जिन' का अर्थ सामान्य केवली अरिहन्त होता है और जब विशेष अरिहन्त के लिए 'जिन' शब्द प्रयुक्त होता है, तब जिन शब्द से जिनेश्वर या जिनेन्द्र (तीर्थंकर) समझा जाता है ।
तीर्थंकर का स्वरूप
'अर्हन्' का एक विशिष्ट रूप - 'तीर्थंकर' भी होता है । 'तीर्थंकर' का अर्थ है— जो तीर्थ को बनाता है, तीर्थ की स्थापना करता है । तीर्थ का शब्दशः अर्थ होता है- " जिसके द्वारा तैरा जा सके, वह तीर्थ है ।"१
तैरने की क्रिया दो प्रकार से होती है । एक तो जलाशय में रहे हुए पानी को तैरने की और दूसरी संसार रूपी सागर को तैरने की । इन दो क्रियाओं प्रथम क्रिया जिस स्थान में, जिससे अथवा जिसके द्वारा होती है, उसे लौकिक तीर्थ कहते हैं; जबकि द्वितीय क्रिया जिसके आश्रय से अथवा जिससे, जिस साधन द्वारा होती है, उसे लोकोत्तर तीर्थ कहते हैं ।
लोक व्यवहार में तीर्थ शब्द पवित्र स्थान, सिद्ध क्ष ेत्र या पवित्र भूमि, नदी या सरोवर के तटवर्ती घाट अथवा समुद्र में ठहरने के स्थान के अर्थ में प्रयुक्त होता है । परन्तु प्रस्तुत में तीर्थ का सम्बन्ध पूर्वोक्त लोकोत्तर तीर्थ के साथ है । अतः तीर्थ का अर्थ यहाँ आगमवचनों के अनुसार चतुविध श्रमण संघ अथवा प्रथम गणधर है, ' अथवा भावतीर्थ ज्ञान दर्शन- चारित्र है ।
अतः केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त होने के बाद जो अर्हन्त धर्म की परम्परा चलाने के लिए श्रमणप्रधान चतुविधसंघ, अर्थात् – साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका रूप चातुर्वर्ण्य धर्मसंघ की प्रथम गणधर की अथवा सम्यग्दर्शन - ज्ञान - चारित्र रूप भावतीर्थ की स्थापना करते हैं, इसीलिए वे तीर्थंकर कहलाते हैं ।
तीर्थंकर के उपदेश के आधार पर उनके साक्षात् मुख्य शिष्य गणधर द्वादशांगी श्रुत (बारह अंगशास्त्रों का समूह ) की रचना करते हैं । उक्त
१ ' तीर्यतेऽनेनेति तीर्थम्'
२
' तित्थं पुण चाउवण्णे समणसंघे पढम गणहरे बा