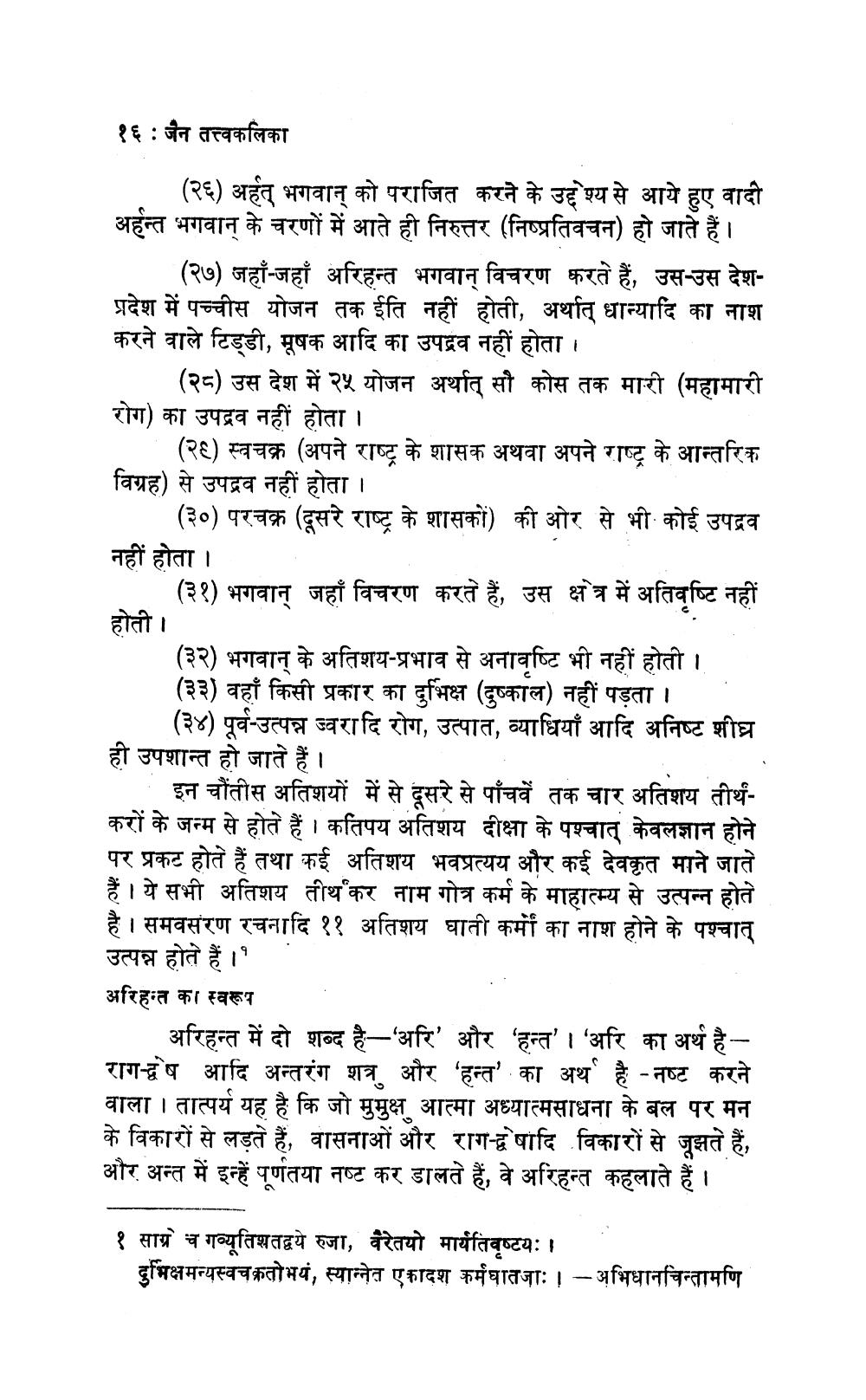________________
१६ : जैन तत्त्वकलिका
(२६) अर्हत् भगवान् को पराजित करने के उद्देश्य से आये हुए वादी अर्हन्त भगवान् के चरणों में आते ही निरुत्तर (निष्प्रतिवचन) हो जाते हैं । (२७) जहाँ-जहाँ अरिहन्त भगवान् विचरण करते हैं, उस उस देशप्रदेश में पच्चीस योजन तक ईति नहीं होती, अर्थात् धान्यादि का नाश करने वाले टिड्डी, मूषक आदि का उपद्रव नहीं होता ।
(२८) उस देश में २५ योजन अर्थात् सो कोस तक मारी ( महामारी रोग) का उपद्रव नहीं होता ।
(२९) स्वचक्र (अपने राष्ट्र के शासक अथवा अपने राष्ट्र के आन्तरिक विग्रह ) से उपद्रव नहीं होता ।
(३०) परचक्र (दूसरे राष्ट्र के शासकों) की ओर से भी कोई उपद्रव नहीं होता ।
(३१) भगवान् जहाँ विचरण करते हैं, उस क्षेत्र में अतिवृष्टि नहीं
होती ।
(३२) भगवान् के अतिशय प्रभाव से अनावृष्टि भी नहीं होती । (३३) वहाँ किसी प्रकार का दुर्भिक्ष (दुष्काल) नहीं पड़ता । (३४) पूर्व उत्पन्न ज्वरादि रोग, उत्पात, व्याधियाँ आदि अनिष्ट शीघ्र ही उपशान्त हो जाते हैं ।
इन चौंतीस अतिशयों में से दूसरे से पाँचवें तक चार अतिशय तीर्थं - करों के जन्म से होते हैं । कतिपय अतिशय दीक्षा के पश्चात् केवलज्ञान होने पर प्रकट होते हैं तथा कई अतिशय भवप्रत्यय और कई देवकृत माने जाते हैं । ये सभी अतिशय तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म के माहात्म्य से उत्पन्न होते है । समवसरण रचनादि ११ अतिशय घाती कर्मों का नाश होने के पश्चात् उत्पन्न होते हैं । "
1
अरिहन्त का स्वरूप
अरिहन्त में दो शब्द है - 'अरि' और 'हन्त' । 'अरि का अर्थ है - राग-द्वेष आदि अन्तरंग शत्रु और 'हन्त' का अर्थ है - नष्ट करने वाला । तात्पर्य यह है कि जो मुमुक्ष आत्मा अध्यात्मसाधना के बल पर मन के विकारों से लड़ते हैं, वासनाओं और राग-द्वेषादि विकारों से जूझते हैं, और अन्त में इन्हें पूर्णतया नष्ट कर डालते हैं, वे अरिहन्त कहलाते हैं ।
१ साग्रे च गव्यूतिशतद्वये रुजा, वैरेतयो मार्यतिवृष्टयः ।
दुर्भिक्ष मन्यस्वचक्रतोभयं स्यान्नेत एकादश कर्मघातजाः ।
,
- अभिधानचिन्तामणि
-