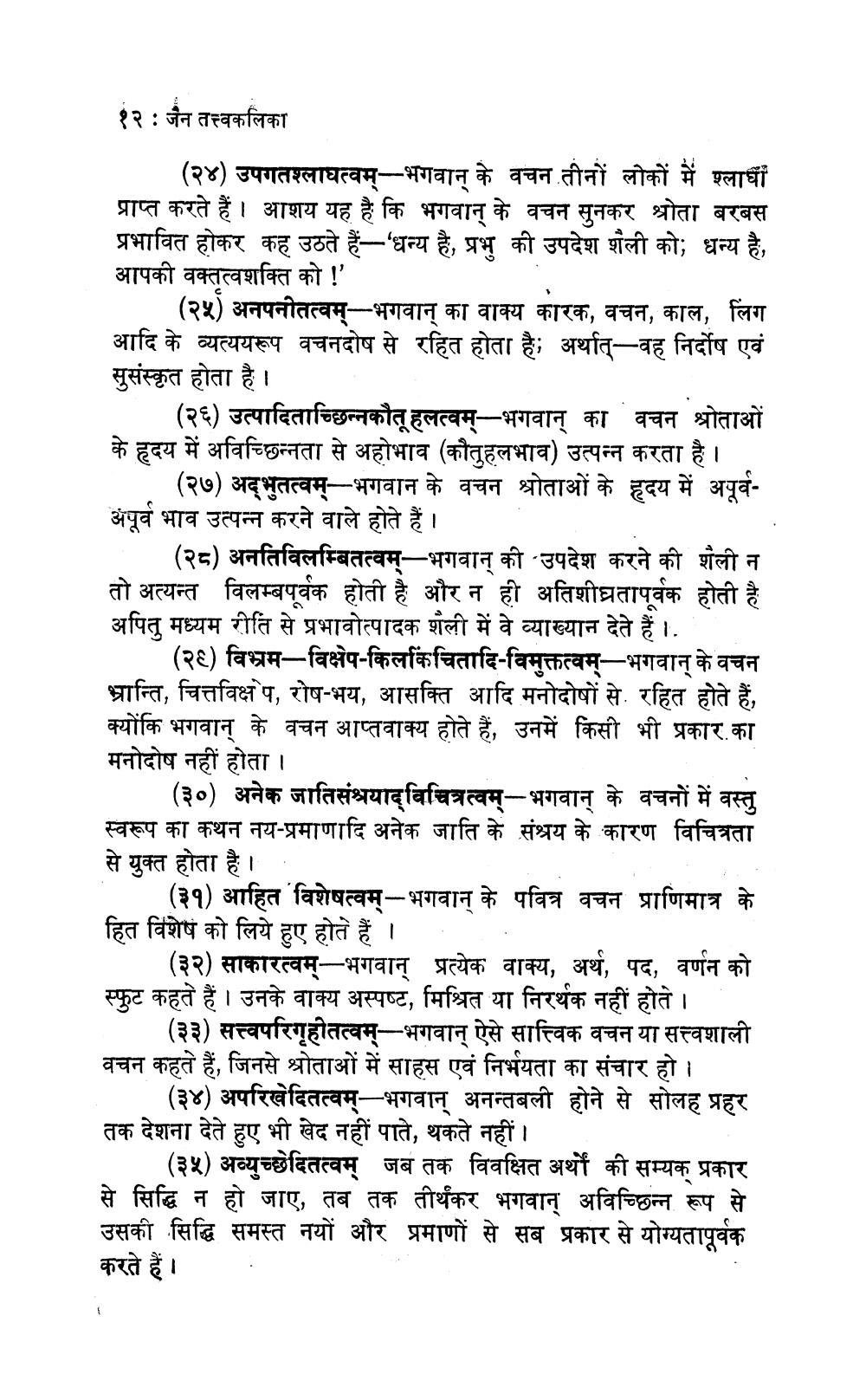________________
१२ : जैन तत्त्वकलिका
(२४) उपगतश्लाघत्वम् - भगवान् के वचन तीनों लोकों में श्लाघाँ प्राप्त करते हैं । आशय यह है कि भगवान् के वचन सुनकर श्रोता बरबस प्रभावित होकर कह उठते हैं - 'धन्य है, प्रभु की उपदेश शैली को; धन्य है, आपकी वक्तत्वशक्ति को !'
(२५) अनपनीतत्वम्—भगवान् का वाक्य कारक, वचन, काल, लिंग आदि के व्यत्ययरूप वचनदोष से रहित होता है; अर्थात् — वह निर्दोष एवं सुसंस्कृत होता है ।
(२६) उत्पादिताच्छिन्नकौतूहलत्वम् — भगवान् का वचन श्रोताओं के हृदय में अविच्छिन्नता से अहोभाव ( कौतुहलभाव) उत्पन्न करता है । (२७) अद्भुतत्वम् — भगवान के वचन श्रोताओं के हृदय में अपूर्व - अपूर्व भाव उत्पन्न करने वाले होते हैं ।
(२८) अनतिविलम्बितत्वम् - भगवान् की उपदेश करने की शैली न तो अत्यन्त विलम्बपूर्वक होती है और न ही अतिशीघ्रतापूर्वक होती है अपितु मध्यम रीति से प्रभावोत्पादक शैली में वे व्याख्यान देते हैं ।.
(२९) विभ्रम - विक्षेप - किलकिचितादि-विमुक्तत्वम् —भगवान् के वचन भ्रान्ति, चित्तविक्ष ेप, रोष-भय, आसक्ति आदि मनोदोषों से रहित होते हैं, क्योंकि भगवान् के वचन आप्तवाक्य होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का मनोदोष नहीं होता ।
(३०) अनेक जातिसंश्रया विचित्रत्वम् - भगवान् के वचनों में वस्तु स्वरूप का कथन नय- प्रमाणादि अनेक जाति के संश्रय के कारण विचित्रता से युक्त होता है ।
(३१) आहित विशेषत्वम् - भगवान् के पवित्र वचन प्राणिमात्र के हित विशेष को लिये हुए होते हैं ।
(३२) साकारत्वम्—भगवान् प्रत्येक वाक्य, अर्थ, पद, वर्णन को स्फुट कहते हैं । उनके वाक्य अस्पष्ट, मिश्रित या निरर्थक नहीं होते ।
(३३) सत्त्वपरिगृहीतत्वम् - भगवान् ऐसे सात्त्विक वचन या सत्त्वशाली वचन कहते हैं, जिनसे श्रोताओं में साहस एवं निर्भयता का संचार हो ।
(३४) अपरिखेदितत्वम् - भगवान् अनन्तबली होने से सोलह प्रहर तक देशना देते हुए भी खेद नहीं पाते, थकते नहीं ।
(३५) अव्युच्छेदितत्वम् जब तक विवक्षित अर्थों की सम्यक् प्रकार से सिद्धि न हो जाए, तब तक तीर्थंकर भगवान् अविच्छिन्न रूप से उसकी सिद्धि समस्त नयों और प्रमाणों से सब प्रकार से योग्यतापूर्वक करते हैं ।