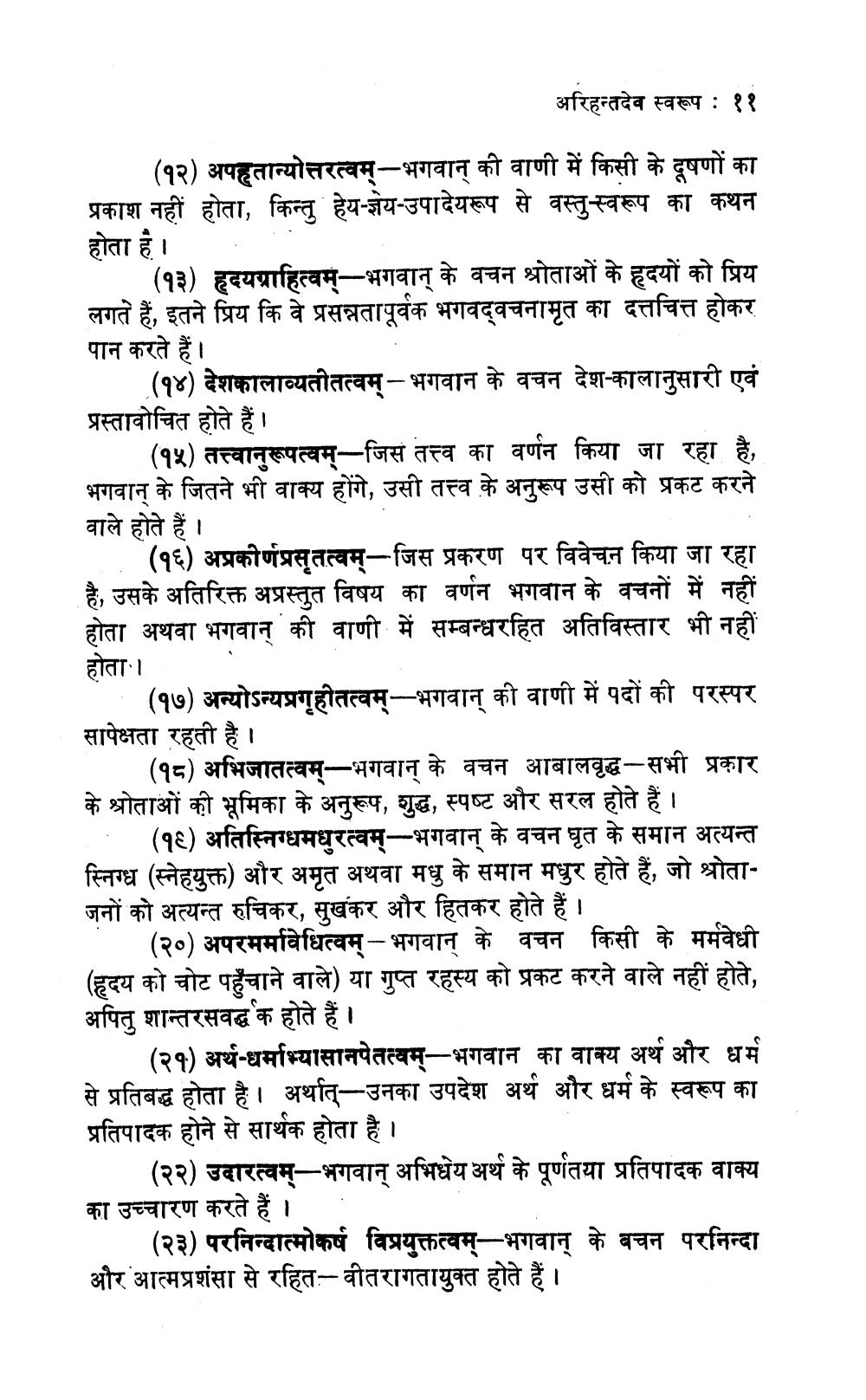________________
अरिहन्तदेव स्वरूप : ११
(१२) अपहृतान्योत्तरत्वम् - भगवान् की वाणी में किसी के दूषणों का प्रकाश नहीं होता, किन्तु हेय-ज्ञेय - उपादेयरूप से वस्तु स्वरूप का कथन होता है।
-
(१३) हृदयग्राहित्वम् — भगवान् के वचन श्रोताओं के हृदयों को प्रिय लगते हैं, इतने प्रिय कि वे प्रसन्नतापूर्वक भगवद्वचनामृत का दत्तचित्त होकर पान करते हैं ।
(१४) देशकालाव्यतीतत्वम् भगवान के वचन देश - कालानुसारी एवं प्रस्तावोचित होते हैं ।
-
(१५) तत्त्वानुरूपत्वम् — जिस तत्त्व का वर्णन किया जा रहा है, भगवान् के जितने भी वाक्य होंगे, उसी तत्त्व के अनुरूप उसी को प्रकट करने वाले होते हैं ।
(१६) अप्रकीर्णप्रसृतत्वम् - जिस प्रकरण पर विवेचन किया जा रहा है, उसके अतिरिक्त अप्रस्तुत विषय का वर्णन भगवान के वचनों में नहीं होता अथवा भगवान् की वाणी में सम्बन्धरहित अतिविस्तार भी नहीं होता ।
(१७) अन्योऽन्यप्रगृहीतत्वम् - भगवान् की वाणी में पदों की परस्पर सापेक्षता रहती है ।
(१८) अभिजातत्वम् - भगवान् के वचन आबालवृद्ध - सभी प्रकार श्रोताओं की भूमिका के अनुरूप, शुद्ध, स्पष्ट और सरल होते हैं ।
(१६) अतिस्निग्धमधुरत्वम् - भगवान् के वचन घृत के समान अत्यन्त स्निग्ध (स्नेहयुक्त) और अमृत अथवा मधु के समान मधुर होते हैं, जो श्रोताजनों को अत्यन्त रुचिकर, सुखकर और हितकर होते हैं ।
(२०) अपरमर्मावेधित्वम् - भगवान् के वचन किसी के मर्मवेधी (हृदय को चोट पहुँचाने वाले) या गुप्त रहस्य को प्रकट करने वाले नहीं होते, अपितु शान्तरसवद्ध के होते हैं ।
(२१) अर्थ - धर्माभ्यासानपेतत्वम् - भगवान का वाक्य अर्थ और धर्म से प्रतिबद्ध होता है । अर्थात् — उनका उपदेश अर्थ और धर्म के स्वरूप का प्रतिपादक होने से सार्थक होता है ।
(२२) उदारत्वम् — भगवान् अभिधेय अर्थ के पूर्णतया प्रतिपादक वाक्य का उच्चारण करते हैं ।
(२३) परनिन्दात्मोकर्ष विप्रयुक्तत्वम् - भगवान् के बचन परनिन्दा और आत्मप्रशंसा से रहित - वीतरागतायुक्त होते हैं ।