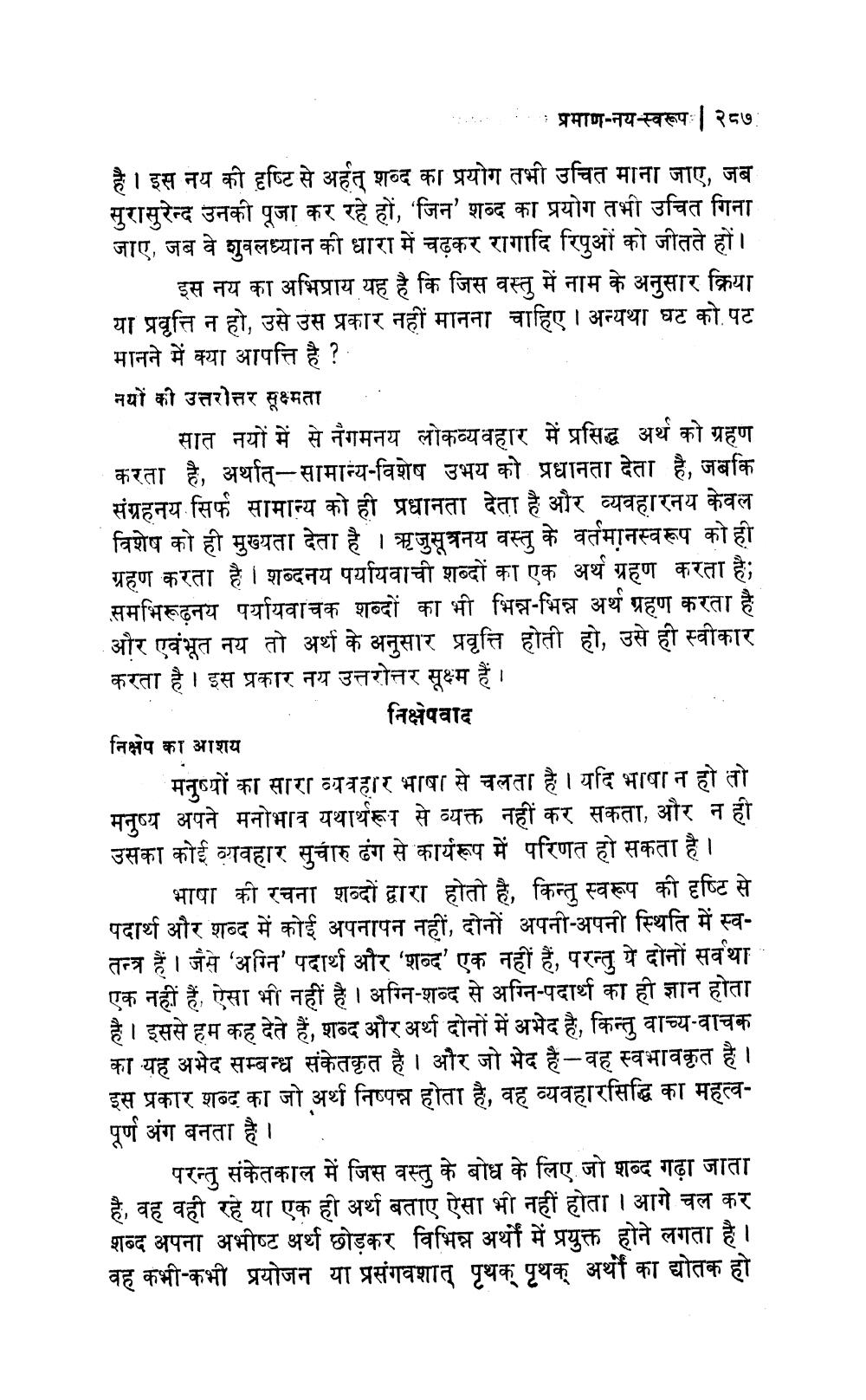________________
प्रमाण - नय - स्वरूपः | २८७ :
है । इस नय की दृष्टि से अर्हतु शब्द का प्रयोग तभी उचित माना जाए, जब सुरासुरेन्द उनकी पूजा कर रहे हों, 'जिन' शब्द का प्रयोग तभी उचित गिना जाए, जब वे शुवलध्यान की धारा में चढ़कर रागादि रिपुओं को जीतते हों ।
इस नय का अभिप्राय यह है कि जिस वस्तु में नाम के अनुसार क्रिया या प्रवृत्ति न हो, उसे उस प्रकार नहीं मानना चाहिए । अन्यथा घट को पट मानने में क्या आपत्ति है ?
नयों को उत्तरोत्तर सूक्ष्मता
सात नयों में से नैगमनय लोकव्यवहार में प्रसिद्ध अर्थ को ग्रहण करता है, अर्थात् - सामान्य- विशेष उभय को प्रधानता देता है, जबकि संग्रहनय सिर्फ सामान्य को ही प्रधानता देता है और व्यवहारनय केवल विशेष को ही मुख्यता देता है । ऋजुसूत्रनय वस्तु के वर्तमानस्वरूप को ही | शब्दनय पर्यायवाची शब्दों का एक अर्थ ग्रहण करता है; ग्रहण करता समभिरूढ़नय पर्यायवाचक शब्दों का भी भिन्न-भिन्न अर्थ ग्रहण करता है और एवंभूत नय तो अर्थ के अनुसार प्रवृत्ति होती हो, उसे ही स्वीकार करता है । इस प्रकार नय उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं ।
निक्षेपवाद
निक्षेप का आशय
मनुष्यों का सारा व्यवहार भाषा से चलता है । यदि भाषा न हो तो मनुष्य अपने मनोभाव यथार्थरूप से व्यक्त नहीं कर सकता, और न ही उसका कोई व्यवहार सुचारु ढंग से कार्यरूप में परिणत हो सकता है ।
भाषा की रचना शब्दों द्वारा होती है, किन्तु स्वरूप की दृष्टि से पदार्थ और शब्द में कोई अपनापन नहीं, दोनों अपनी-अपनी स्थिति में स्वतन्त्र हैं । जैसे 'अग्नि' पदार्थ और 'शब्द' एक नहीं हैं, परन्तु ये दोनों सर्वथा एक नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है । अग्नि शब्द से अग्नि-पदार्थ का ही ज्ञान होता है । इससे हम कह देते हैं, शब्द और अर्थ दोनों में अभेद है, किन्तु वाच्य वाचक का यह अभेद सम्बन्ध संकेतकृत है । और जो भेद हैं - वह स्वभावकृत है । इस प्रकार शब्द का जो अर्थ निष्पन्न होता है, वह व्यवहारसिद्धि का महत्व - पूर्ण अंग बनता है ।
परन्तु संकेतकाल में जिस वस्तु के बोध के लिए जो शब्द गढ़ा जाता है, वह वही रहे या एक ही अर्थ बताए ऐसा भी नहीं होता । आगे चल कर शब्द अपना अभीष्ट अर्थ छोड़कर विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने लगता है । वह कभी-कभी प्रयोजन या प्रसंगवशात् पृथक् पृथक् अर्थों का द्योतक हो