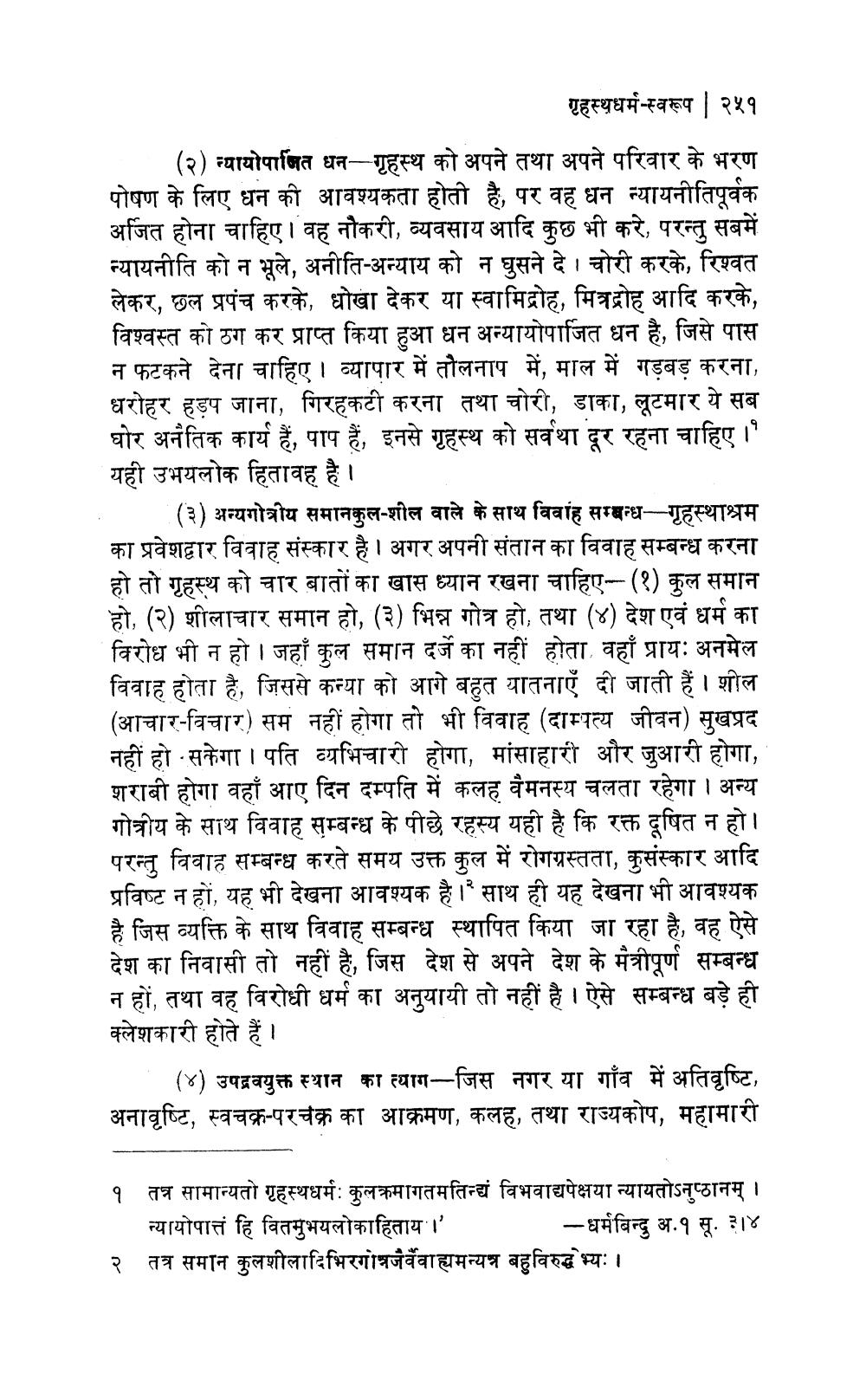________________
गृहस्थधर्म-स्वरूप | २५१ (२) न्यायोपार्जित धन-गृहस्थ को अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए धन की आवश्यकता होती है, पर वह धन न्यायनीतिपूर्वक अर्जित होना चाहिए। वह नौकरी, व्यवसाय आदि कुछ भी करे, परन्तु सबमें न्यायनीति को न भूले, अनीति-अन्याय को न घुसने दे। चोरी करके, रिश्वत लेकर, छल प्रपंच करके, धोखा देकर या स्वामिद्रोह, मित्रद्रोह आदि करके, विश्वस्त को ठग कर प्राप्त किया हुआ धन अन्यायोपार्जित धन है, जिसे पास न फटकने देना चाहिए। व्यापार में तौलनाप में, माल में गड़बड़ करना, धरोहर हड़प जाना, गिरहकटी करना तथा चोरी, डाका, लूटमार ये सब घोर अनैतिक कार्य हैं, पाप हैं, इनसे गृहस्थ को सर्वथा दूर रहना चाहिए।' यही उभयलोक हितावह है। . (३) अन्यगोत्रीय समानकुल-शील वाले के साथ विवाह सम्बन्ध-गृहस्थाश्रम का प्रवेशद्वार विवाह संस्कार है । अगर अपनी संतान का विवाह सम्बन्ध करना हो तो गृहस्थ को चार बातों का खास ध्यान रखना चाहिए-(१) कूल समान हो, (२) शीलाचार समान हो, (३) भिन्न गोत्र हो, तथा (४) देश एवं धर्म का विरोध भी न हो । जहाँ कूल समान दर्जे का नहीं होता, वहाँ प्रायः अनमेल विवाह होता है, जिससे कन्या को आगे बहत यातनाएँ दी जाती हैं। शील (आचार-विचार) सम नहीं होगा तो भी विवाह (दाम्पत्य जीवन) सुखप्रद नहीं हो सकेगा। पति व्यभिचारी होगा, मांसाहारी और जुआरी होगा, शराबी होगा वहाँ आए दिन दम्पति में कलह वैमनस्य चलता रहेगा । अन्य गोत्रीय के साथ विवाह सम्बन्ध के पीछे रहस्य यही है कि रक्त दूषित न हो। परन्तु विवाह सम्बन्ध करते समय उक्त कुल में रोगग्रस्तता, कुसंस्कार आदि प्रविष्ट न हों, यह भी देखना आवश्यक है। साथ ही यह देखना भी आवश्यक है जिस व्यक्ति के साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित किया जा रहा है, वह ऐसे देश का निवासी तो नहीं है, जिस देश से अपने देश के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध न हों, तथा वह विरोधी धर्म का अनुयायी तो नहीं है । ऐसे सम्बन्ध बड़े ही क्लेशकारी होते हैं।
(४) उपद्रवयुक्त स्थान का त्याग-जिस नगर या गाँव में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, स्वचक्र-परचक्र का आक्रमण, कलह, तथा राज्यकोप, महामारी
१ तत्र सामान्यतो गृहस्थधर्मः कुलक्रमागतमतिन्द्यं विभवाद्यपेक्षया न्यायतोऽनुष्ठानम् ।
न्यायोपात्तं हि वितमुभयलोकाहिताय ।' -धर्मबिन्दु अ.१ सू. ३।४ २ तत्र समान कुलशीलादिभिरगोत्रजर्वैवाह्यमन्यत्र बहुविरुद्ध भ्यः ।