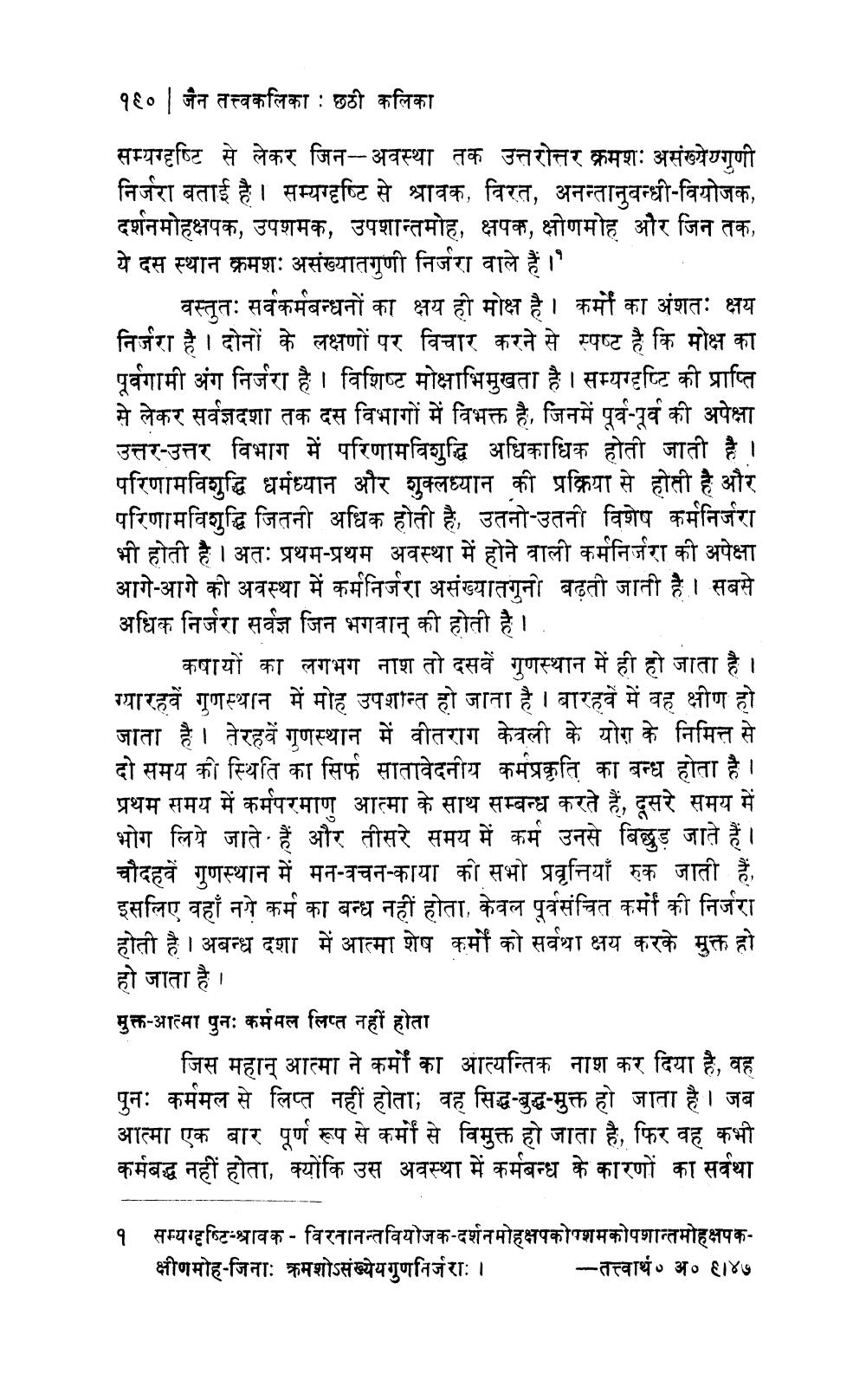________________
१६० | जैन तत्त्वकलिका : छठी कलिका सम्यग्दृष्टि से लेकर जिन-अवस्था तक उत्तरोत्तर क्रमशः असंख्येग्गुणी निर्जरा बताई है। सम्यग्दृष्टि से श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धी-वियोजक, दर्शनमोहक्षपक, उपशमक, उपशान्तमोह, क्षपक, क्षोणमोह और जिन तक, ये दस स्थान क्रमशः असंख्यातगुणी निर्जरा वाले हैं।'
___ वस्तुतः सर्वकर्मबन्धनों का क्षय ही मोक्ष है। कर्मों का अंशतः क्षय निर्जरा है । दोनों के लक्षणों पर विचार करने से स्पष्ट है कि मोक्ष का पूर्वगामी अंग निर्जरा है। विशिष्ट मोक्षाभिमुखता है। सम्यग्दृष्टि की प्राप्ति से लेकर सर्वज्ञदशा तक दस विभागों में विभक्त है, जिनमें पूर्व-पूर्व की अपेक्षा उत्तर-उत्तर विभाग में परिणामविशुद्धि अधिकाधिक होती जाती है। परिणामविशुद्धि धर्मध्यान और शुक्लध्यान की प्रक्रिया से होती है और परिणामविशुद्धि जितनी अधिक होती है, उतनो-उतनी विशेष कर्मनिर्जरा भी होती है । अतः प्रथम-प्रथम अवस्था में होने वाली कर्मनिर्जरा की अपेक्षा आगे-आगे को अवस्था में कर्मनिर्जरा असंख्यातगुनी बढ़ती जाती है। सबसे अधिक निर्जरा सर्वज्ञ जिन भगवान् की होती है।
कषायों का लगभग नाश तो दसवें गुणस्थान में ही हो जाता है। ग्यारहवें गुणस्थान में मोह उपशान्त हो जाता है । बारहवे में वह क्षीण हो जाता है। तेरहवें गुणस्थान में वीतराग केवली के योग के निमित्त से दो समय की स्थिति का सिर्फ सातावेदनीय कमप्रकृति का बन्ध होता है। प्रथम समय में कर्मपरमाणु आत्मा के साथ सम्बन्ध करते हैं, दूसरे समय में भोग लिये जाते हैं और तीसरे समय में कर्म उनसे बिछड जाते हैं। चौदहवें गुणस्थान में मन-वचन-काया की सभी प्रवृत्तियाँ रुक जाती हैं, इसलिए वहाँ नगे कर्म का बन्ध नहीं होता, केवल पूर्वसंचित कर्मों की निर्जरा होती है। अबन्ध दशा में आत्मा शेष कर्मों को सर्वथा क्षय करके मुक्त हो हो जाता है। मुक्त-आत्मा पुनः कर्ममल लिप्त नहीं होता
जिस महान् आत्मा ने कर्मों का आत्यन्तिक नाश कर दिया है, वह पुनः कर्ममल से लिप्त नहीं होता; वह सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो जाता है। जब आत्मा एक बार पूर्ण रूप से कर्मों से विमुक्त हो जाता है, फिर वह कभी कर्मबद्ध नहीं होता, क्योंकि उस अवस्था में कर्मबन्ध के कारणों का सर्वथा
१ सम्यग्दृष्टि श्रावक - विरतानन्तवियोजक-दर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्षपक
क्षीणमोह-जिनाः क्रमशोऽसंख्येयगुणनिर्जराः। -तत्त्वार्थ • अ० ६।४७