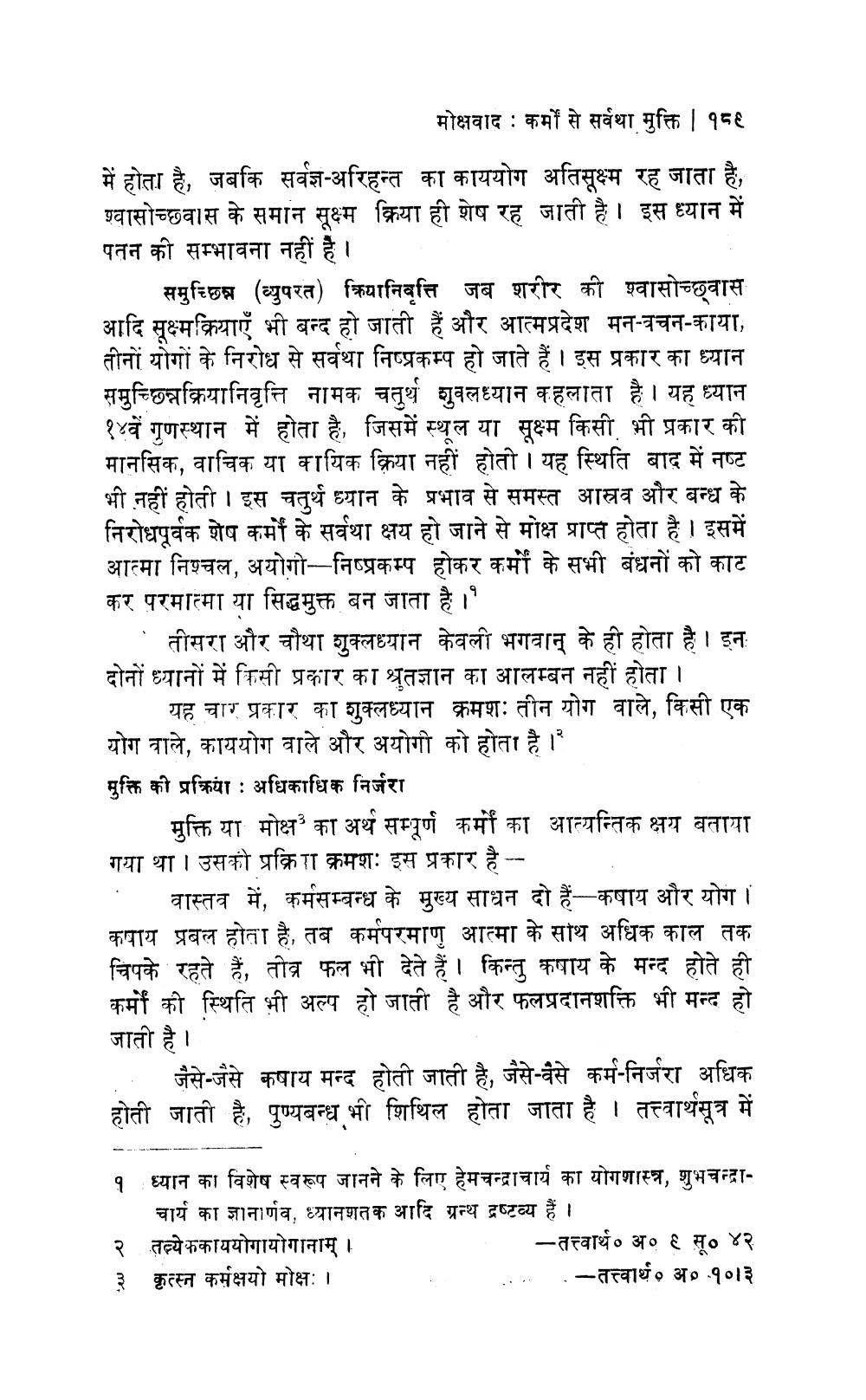________________
मोक्षवाद : कर्मों से सर्वथा मुक्ति | १८९
में होता है, जबकि सर्वज्ञ - अरिहन्त का काययोग अतिसूक्ष्म रह जाता है, श्वासोच्छवास के समान सूक्ष्म क्रिया ही शेष रह जाती है । इस ध्यान में पतन की सम्भावना नहीं है ।
समुच्छिन्न ( व्युपरत ) क्रियानिवृत्ति जब शरीर की श्वासोच्छ्वास आदि सूक्ष्म क्रियाएँ भी बन्द हो जाती हैं और आत्मप्रदेश मन-वचन-काया, तीनों योगों के निरोध से सर्वथा निष्प्रकम्प हो जाते हैं। इस प्रकार का ध्यान समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति नामक चतुर्थ शुवलध्यान कहलाता है । यह ध्यान १४ वे गुणस्थान में होता है, जिसमें स्थूल या सूक्ष्म किसी भी प्रकार की मानसिक, वाचिक या कायिक क्रिया नहीं होती । यह स्थिति बाद में नष्ट भी नहीं होती । इस चतुर्थ ध्यान के प्रभाव से समस्त आस्रव और बन्ध के निरोधपूर्वक शेष कर्मों के सर्वथा क्षय हो जाने से मोक्ष प्राप्त होता है । इसमें आत्मा निश्चल, अयोगो - निष्प्रकम्प होकर कर्मों के सभी बंधनों को काट कर परमात्मा या सिद्धमुक्त बन जाता है ।'
तीसरा और चौथा शुक्लध्यान केवली भगवान् के ही होता है । इन दोनों ध्यानों में किसी प्रकार का श्रुतज्ञान का आलम्बन नहीं होता ।
यह चार प्रकार का शुक्लध्यान क्रमशः तीन योग वाले, किसी एक योग वाले, काययोग वाले और अयोगी को होता है ।"
मुक्ति की प्रक्रिया : अधिकाधिक निर्जरा
मुक्तिया मोक्ष का अर्थ सम्पूर्ण कर्मों का आत्यन्तिक क्षय बताया गया था । उसकी प्रक्रिश क्रमशः इस प्रकार है
वास्तव में, कर्मसम्बन्ध के मुख्य साधन दो हैं— कषाय और योग । कषाय प्रबल होता है, तब कर्मपरमाणु आत्मा के साथ अधिक काल तक चिपके रहते हैं, तीव्र फल भी देते हैं । किन्तु कषाय के मन्द होते ही कर्मों की स्थिति भी अल्प हो जाती है और फलप्रदानशक्ति भी मन्द हो जाती है ।
जैसे - जैसे कषाय मन्द होती जाती है, जैसे-वैसे कर्म- निर्जरा अधिक होती जाती है, पुण्यबन्ध भी शिथिल होता जाता है । तत्त्वार्थसूत्र में
ध्यान का विशेष स्वरूप जानने के लिए हेमचन्द्राचार्य का योगशास्त्र, शुभचन्द्राचार्य का ज्ञानार्णव, ध्यानशतक आदि ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं ।
२ तत्येक काययोगायोगानाम् ।
० अ० १ सू० ४२
- तत्त्वार्थ ० . - तत्त्वार्थ० अ० १०।३
३ कृत्स्न कर्मक्षयो मोक्षः ।
१