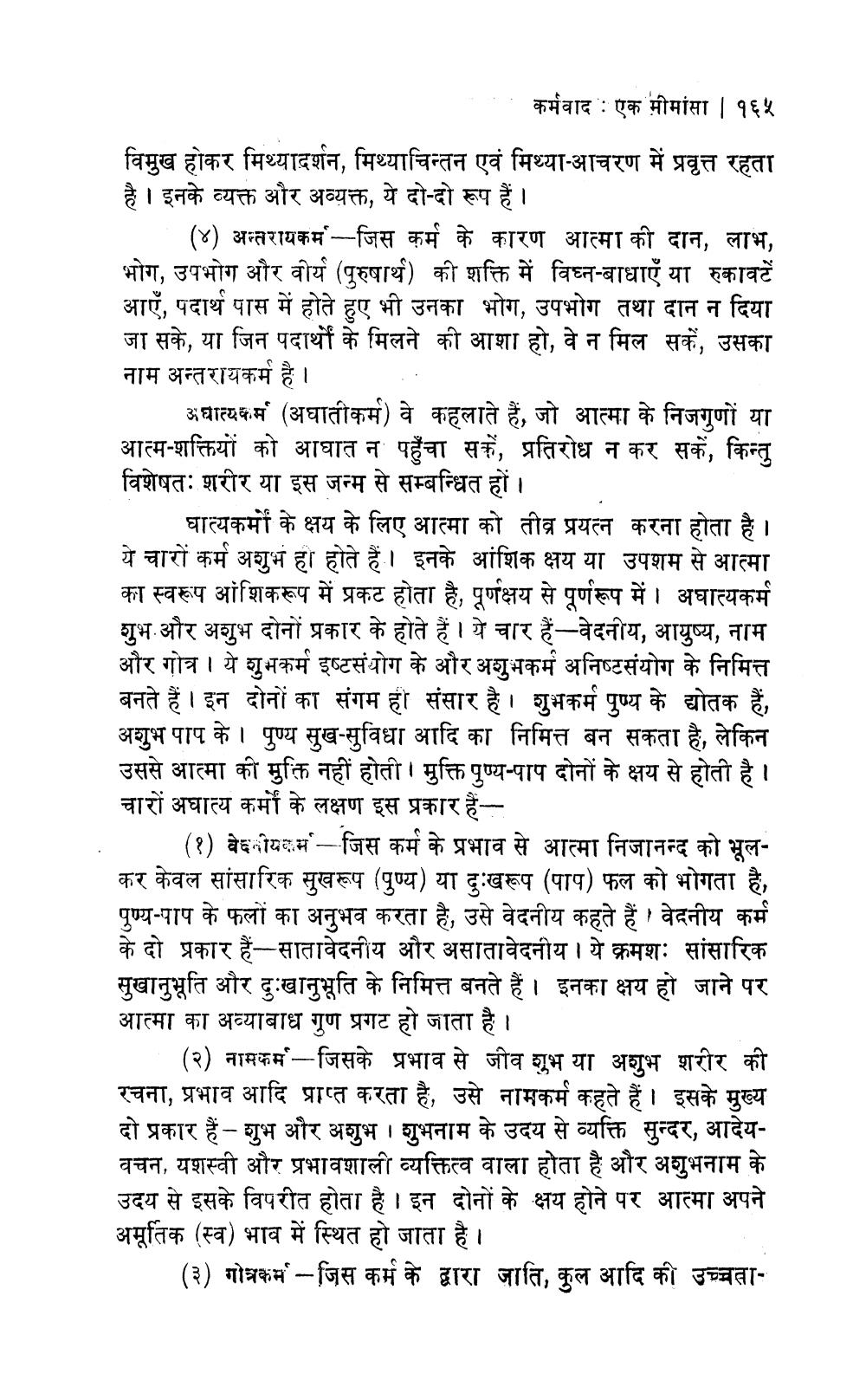________________
कर्मवाद : एक मीमांसा | १६५
विमुख होकर मिथ्यादर्शन, मिथ्याचिन्तन एवं मिथ्या - आचरण में प्रवृत्त रहता है | इनके व्यक्त और अव्यक्त, ये दो-दो रूप हैं ।
(४) अन्तरायकर्म - जिस कर्म के कारण आत्मा की दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य ( पुरुषार्थ) की शक्ति में विघ्न-बाधाएँ या रुकावटें आएँ, पदार्थ पास में होते हुए भी उनका भोग, उपभोग तथा दान न दिया जा सके, या जिन पदार्थों के मिलने की आशा हो, वे न मिल सकें, उसका नाम अन्तरायकर्म है ।
अधात्यकर्म (अघातीकर्म) वे कहलाते हैं, जो आत्मा के निजगुणों या आत्म-शक्तियों को आघात न पहुँचा सकें, प्रतिरोध न कर सकें, किन्तु विशेषतः शरीर या इस जन्म से सम्बन्धित हों ।
घात्यकर्मों के क्षय के लिए आत्मा को तीव्र प्रयत्न करना होता है । ये चारों कर्म अशुभ हो होते हैं । इनके आंशिक क्षय या उपशम से आत्मा का स्वरूप आंशिकरूप में प्रकट होता है, पूर्णक्षय से पूर्णरूप में । अघात्यकर्म शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। ये चार हैं - वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र । ये शुभकर्म इष्टसंयोग के और अशुभकर्म अनिष्टसंयोग के निमित्त बनते हैं । इन दोनों का संगम ही संसार है । शुभकर्म पुण्य के द्योतक हैं, अशुभ पाप के । पुण्य सुख-सुविधा आदि का निमित्त बन सकता है, लेकिन उससे आत्मा की मुक्ति नहीं होती । मुक्ति पुण्य-पाप दोनों के क्षय से होती है । चारों अघात्य कर्मों के लक्षण इस प्रकार हैं
(१) वेद - जिस कर्म के प्रभाव से आत्मा निजानन्द को भूलकर केवल सांसारिक सुखरूप (पुण्य) या दुःखरूप (पाप) फल को भोगता है, पुण्य-पाप के फलों का अनुभव करता है, उसे वेदनीय कहते हैं । वेदनीय कर्म के दो प्रकार हैं- सातावेदनीय और असातावेदनीय । ये क्रमशः सांसारिक सुखानुभूति और दुःखानुभूति के निमित्त बनते हैं । इनका क्षय हो जाने पर आत्मा का अयाबाध गुण प्रगट हो जाता है ।
(२) नामकर्म - जिसके प्रभाव से जीव शुभ या अशुभ शरीर की रचना, प्रभाव आदि प्राप्त करता है, उसे नामकर्म कहते हैं । इसके मुख्य दो प्रकार हैं- शुभ और अशुभ। शुभनाम के उदय से व्यक्ति सुन्दर, आदेय - वचन, यशस्वी और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है और अशुभनाम के उदय से इसके विपरीत होता है । इन दोनों के क्षय होने पर आत्मा अपने अमूर्ति (स्व) भाव में स्थित हो जाता है ।
(३) गोत्रकर्म - जिस कर्म के द्वारा जाति, कुल आदि की उच्चता