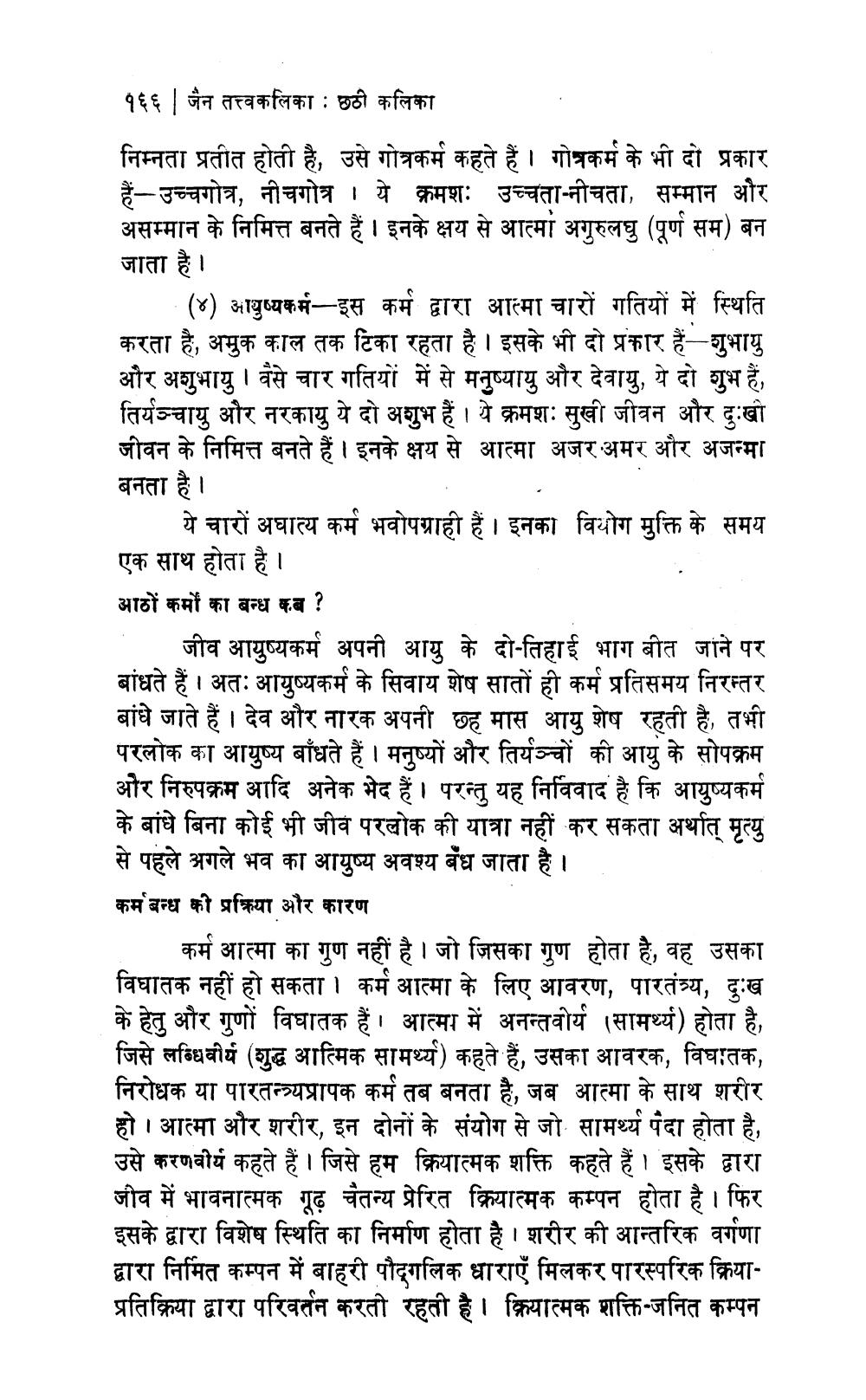________________
१६६ / जैन तत्त्वकलिका : छठी कलिका निम्नता प्रतीत होती है, उसे गोत्रकर्म कहते हैं । गोत्रकर्म के भी दो प्रकार हैं-उच्चगोत्र, नीचगोत्र । ये क्रमशः उच्चता-नीचता, सम्मान और असम्मान के निमित्त बनते हैं । इनके क्षय से आत्मां अगुरुलघु (पूर्ण सम) बन जाता है।
(४) आयुष्यकर्म-इस कर्म द्वारा आत्मा चारों गतियों में स्थिति करता है, अमुक काल तक टिका रहता है । इसके भी दो प्रकार हैं-शुभायु और अशुभायु । वैसे चार गतियों में से मनुष्यायु और देवायु, ये दो शुभ हैं, तिर्यञ्चायु और नरकायु ये दो अशुभ हैं । ये क्रमशः सुखी जीवन और दुःखी जीवन के निमित्त बनते हैं। इनके क्षय से आत्मा अजर अमर और अजन्मा बनता है।
ये चारों अघात्य कर्म भवोपग्राही हैं। इनका वियोग मुक्ति के समय एक साथ होता है। आठों कर्मों का बन्ध कब ?
जीव आयुष्यकर्म अपनी आयु के दो-तिहाई भाग बीत जाने पर बांधते हैं । अतः आयुष्यकर्म के सिवाय शेष सातों ही कर्म प्रतिसमय निरन्तर बांधे जाते हैं । देव और नारक अपनी छह मास आयु शेष रहती है, तभी परलोक का आयुष्य बाँधते हैं । मनुष्यों और तिर्यञ्चों की आयु के सोपक्रम
और निरुपक्रम आदि अनेक भेद हैं। परन्तु यह निर्विवाद है कि आयुष्यकर्म के बांधे बिना कोई भी जीव परलोक की यात्रा नहीं कर सकता अर्थात् मृत्यु से पहले अगले भव का आयुष्य अवश्य बंध जाता है। कर्मबन्ध की प्रक्रिया और कारण
कर्म आत्मा का गुण नहीं है । जो जिसका गुण होता है, वह उसका विघातक नहीं हो सकता। कर्म आत्मा के लिए आवरण, पारतंत्र्य, दुःख के हेतु और गुणों विघातक हैं। आत्मा में अनन्तवीर्य (सामर्थ्य) होता है, जिसे लब्धिवीर्य (शुद्ध आत्मिक सामर्थ्य) कहते हैं, उसका आवरक, विघातक, निरोधक या पारतन्त्र्यप्रापक कर्म तब बनता है, जब आत्मा के साथ शरीर हो । आत्मा और शरीर, इन दोनों के संयोग से जो सामर्थ्य पैदा होता है, उसे करणवीर्य कहते हैं । जिसे हम क्रियात्मक शक्ति कहते हैं। इसके द्वारा जीव में भावनात्मक गूढ़ चैतन्य प्रेरित क्रियात्मक कम्पन होता है। फिर इसके द्वारा विशेष स्थिति का निर्माण होता है। शरीर की आन्तरिक वर्गणा द्वारा निर्मित कम्पन में बाहरी पौद्गलिक धाराएँ मिलकर पारस्परिक क्रियाप्रतिक्रिया द्वारा परिवर्तन करती रहती है। क्रियात्मक शक्ति-जनित कम्पन