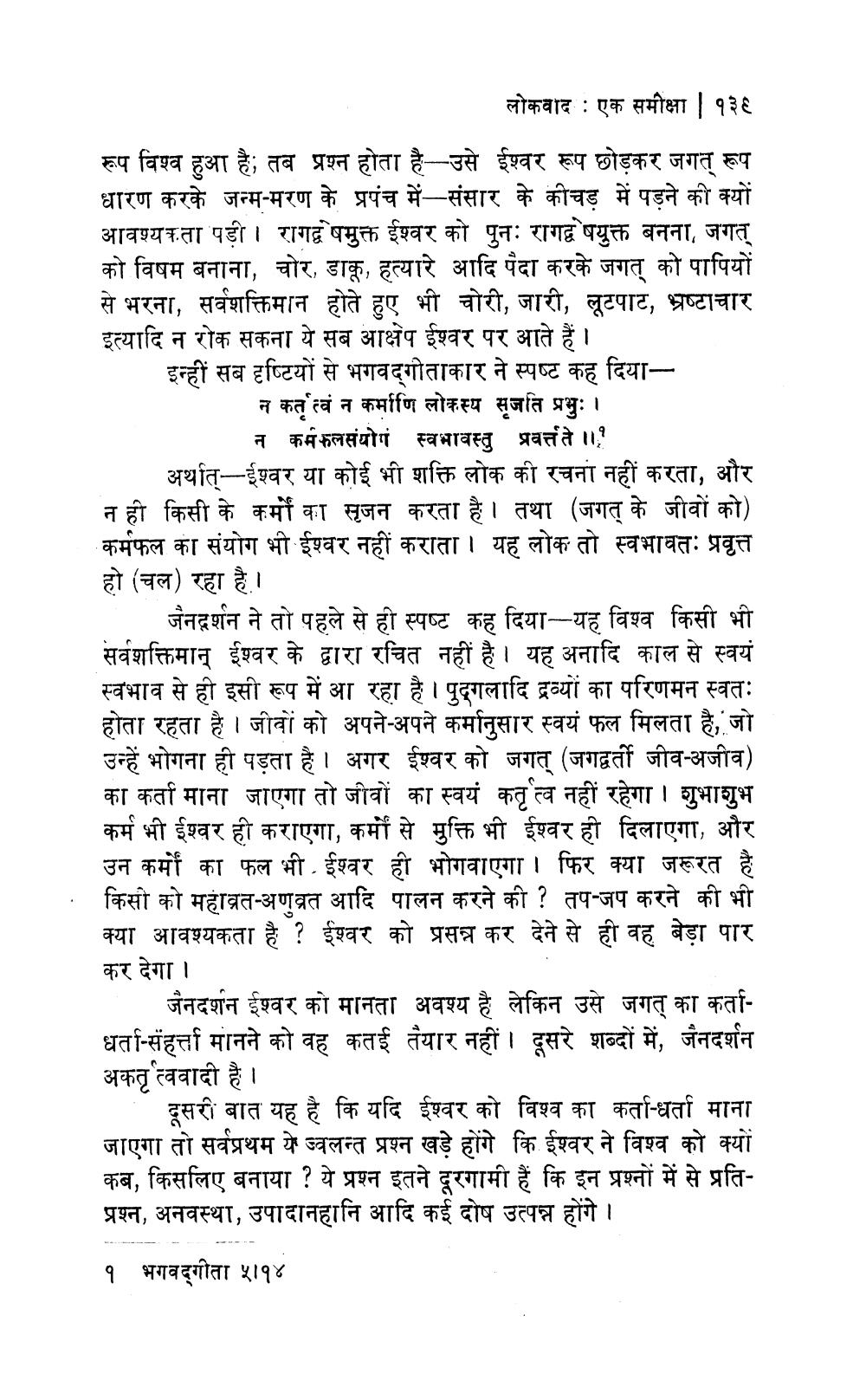________________
लोकवाद : एक समीक्षा | १३६ रूप विश्व हुआ है, तब प्रश्न होता है उसे ईश्वर रूप छोड़कर जगत् रूप धारण करके जन्म-मरण के प्रपंच में संसार के कीचड़ में पड़ने की क्यों आवश्यकता पड़ी। रागद्वषमुक्त ईश्वर को पुनः रागद्वेषयुक्त बनना, जगत् को विषम बनाना, चोर, डाकू, हत्यारे आदि पैदा करके जगत् को पापियों से भरना, सर्वशक्तिमान होते हुए भी चोरी, जारी, लूटपाट, भ्रष्टाचार इत्यादि न रोक सकना ये सब आक्षेप ईश्वर पर आते हैं। इन्हीं सब दृष्टियों से भगवद्गीताकार ने स्पष्ट कह दिया
न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।
न कर्मफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ अर्थात्-ईश्वर या कोई भी शक्ति लोक की रचना नहीं करता, और न ही किसी के कर्मों का सृजन करता है। तथा (जगत के जीवों को) कर्मफल का संयोग भी ईश्वर नहीं कराता। यह लोक तो स्वभावतः प्रवृत्त हो (चल) रहा है।
जैनदर्शन ने तो पहले से ही स्पष्ट कह दिया-यह विश्व किसी भी सर्वशक्तिमान् ईश्वर के द्वारा रचित नहीं है। यह अनादि काल से स्वयं स्वभाव से ही इसी रूप में आ रहा है। पुद्गलादि द्रव्यों का परिणमन स्वतः होता रहता है । जीवों को अपने-अपने कर्मानुसार स्वयं फल मिलता है, जो उन्हें भोगना ही पड़ता है। अगर ईश्वर को जगत् (जगद्वर्ती जीव-अजीव) का कर्ता माना जाएगा तो जीवों का स्वयं कतृत्व नहीं रहेगा। शुभाशुभ कर्म भी ईश्वर ही कराएगा, कर्मों से मुक्ति भी ईश्वर ही दिलाएगा, और उन कर्मों का फल भी . ईश्वर ही भोगवाएगा। फिर क्या जरूरत है किसी को महाव्रत-अणवत आदि पालन करने की ? तप-जप करने की भी क्या आवश्यकता है ? ईश्वर को प्रसन्न कर देने से ही वह बेड़ा पार कर देगा।
जैनदर्शन ईश्वर को मानता अवश्य है लेकिन उसे जगत् का कर्ताधर्ता-संह" मानने को वह कतई तैयार नहीं। दूसरे शब्दों में, जैनदर्शन अकतृत्ववादी है।
दूसरी बात यह है कि यदि ईश्वर को विश्व का कर्ता-धर्ता माना जाएगा तो सर्वप्रथम ये ज्वलन्त प्रश्न खड़े होंगे कि ईश्वर ने विश्व को क्यों कब, किसलिए बनाया ? ये प्रश्न इतने दूरगामी हैं कि इन प्रश्नों में से प्रतिप्रश्न, अनवस्था, उपादानहानि आदि कई दोष उत्पन्न होंगे।
१ भगवद्गीता ५।१४