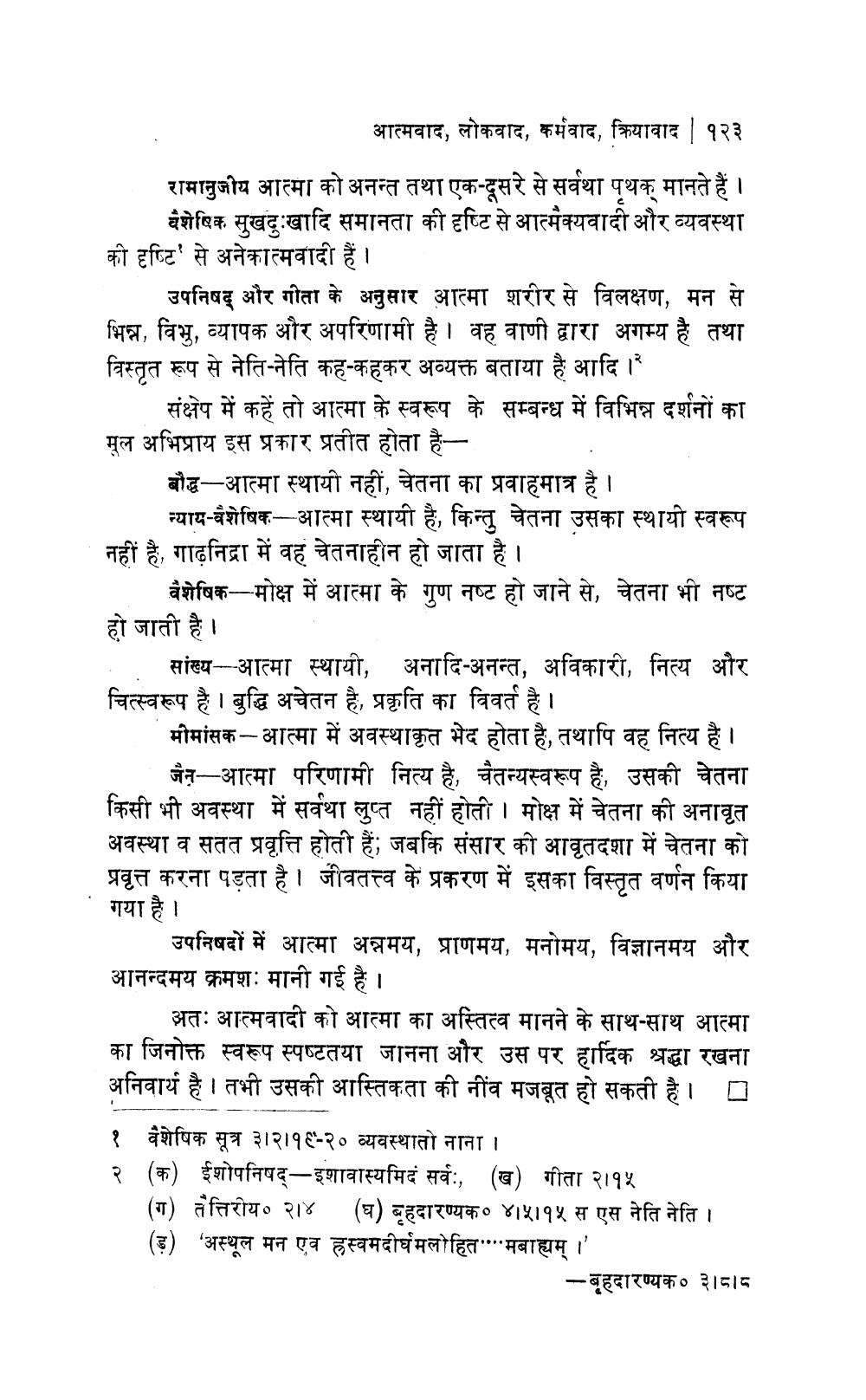________________
आत्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद, क्रियावाद | १२३
रामानुजीय आत्मा को अनन्त तथा एक-दूसरे से सर्वथा पृथक् मानते हैं । वैशेषिक सुखदुःखादि समानता की दृष्टि से आत्मैक्यवादी और व्यवस्था की दृष्टि' से अनेकात्मवादी हैं ।
उपनिषद् और गीता के अनुसार आत्मा शरीर से विलक्षण, मन से भिन्न, विभु, व्यापक और अपरिणामी है । वह वाणी द्वारा अगम्य है तथा विस्तृत रूप से नेति नेति कह कहकर अव्यक्त बताया है आदि ।
संक्षेप में कहें तो आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में विभिन्न दर्शनों का मूल अभिप्राय इस प्रकार प्रतीत होता है
बौद्ध - आत्मा स्थायी नहीं, चेतना का प्रवाहमात्र है । न्याय-वैशेषिक – आत्मा स्थायी है, किन्तु चेतना उसका स्थायी स्वरूप नहीं है, गाढ़निद्रा में वह चेतनाहीन हो जाता है ।
वैशेषिक – मोक्ष में आत्मा के गुण नष्ट हो जाने से, चेतना भी नष्ट हो जाती है ।
सांख्य
- आत्मा स्थायी,
अनादि-अनन्त, अविकारी, नित्य और चित्स्वरूप है | बुद्धि अचेतन है, प्रकृति का विवर्त है ।
मीमांसक - आत्मा में अवस्थाकृत भेद होता है, तथापि वह नित्य है । जैन - आत्मा परिणामी नित्य है, चैतन्यस्वरूप है, उसकी चेतना किसी भी अवस्था में सर्वथा लुप्त नहीं होती । मोक्ष में चेतना की अनावृत अवस्था व सतत प्रवृत्ति होती हैं, जबकि संसार की आवृतदशा में चेतना को प्रवृत्त करना पड़ता है । जीवतत्त्व के प्रकरण में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है ।
उपनिषदों में आत्मा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय क्रमशः मानी गई है ।
अतः आत्मवादी को आत्मा का अस्तित्व मानने के साथ-साथ आत्मा का जिनोक्त स्वरूप स्पष्टतया जानना और उस पर हार्दिक श्रद्धा रखना अनिवार्य है । तभी उसकी आस्तिकता की नींव मजबूत हो सकती है । O
१ वैशेषिक सूत्र ३।२।१६ - २० व्यवस्थातो नाना ।
२ (क) ईशोपनिषद् - इशावास्यमिदं सर्वः, (ख) गीता २।१५
(ग) तैत्तिरीय० २।४ (घ) बृहदारण्यक० ४।५।१५ स एस नेति नेति ।
(ड़) 'अस्थूल मन एव ह्रस्वमदीर्घ मलोहित 'मबाह्यम् ।'
- बृहदारण्यक० ३।८८