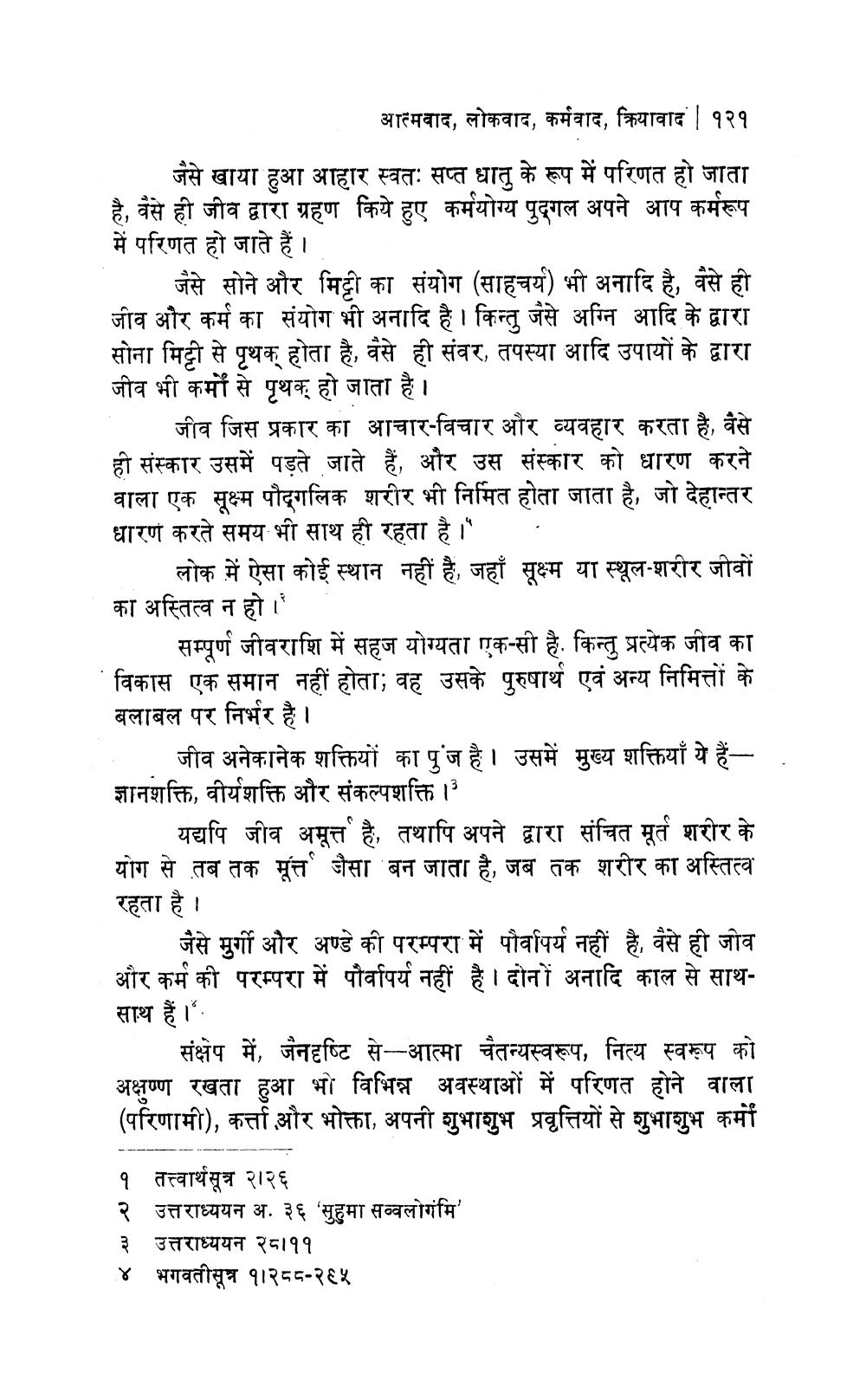________________
आत्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद, क्रियावाद | १२१
जैसे खाया हुआ आहार स्वतः सप्त धातु के रूप में परिणत हो जाता है, वैसे ही जीव द्वारा ग्रहण किये हुए कर्मयोग्य पुद्गल अपने आप कर्मरूप में परिणत हो जाते हैं ।
जैसे सोने और मिट्टी का संयोग ( साहचर्य) भी अनादि है, वैसे ही जीव और कर्म का संयोग भी अनादि है । किन्तु जैसे अग्नि आदि के द्वारा सोना मिट्टी से पृथक् होता है, वैसे ही संवर, तपस्या आदि उपायों के द्वारा जीव भी कर्मों से पृथक हो जाता है ।
जीव जिस प्रकार का आचार-विचार और व्यवहार करता है, वैसे ही संस्कार उसमें पड़ते जाते हैं, और उस संस्कार को धारण करने वाला एक सूक्ष्म पौद्गलिक शरीर भी निर्मित होता जाता है, जो देहान्तर धारण करते समय भी साथ ही रहता है ।"
लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ सूक्ष्म या स्थूल शरीर जीवों IT अस्तित्व न हो ।'
सम्पूर्ण जीवराशि में सहज योग्यता एक-सी है. किन्तु प्रत्येक जीव का विकास एक समान नहीं होता; वह उसके पुरुषार्थ एवं अन्य निमित्तों के बलाबल पर निर्भर है ।
जीव अनेकानेक शक्तियों का पुंज है । उसमें मुख्य शक्तियाँ ये हैंज्ञानशक्ति, वीर्यशक्ति और संकल्पशक्ति ।
यद्यपि जीव अमूर्त है, तथापि अपने द्वारा संचित मूर्त शरीर के योग से तब तक मूर्त' जैसा बन जाता है, जब तक शरीर का अस्तित्व रहता है ।
जैसे मुर्गी और अण्डे की परम्परा में पौर्वापर्य नहीं है, वैसे ही जीव और कर्म की परम्परा में पौर्वापर्य नहीं है । दोनों अनादि काल से साथसाथ हैं ।
संक्षेप में, जैनदृष्टि से - आत्मा चैतन्यस्वरूप, नित्य स्वरूप को अक्षुण्ण रखता हुआ भो विभिन्न अवस्थाओं में परिणत होने वाला ( परिणामी ), कर्त्ता और भोक्ता, अपनी शुभाशुभ प्रवृत्तियों से शुभाशुभ कर्मों
१ तत्त्वार्थ सूत्र २।२६
२ उत्तराध्ययन अ. ३६ 'सुहुमा सव्वलोगंमि'
३ उत्तराध्ययन २८।११
४ भगवतीसूत्र १।२८८-२६५