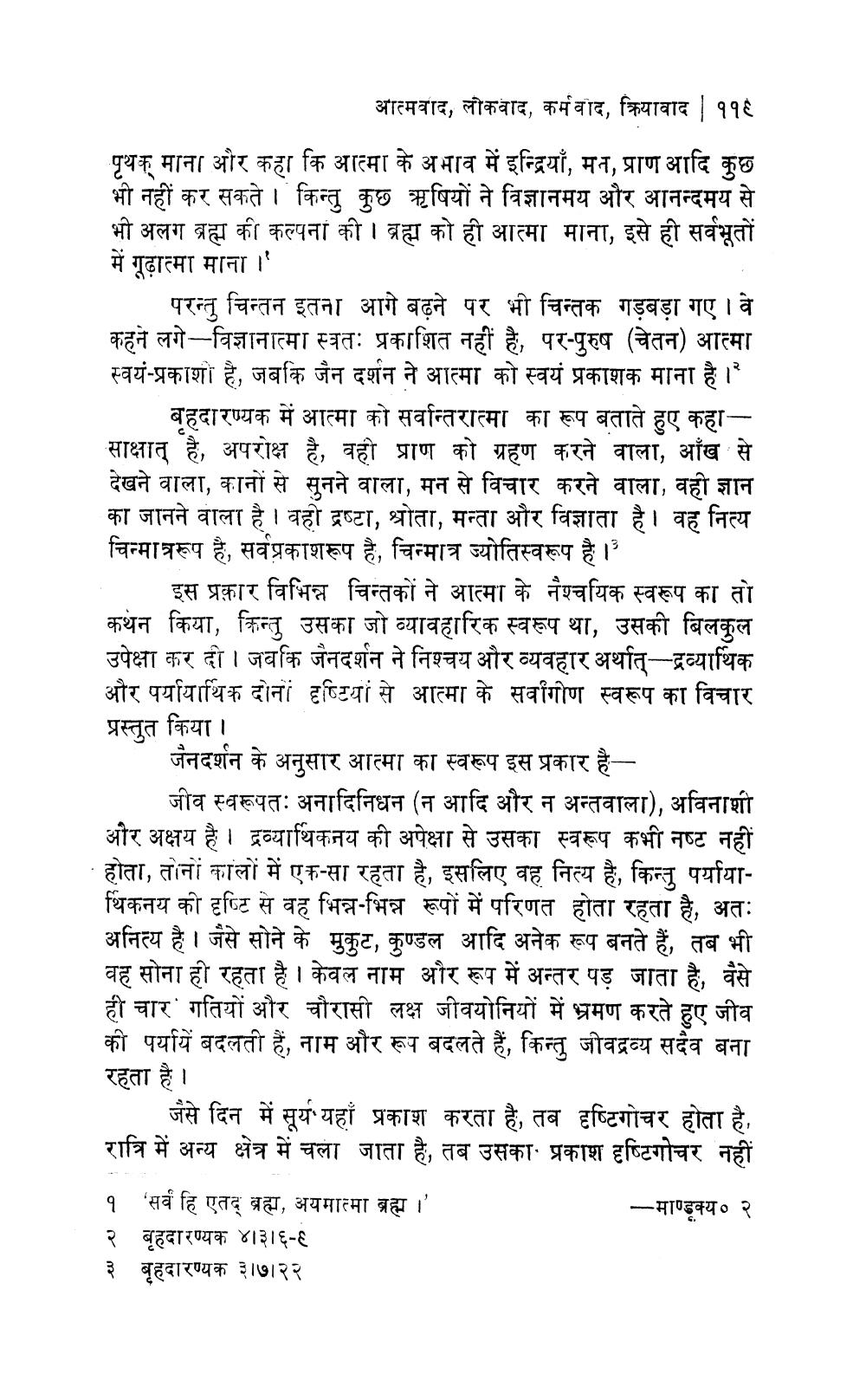________________
आत्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद, क्रियावाद | ११६
पृथक् माना और कहा कि आत्मा के अभाव में इन्द्रियाँ, मन, प्राण आदि कुछ भी नहीं कर सकते । किन्तु कुछ ऋषियों ने विज्ञानमय और आनन्दमय से भी अलग ब्रह्म की कल्पना की। ब्रह्म को ही आत्मा माना, इसे ही सर्वभूतों में गूढात्मा माना।
परन्तु चिन्तन इतना आगे बढ़ने पर भी चिन्तक गड़बड़ा गए । वे कहने लगे-विज्ञानात्मा स्वतः प्रकाशित नहीं है, पर-पुरुष (चेतन) आत्मा स्वयं-प्रकाशो है, जबकि जैन दर्शन ने आत्मा को स्वयं प्रकाशक माना है।'
बृहदारण्यक में आत्मा को सर्वान्तरात्मा का रूप बताते हुए कहासाक्षात् है, अपरोक्ष है, वही प्राण को ग्रहण करने वाला, आँख से देखने वाला, कानों से सुनने वाला, मन से विचार करने वाला, वही ज्ञान का जानने वाला है । वही द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और विज्ञाता है। वह नित्य चिन्मात्ररूप है, सर्वप्रकाशरूप है, चिन्मात्र ज्योतिस्वरूप है।
इस प्रकार विभिन्न चिन्तकों ने आत्मा के नैश्चयिक स्वरूप का तो कथन किया, किन्तु उसका जो व्यावहारिक स्वरूप था, उसकी बिलकुल उपेक्षा कर दी । जबकि जैनदर्शन ने निश्चय और व्यवहार अर्थात्-द्रव्यार्थिक और पर्यायाथिक दोनों दृष्टियों से आत्मा के सर्वांगीण स्वरूप का विचार प्रस्तुत किया।
जैनदर्शन के अनुसार आत्मा का स्वरूप इस प्रकार है
जीव स्वरूपतः अनादिनिधन (न आदि और न अन्तवाला), अविनाशी और अक्षय है। द्रव्याथिकनय की अपेक्षा से उसका स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता, तोनों कालों में एक-सा रहता है, इसलिए वह नित्य है, किन्तु पर्यायाथिकनय की दृष्टि से वह भिन्न-भिन्न रूपों में परिणत होता रहता है, अतः अनित्य है । जैसे सोने के मुकुट, कुण्डल आदि अनेक रूप बनते हैं, तब भी वह सोना ही रहता है । केवल नाम और रूप में अन्तर पड़ जाता है, वैसे ही चार गतियों और चौरासी लक्ष जीवयोनियों में भ्रमण करते हुए जीव की पर्यायें बदलती हैं, नाम और रूप बदलते हैं, किन्तु जीवद्रव्य सदैव बना रहता है।
जैसे दिन में सूर्य यहाँ प्रकाश करता है, तब दृष्टिगोचर होता है, रात्रि में अन्य क्षेत्र में चला जाता है, तब उसका प्रकाश दृष्टिगोचर नहीं १ 'सर्वं हि एतद् ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म ।'
-माण्डक्य०२ २ बृहदारण्यक ४।३।६-६ ३ बृहदारण्यक ३।७।२२