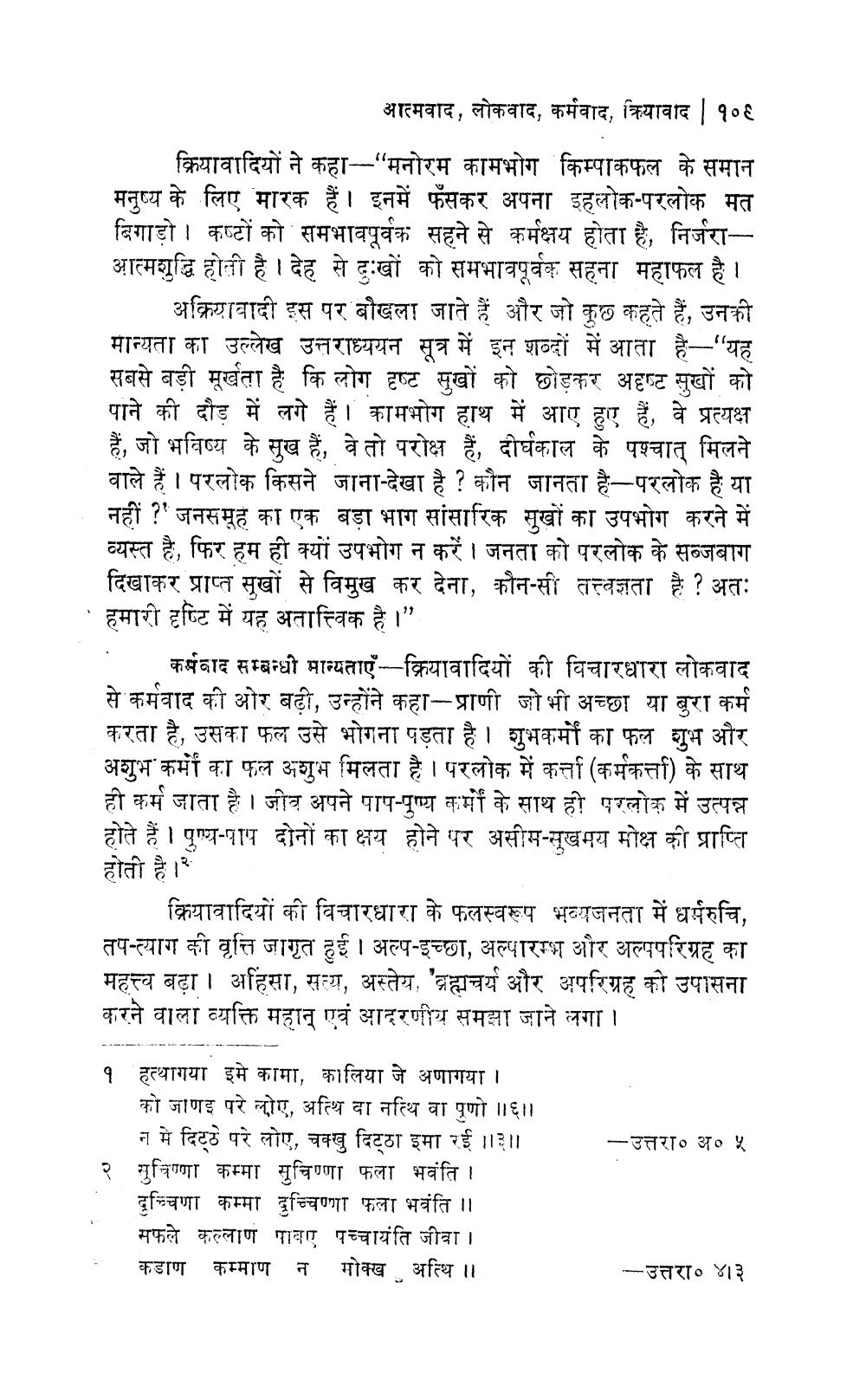________________
आत्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद, क्रियावाद | १०६
क्रियावादियों ने कहा - " मनोरम कामभोग किम्पाकफल के समान मनुष्य के लिए मारक हैं । इनमें फँसकर अपना इहलोक-परलोक मत बिगाड़ो । कष्टों को समभावपूर्वक सहने से कर्मक्षय होता है, निर्जराआत्मशुद्धि होती है । देह से दुःखों को समभावपूर्वक सहना महाफल है ।
अक्रियावादी इस पर बोखला जाते हैं और जो कुछ कहते हैं, उनकी मान्यता का उल्लेख उत्तराध्ययन सूत्र में इन शब्दों में आता है - "यह सबसे बड़ी मूर्खता है कि लोग दृष्ट सुखों को छोड़कर अदृष्ट सुखों को पाने की दौड़ में लगे हैं । कामभोग हाथ में आए हुए हैं, वे प्रत्यक्ष हैं, जो भविष्य के सुख हैं, वे तो परोक्ष हैं, दीर्घकाल के पश्चात् मिलने वाले हैं । परलोक किसने जाना देखा है ? कौन जानता है - परलोक है या नहीं ?' जनसमूह का एक बड़ा भाग सांसारिक सुखों का उपभोग करने में व्यस्त है, फिर हम ही क्यों उपभोग न करें। जनता को परलोक के सब्जबाग दिखाकर प्राप्त सुखों से विमुख कर देना, कौन-सी तत्त्वज्ञता है ? अतः हमारी दृष्टि में यह अतात्त्विक है । "
कर्मवाद सम्बन्धी मान्यताएँ - क्रियावादियों की विचारधारा लोकवाद से कर्मवाद की ओर बढ़ी, उन्होंने कहा - प्राणी जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसका फल उसे भोगना पड़ता है । शुभकर्मों का फल शुभ और अशुभ कर्मों का फल अशुभ मिलता है । परलोक में कर्त्ता (कर्मकर्ता ) के साथ ही कर्म जाता है । जीव अपने पाप-पुण्य कर्मों के साथ ही परलोक में उत्पन्न होते हैं । पुण्य-पाप दोनों का क्षय होने पर असीम सुखमय मोक्ष की प्राप्ति होती है।
क्रियावादियों की विचारधारा के फलस्वरूप भव्यजनता में धर्मरुचि, तप त्याग की वृत्ति जागृत हुई । अल्प- इच्छा, अल्पारम्भ और अल्पपरिग्रह का महत्त्व बढ़ा । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 'ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की उपासना करने वाला व्यक्ति महान् एवं आदरणीय समझा जाने लगा ।
१ हत्थागया इमे कामा, कालिया जे अणागया ।
को जाइ परे लोए, अस्थि वा नत्थि वा पुणो ॥ ६ ॥ | न मे दिट्ठे परे लोए, चक्खु दिट्ठा इमा रई ॥३॥
२ सुचिणा कम्मा सुचिण्णा फला भवंति । दुचिणा कम्मा दुच्चिण्णा फला भवंति ॥ मफले कल्ला पावए पच्चायंति जीवा । कडाण कम्माण न मोक्ख अस्थि ||
- उत्तरा० अ० ५
- उत्तरा० ४।३