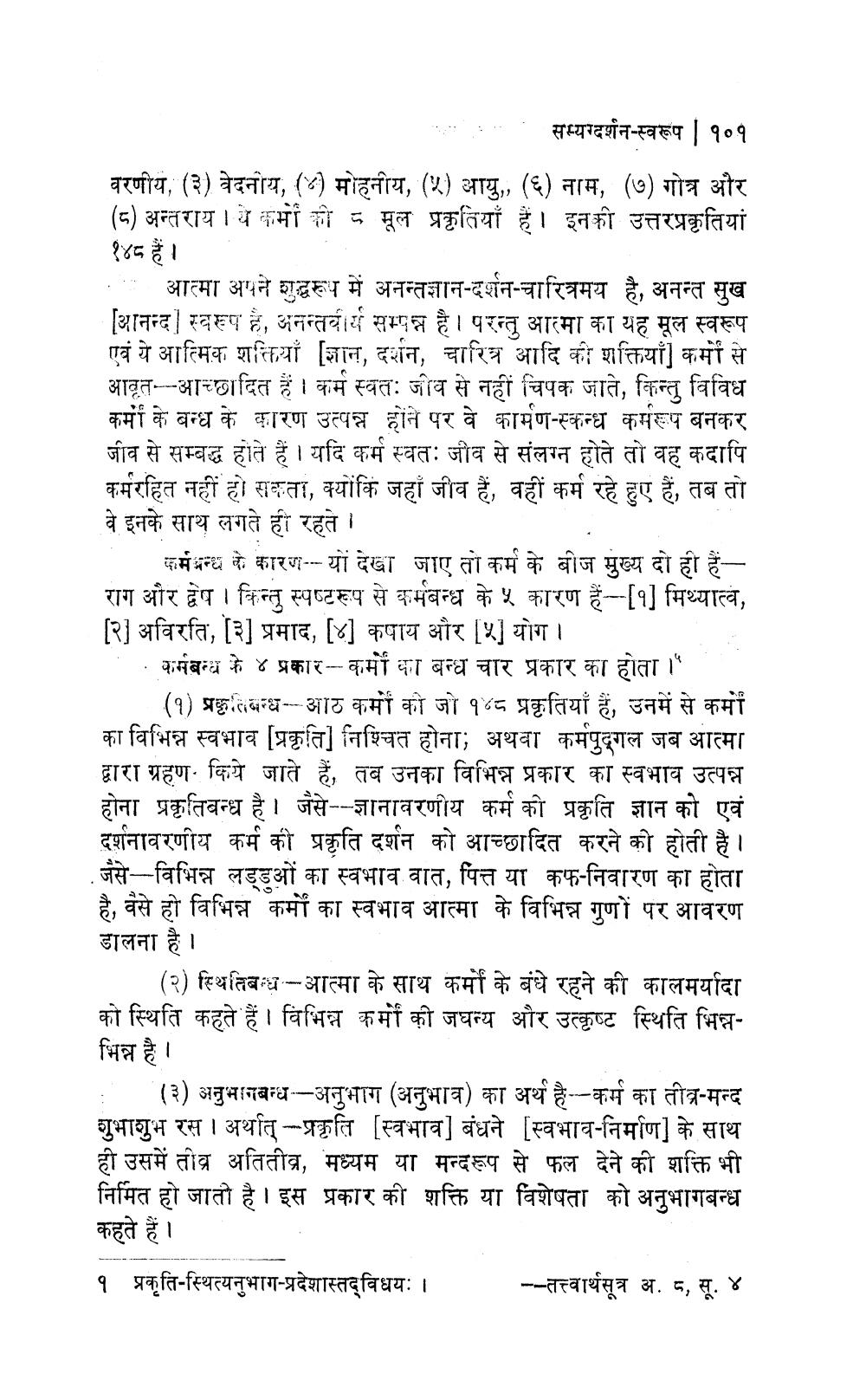________________
....... सम्यग्दर्शन-स्वरूप | १०१ वरणीय, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयु,, (६) नाम, (७) गोत्र और (८) अन्तराय । ये कर्मों की ८ मूल प्रकृतियाँ हैं। इनकी उत्तरप्रकृतियां
... आत्मा अपने शुद्धरूप में अनन्तज्ञान-दर्शन-चारित्रमय है, अनन्त सुख [आनन्द ] स्वरूप है, अनन्तवीर्य सम्पन्न है। परन्तु आत्मा का यह मूल स्वरूप एवं ये आत्मिक शक्तियाँ [ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि की शक्तियाँ] कर्मों से आवृत--आच्छादित हैं। कर्म स्वतः जीव से नहीं चिपक जाते, किन्तु विविध कमी के बन्ध के कारण उत्पन्न होने पर वे कामण-स्कन्ध कमरूप बनकर जीव से सम्बद्ध होते हैं । यदि कर्म स्वतः जीव से संलग्न होते तो वह कदापि कर्मरहित नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ जीव हैं, वहीं कर्म रहे हुए हैं, तब तो वे इनके साथ लगते ही रहते ।
कर्मबन्ध के कारण--- यों देखा जाए तो कर्म के बीज मुख्य दो ही हैंराग और द्वेष । किन्तु स्पष्ट रूप से कर्मबन्ध के ५ कारण हैं---[१] मिथ्यात्व, [२] अविरति, [३] प्रमाद, [४] कपाय और [५] योग। .. कर्मबन्ध के ४ प्रकार --- कर्मों का बन्ध चार प्रकार का होता।
(१) प्रकृतिबन्ध---आठ कर्मों को जो १४८ प्रकृतियाँ हैं, उनमें से कर्मों का विभिन्न स्वभाव [प्रकृति] निश्चित होना; अथवा कर्मपुद्गल जब आत्मा द्वारा ग्रहण किये जाते हैं, तब उनका विभिन्न प्रकार का स्वभाव उत्पन्न होना प्रकृतिबन्ध है। जैसे--ज्ञानावरणीय कर्म को प्रकृति ज्ञान को एवं दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृति दर्शन को आच्छादित करने को होती है। जैसे-विभिन्न लड्डओं का स्वभाव वात, पित्त या कफ-निवारण का होता है, वैसे हो विभिन्न कर्मों का स्वभाव आत्मा के विभिन्न गुणों पर आवरण डालना है।
(२) स्थितिबन्ध-आत्मा के साथ कर्मों के बंधे रहने की कालमर्यादा को स्थिति कहते हैं। विभिन्न कर्मों की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति भिन्नभिन्न है।
(३) अनुभागबन्ध-अनुभाग (अनुभाव) का अर्थ है---कर्म का तीव्र-मन्द शुभाशुभ रस । अर्थात् ---प्रकृति [स्वभाव] बंधने [स्वभाव-निर्माण] के साथ ही उसमें तीव्र अतितीव्र, मध्यम या मन्दरूप से फल देने की शक्ति भी निर्मित हो जाती है । इस प्रकार की शक्ति या विशेषता को अनुभागबन्ध कहते हैं। १ प्रकृति-स्थित्यनुभाग-प्रदेशास्तद्विधयः । --तत्त्वार्थसूत्र अ. ८, सू. ४