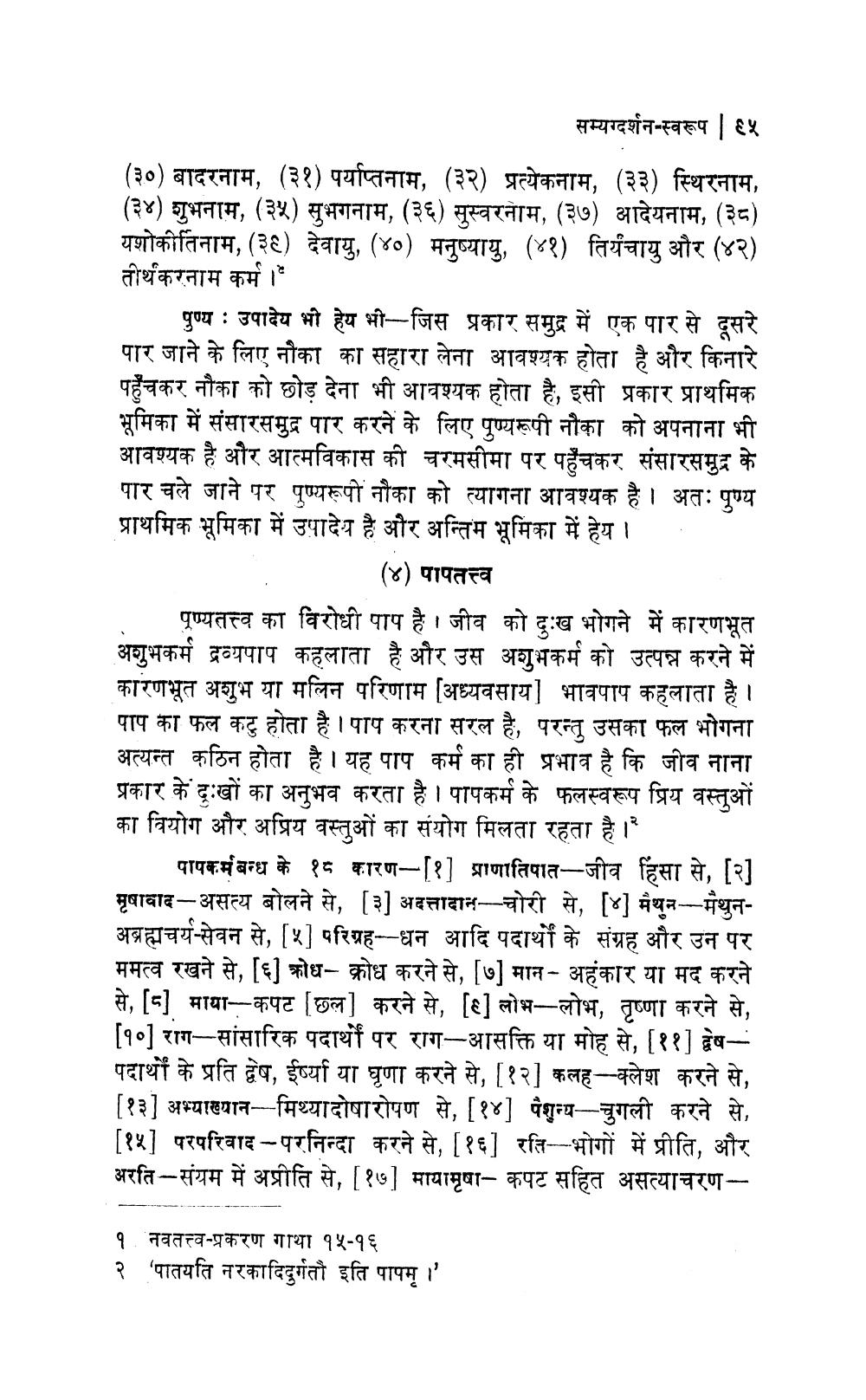________________
सम्यग्दर्शन- स्वरूप | ६५
(३०) बादरनाम, (३१) पर्याप्तनाम, (३२) प्रत्येकनाम, (३३) स्थिरनाम, (३४) शुभनाम, (३५) सुभगनाम, (३६) सुस्वरनाम, (३७) आदेयनाम, (३८) यशोकीर्तिनाम, (३९) देवायु, (४०) मनुष्यायु, (४१) तिर्यंचायु और (४२) तीर्थंकरनाम कर्म ।
पुण्य : उपादेय भी हेय भी - जिस प्रकार समुद्र में एक पार से दूसरे पार जाने के लिए नौका का सहारा लेना आवश्यक होता है और किनारे पहुँचकर नौका को छोड़ देना भी आवश्यक होता है, इसी प्रकार प्राथमिक भूमिका में संसारसमुद्र पार करने के लिए पुण्यरूपी नौका को अपनाना भी आवश्यक है और आत्मविकास की चरमसीमा पर पहुँचकर संसारसमुद्र के पार चले जाने पर पुण्यरूपी नौका को त्यागना आवश्यक है । अतः पुण्य प्राथमिक भूमिका में उपादेय है और अन्तिम भूमिका में हेय ।
(४) पापतत्त्व
पुण्यतत्त्व का विरोधी पाप है । जीव को दुःख भोगने में कारणभूत अशुभकर्म द्रव्यपाप कहलाता है और उस अशुभकर्म को उत्पन्न करने में कारणभूत अशुभ या मलिन परिणाम [ अध्यवसाय ] भावपाप कहलाता है । पाप का फल कटु होता है । पाप करना सरल है, परन्तु उसका फल भोगना अत्यन्त कठिन होता है । यह पाप कर्म का ही प्रभाव है कि जीव नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव करता है । पापकर्म के फलस्वरूप प्रिय वस्तुओं ar faयोग और अप्रिय वस्तुओं का संयोग मिलता रहता है । "
[४] मैथुन - मैथुन -
पापकर्मबन्ध के १८ कारण - [१] प्राणातिपात – जीव हिंसा से, [२] मृषावाद - असत्य बोलने से, [३] अदत्तादान - चोरी से, अब्रह्मचर्य सेवन से, [५] परिग्रह--धन आदि पदार्थों के संग्रह और उन पर ममत्व रखने से, [६] क्रोध- क्रोध करने से, [७] मान- अहंकार या मद करने से, [5] माया - कपट [ छल] करने से, [8] लोभ - लोभ, तृष्णा करने से, [१०] राग - सांसारिक पदार्थों पर राग - आसक्ति या मोह से, [११] द्वेषपदार्थों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या घृणा करने से, [१२] कलह-क्लेश करने से, [१३] अभ्याख्यान - - मिथ्या दोषारोपण से, [१४] पैशुन्य - चुगली करने से, [१५] परपरिवाद - परनिन्दा करने से, [१६] रति-भोगों में प्रीति, और अरति - संयम में अप्रीति से, [१७] मायामृषा- कपट सहित असत्याचरण
---
१ नवतत्त्व - प्रकरण गाथा १५-१६
२ 'पातयति नरकादिदुर्गतौ इति पापमृ ।'
--