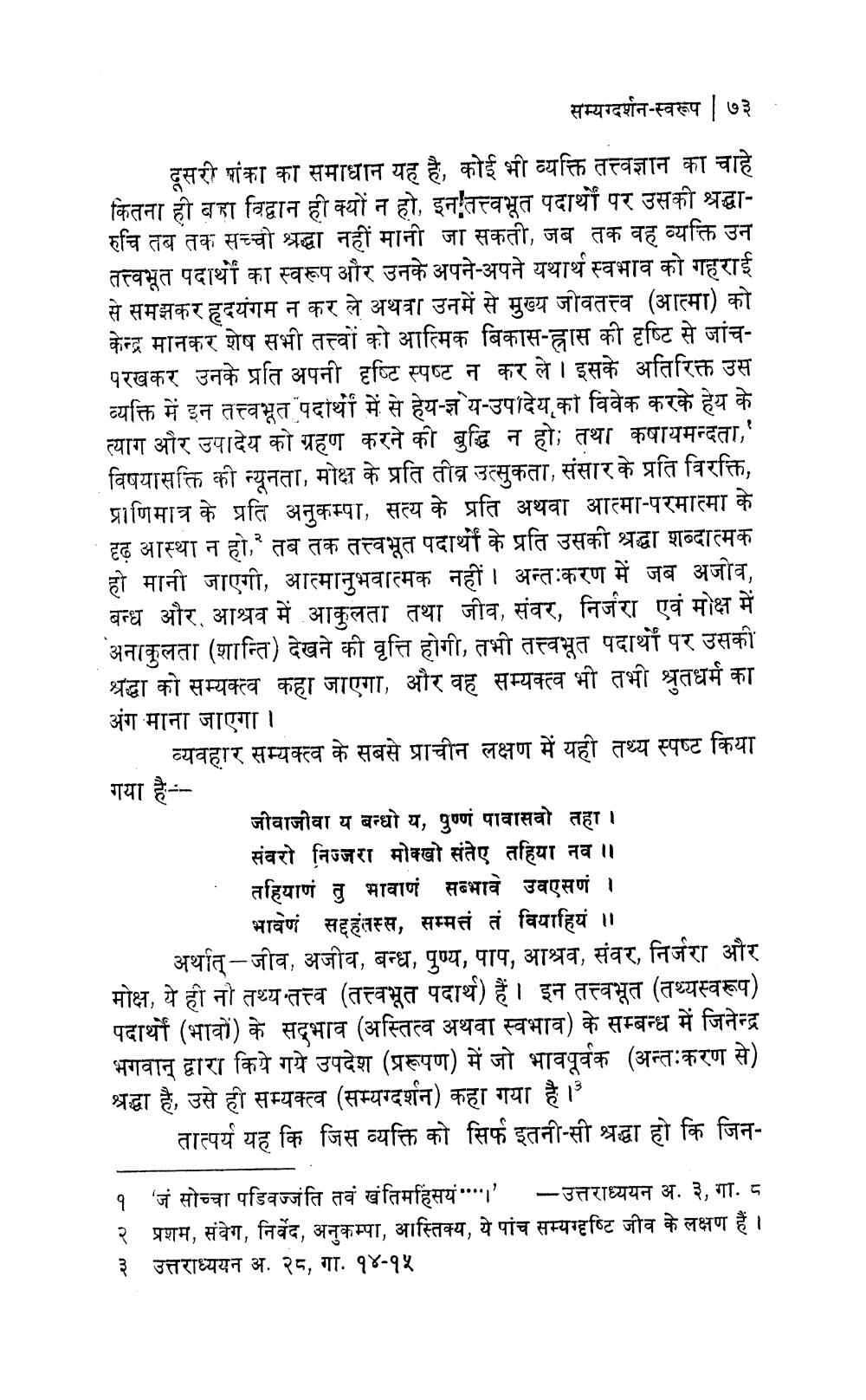________________
सम्यग्दर्शन- स्वरूप | ७३
दूसरी शंका का समाधान यह है, कोई भी व्यक्ति तत्त्वज्ञान का चाहे कितना ही बड़ा विद्वान ही क्यों न हो, इन तत्त्वभूत पदार्थों पर उसकी श्रद्धारुचि तब तक सच्ची श्रद्धा नहीं मानी जा सकती, जब तक वह व्यक्ति उन तत्त्वभूत पदार्थों का स्वरूप और उनके अपने-अपने यथार्थ स्वभाव को गहराई से समझकर हृदयंगम न कर ले अथवा उनमें से मुख्य जीवतत्त्व (आत्मा) को केन्द्र मानकर शेष सभी तत्त्वों को आत्मिक बिकास - ह्रास की दृष्टि से जांचपरखकर उनके प्रति अपनी दृष्टि स्पष्ट न कर ले। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति में इन तत्त्वभूत पदार्थों में से हेय-ज्ञ य उपादेय का विवेक करके हेय के त्याग और उपादेय को ग्रहण करने की बुद्धि न हो; तथा कषायमन्दता, ' विषयासक्ति की न्यूनता, मोक्ष के प्रति तीव्र उत्सुकता, संसार के प्रति विरक्ति, प्राणिमात्र के प्रति अनुकम्पा, सत्य के प्रति अथवा आत्मा-परमात्मा के दृढ़ आस्था न हो, तब तक तत्त्वभूत पदार्थों के प्रति उसकी श्रद्धा शब्दात्मक हो मानी जाएगी, आत्मानुभवात्मक नहीं । अन्तःकरण में जब अजीव, बन्ध और आश्रव में आकुलता तथा जीव, संवर, निर्जरा एवं मोक्ष में नाकुलता (शान्ति) देखने की वृत्ति होगी, तभी तत्त्वभूत पदार्थों पर उसकी श्रद्धा को सम्यक्त्व कहा जाएगा, और वह सम्यक्त्व भी तभी श्रुतधर्म का अंग माना जाएगा ।
ર
व्यवहार सम्यक्त्व के सबसे प्राचीन लक्षण में यही तथ्य स्पष्ट किया
गया है
-
जीवाजीवा य बन्धो य, पुण्णं पावासवो तहा । संवरो निज्जरा मोक्खो संतेए तहिया नव ॥ तहियाणं तु भावाणं सब्भावे उवएसणं । भावणं सद्दहंतस्स सम्मत्तं तं वियाहियं ॥
अर्थात् - जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये ही नो तथ्य तत्त्व ( तत्त्वभूत पदार्थ ) हैं । इन तत्त्वभूत (तथ्यस्वरूप ) पदार्थों (भावों) के सदभाव (अस्तित्व अथवा स्वभाव) के सम्बन्ध में जिनेन्द्र भगवान् द्वारा किये गये उपदेश (प्ररूपण) में जो भावपूर्वक (अन्तःकरण से ) श्रद्धा है, उसे ही सम्यक्त्व ( सम्यग्दर्शन) कहा गया है ।
तात्पर्य यह कि जिस व्यक्ति को सिर्फ इतनी-सी श्रद्धा हो कि जिन
१
'जं सोच्चा पडिवज्जं ति तवं खंतिमहिंसयं '' - उत्तराध्ययन अ. ३, गा. ८ २ प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा, आस्तिक्य, ये पांच सम्यग्दृष्टि जीव के लक्षण हैं । ३ उत्तराध्ययन अ. २८, गा. १४-१५