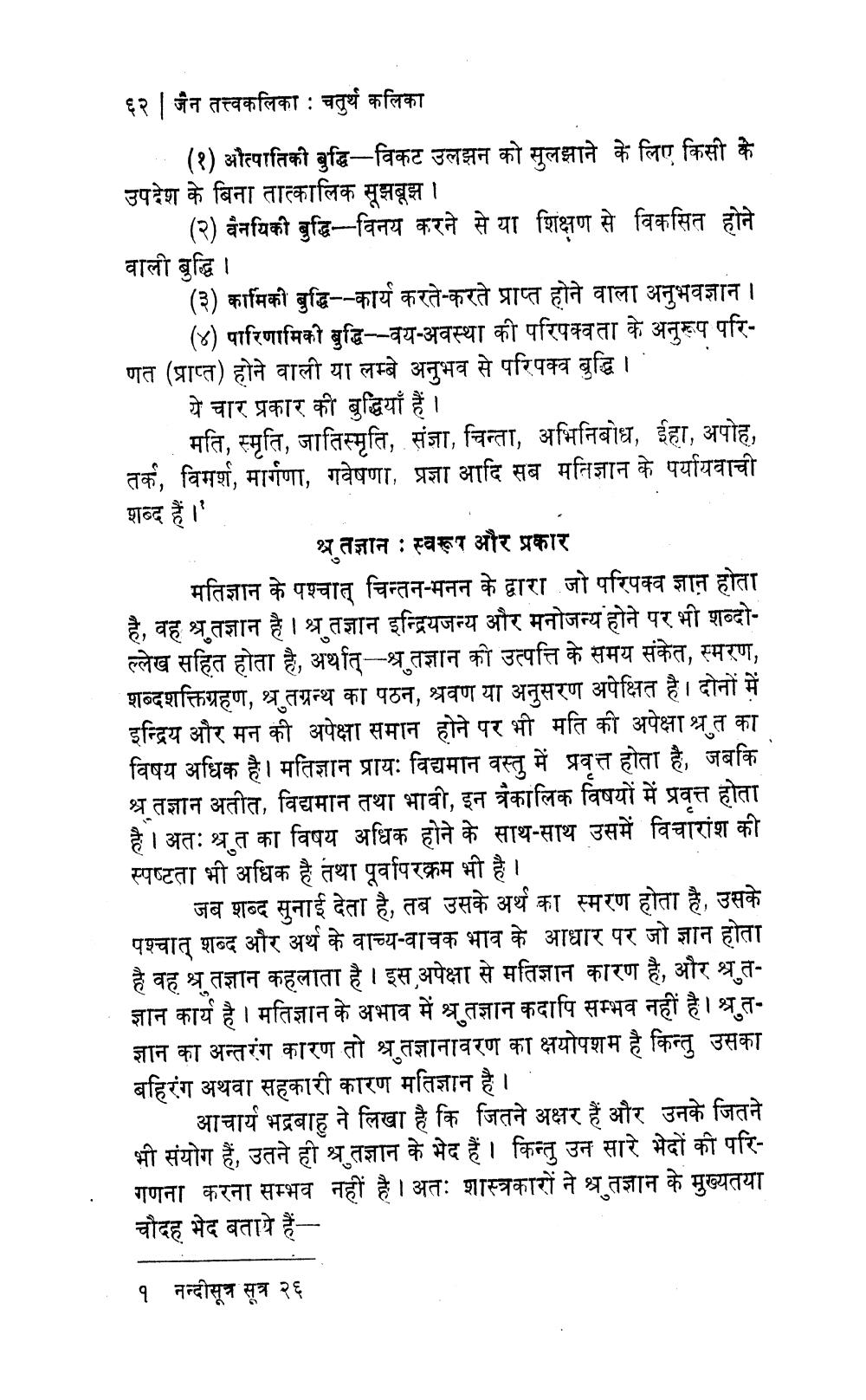________________
६२ | जैन तत्त्वकलिका : चतुर्थ कलिका
(१) औत्पातिकी बुद्धि - विकट उलझन को सुलझाने के लिए किसी के उपदेश के बिना तात्कालिक सूझबूझ ।
(२) वैनयिकी बुद्धि-विनय करने से या शिक्षण से विकसित होने वाली बुद्धि |
(३) कार्मिकी बुद्धि-- कार्य करते-करते प्राप्त होने वाला अनुभवज्ञान | (४) पारिणामिको बुद्धि-- वय अवस्था की परिपक्वता के अनुरूप परि णत ( प्राप्त) होने वाली या लम्बे अनुभव से परिपक्व बुद्धि । ये चार प्रकार की बुद्धियाँ हैं ।
मति, स्मृति, जातिस्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध, ईहा, अपोह, तर्क, विमर्श, मार्गणा, गवेषणा, प्रज्ञा आदि सब मतिज्ञान के पर्यायवाची शब्द हैं ।'
श्रुतज्ञान : स्वरूप और प्रकार
मतिज्ञान के पश्चात् चिन्तन-मनन के द्वारा जो परिपक्व ज्ञान होता है, वह श्रुतज्ञान है | श्रुतज्ञान इन्द्रियजन्य और मनोजन्य होने पर भी शब्दो - ल्लेख सहित होता है, अर्थात् श्रुतज्ञान की उत्पत्ति के समय संकेत, स्मरण, शब्दशक्तिग्रहण, श्रृतग्रन्थ का पठन, श्रवण या अनुसरण अपेक्षित है। दोनों में इन्द्रिय और मन की अपेक्षा समान होने पर भी मति की अपेक्षा श्रुत का विषय अधिक है । मतिज्ञान प्रायः विद्यमान वस्तु में प्रवृत्त होता है, जबकि श्रुतज्ञान अतीत, विद्यमान तथा भावी, इन त्रैकालिक विषयों में प्रवृत्त होता है | अतः श्रुत का विषय अधिक होने के साथ-साथ उसमें विचारांश की स्पष्टता भी अधिक है तथा पूर्वापरक्रम भी है ।
जब शब्द सुनाई देता है, तब उसके अर्थ का स्मरण होता है, उसके पश्चात् शब्द और अर्थ के वाच्य वाचक भाव के आधार पर जो ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान कहलाता है । इस अपेक्षा से मतिज्ञान कारण है, और श्रुतज्ञान कार्य है । मतिज्ञान के अभाव में श्रुतज्ञान कदापि सम्भव नहीं है। श्रुतज्ञान का अन्तरंग कारण तो श्रुतज्ञानावरण का क्षयोपशम है किन्तु उसका बहिरंग अथवा सहकारी कारण मतिज्ञान है ।
आचार्य भद्रबाहु ने लिखा है कि जितने अक्षर हैं और उनके जितने भी संयोग हैं, उतने ही श्रुतज्ञान के भेद हैं । किन्तु उन सारे भेदों की परिगणना करना सम्भव नहीं है । अतः शास्त्रकारों ने श्र तज्ञान के मुख्यतया चौदह भेद बताये हैं
१ नन्दीसूत्र सूत्र २६