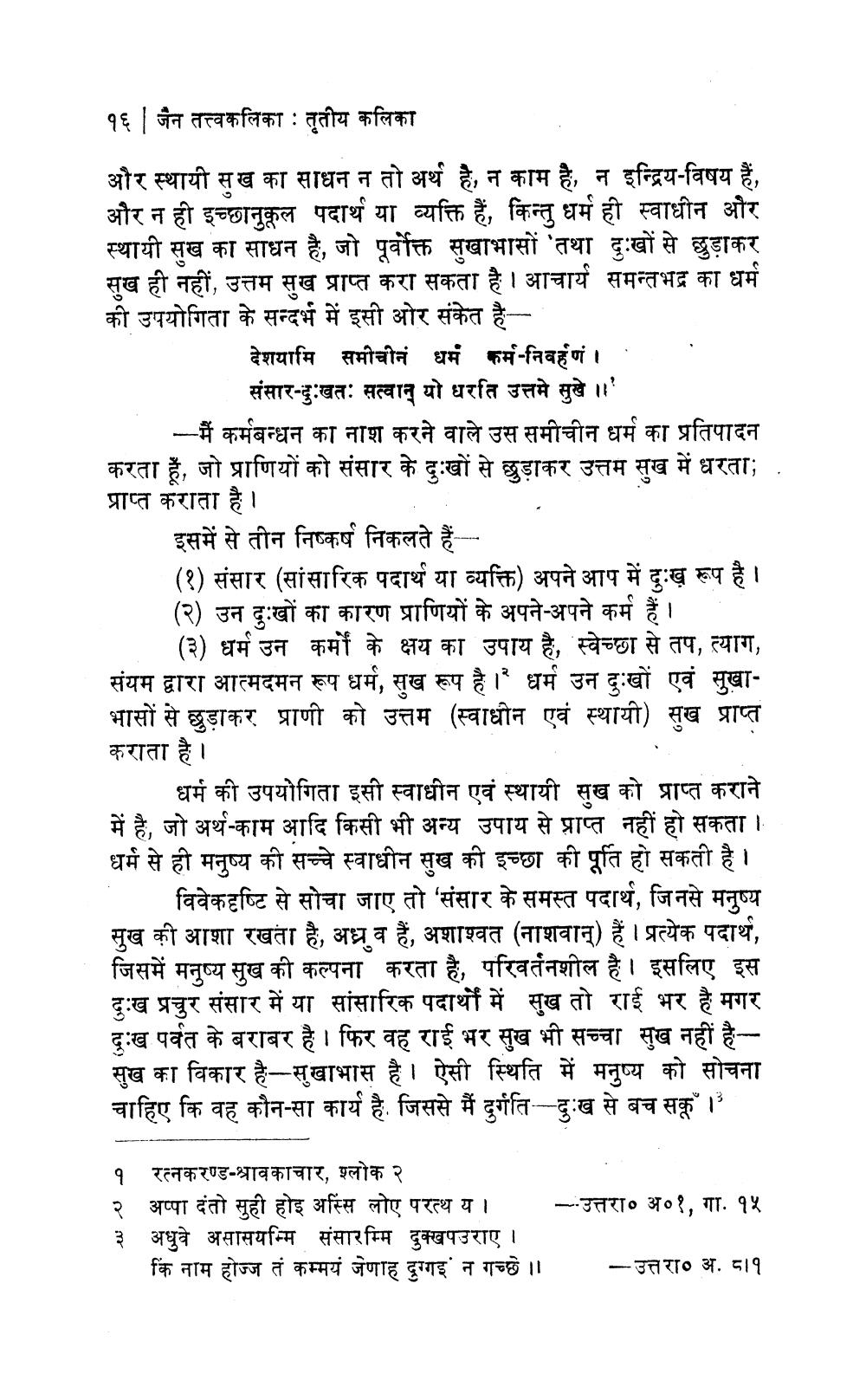________________
१६ | जैन तत्त्वकलिका : तृतीय कलिका
और स्थायी सुख का साधन न तो अर्थ है, न काम है, न इन्द्रिय विषय हैं, और न ही इच्छानुकूल पदार्थ या व्यक्ति हैं, किन्तु धर्म ही स्वाधीन और स्थायी सुख का साधन है, जो पूर्वोक्त सुखाभासों तथा दुःखों से छुड़ाकर सुख ही नहीं, उत्तम सुख प्राप्त करा सकता है । आचार्य समन्तभद्र का धर्म की उपयोगिता के सन्दर्भ में इसी ओर संकेत है
देशयामि समीचीनं धर्म कर्म निवर्हणं । संसार-दुःखतः सत्वान् यो धरति उत्तमे सुखे ।।'
- मैं कर्मबन्धन का नाश करने वाले उस समीचीन धर्म का प्रतिपादन करता हूँ, जो प्राणियों को संसार के दुःखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में धरता; प्राप्त कराता है ।
इसमें से तीन निष्कर्ष निकलते हैं
(१) संसार ( सांसारिक पदार्थ या व्यक्ति) अपने आप में दुःख रूप है । (२) उन दुःखों का कारण प्राणियों के अपने-अपने कर्म हैं ।
(३) धर्म उन कर्मों के क्षय का उपाय है, स्वेच्छा से तप, त्याग, संयम द्वारा आत्मदमन रूप धर्म, सुख रूप है ।" धर्म उन दुःखों एवं सुखाभासों से छुड़ाकर प्राणी को उत्तम (स्वाधीन एवं स्थायी) सुख प्राप्त कराता है ।
धर्म की उपयोगिता इसी स्वाधीन एवं स्थायी सुख को प्राप्त कराने है, जो अर्थ - काम आदि किसी भी अन्य उपाय से प्राप्त नहीं हो सकता । धर्म से ही मनुष्य की सच्चे स्वाधीन सुख की इच्छा की पूर्ति हो सकती है । विवेकदृष्टि से सोचा जाए तो 'संसार के समस्त पदार्थ, जिनसे मनुष्य सुख की आशा रखता है, अध्रुव हैं, अशाश्वत ( नाशवान् ) हैं । प्रत्येक पदार्थ, जिसमें मनुष्य सुख की कल्पना करता है, परिवर्तनशील है । इसलिए इस दुःख प्रचुर संसार में या सांसारिक पदार्थों में सुख तो राई भर है मगर दुःख पर्वत के बराबर है । फिर वह राई भर सुख भी सच्चा सुख नहीं हैसुख का विकार है - सुखाभास है । ऐसी स्थिति में मनुष्य को सोचना चाहिए कि वह कौन-सा कार्य है जिससे मैं दुर्गति - दुःख से बच सकूँ ।
१
रत्नकरण्ड श्रावकाचार, श्लोक २
२ अप्पा दंतो सुही होइ अस्सि लोए परत्थ य । ३ अधुवे असासयम्मि संसारम्मि दुक्खपउराए । किं नाम होज्ज तं कम्मयं जेणाह दुग्गइ न गच्छे ||
- उत्तरा० अ०१, गा. १५
- उत्तरा० अ. ८1१