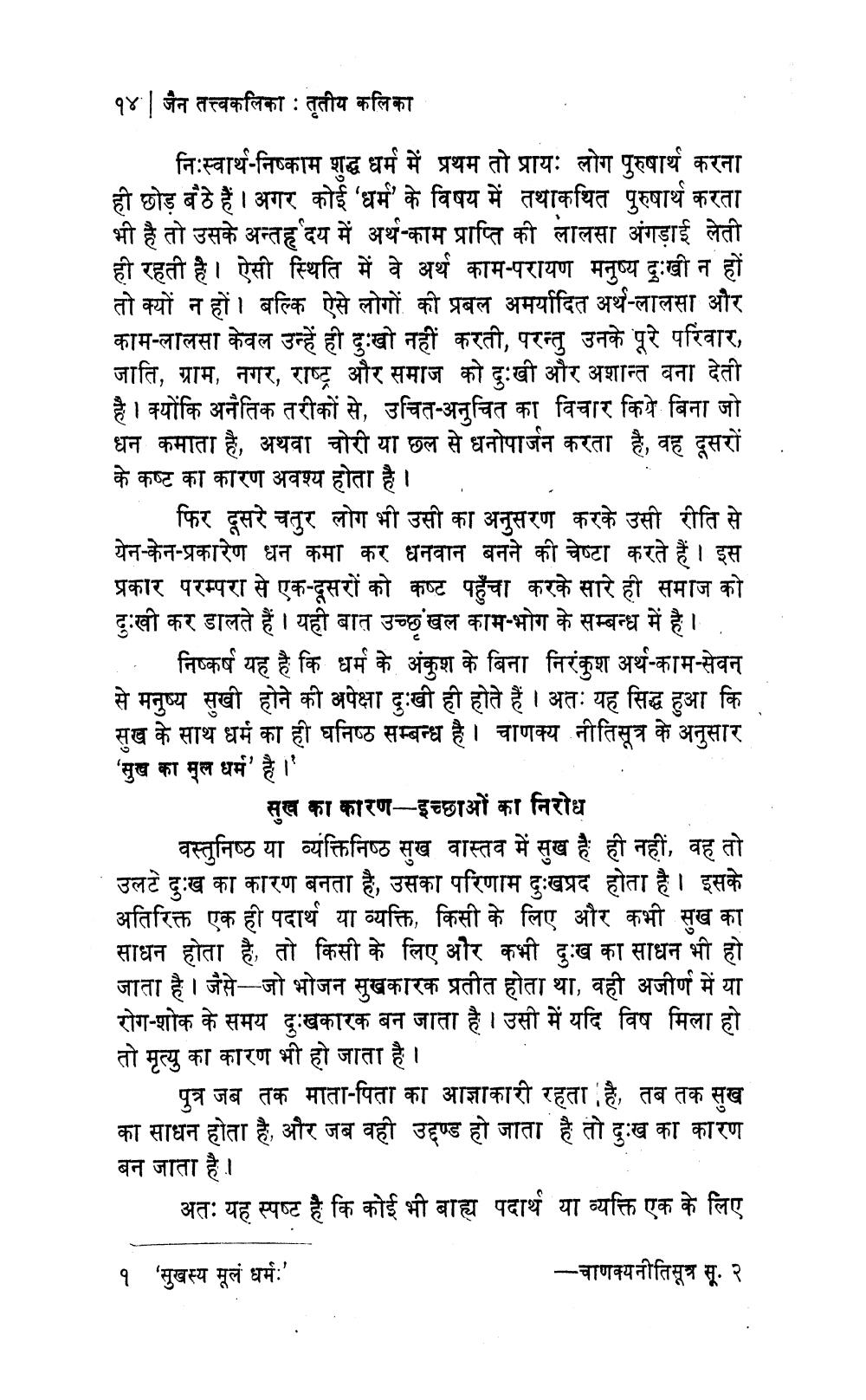________________
१४ | जैन तत्त्वकलिका : तृतीय कलिका ___निःस्वार्थ-निष्काम शुद्ध धर्म में प्रथम तो प्रायः लोग पुरुषार्थ करना ही छोड बैठे हैं। अगर कोई 'धर्म' के विषय में तथाकथित पुरुषार्थ करता भी है तो उसके अन्तर्हृदय में अर्थ-काम प्राप्ति की लालसा अंगड़ाई लेती ही रहती है। ऐसी स्थिति में वे अर्थ काम-परायण मनुष्य दुःखी न हों तो क्यों न हों। बल्कि ऐसे लोगों की प्रबल अमर्यादित अर्थ-लालसा और काम-लालसा केवल उन्हें ही दुःखो नहीं करती, परन्तु उनके पूरे परिवार, जाति, ग्राम, नगर, राष्ट्र और समाज को दुःखी और अशान्त बना देती है। क्योंकि अनैतिक तरीकों से, उचित-अनुचित का विचार किये बिना जो धन कमाता है, अथवा चोरी या छल से धनोपार्जन करता है, वह दूसरों के कष्ट का कारण अवश्य होता है।
फिर दूसरे चतुर लोग भी उसी का अनुसरण करके उसी रीति से येन-केन-प्रकारेण धन कमा कर धनवान बनने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार परम्परा से एक-दूसरों को कष्ट पहुँचा करके सारे ही समाज को दुःखी कर डालते हैं । यही बात उच्छंखल काम-भोग के सम्बन्ध में है। . .. निष्कर्ष यह है कि धर्म के अंकुश के बिना निरंकुश अर्थ-काम-सेवन से मनुष्य सुखी होने की अपेक्षा दुःखी ही होते हैं । अतः यह सिद्ध हुआ कि सुख के साथ धर्म का ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। चाणक्य नीतिसूत्र के अनुसार 'सुख का म्ल धर्म' है।'
सुख का कारण-इच्छाओं का निरोध वस्तुनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ सुख वास्तव में सुख है ही नहीं, वह तो उलटे दुःख का कारण बनता है, उसका परिणाम दुःखप्रद होता है। इसके अतिरिक्त एक ही पदार्थ या व्यक्ति, किसी के लिए और कभी सुख का साधन होता है, तो किसी के लिए और कभी दुःख का साधन भी हो जाता है। जैसे-जो भोजन सुखकारक प्रतीत होता था, वही अजीर्ण में या रोग-शोक के समय दुःखकारक बन जाता है । उसी में यदि विष मिला हो तो मृत्यु का कारण भी हो जाता है।
पुत्र जब तक माता-पिता का आज्ञाकारी रहता है, तब तक सुख का साधन होता है, और जब वही उद्दण्ड हो जाता है तो दुःख का कारण बन जाता है।
अतः यह स्पष्ट है कि कोई भी बाह्य पदार्थ या व्यक्ति एक के लिए
१ 'सुखस्य मूलं धर्मः'
-चाणक्यनीतिसूत्र सू. २