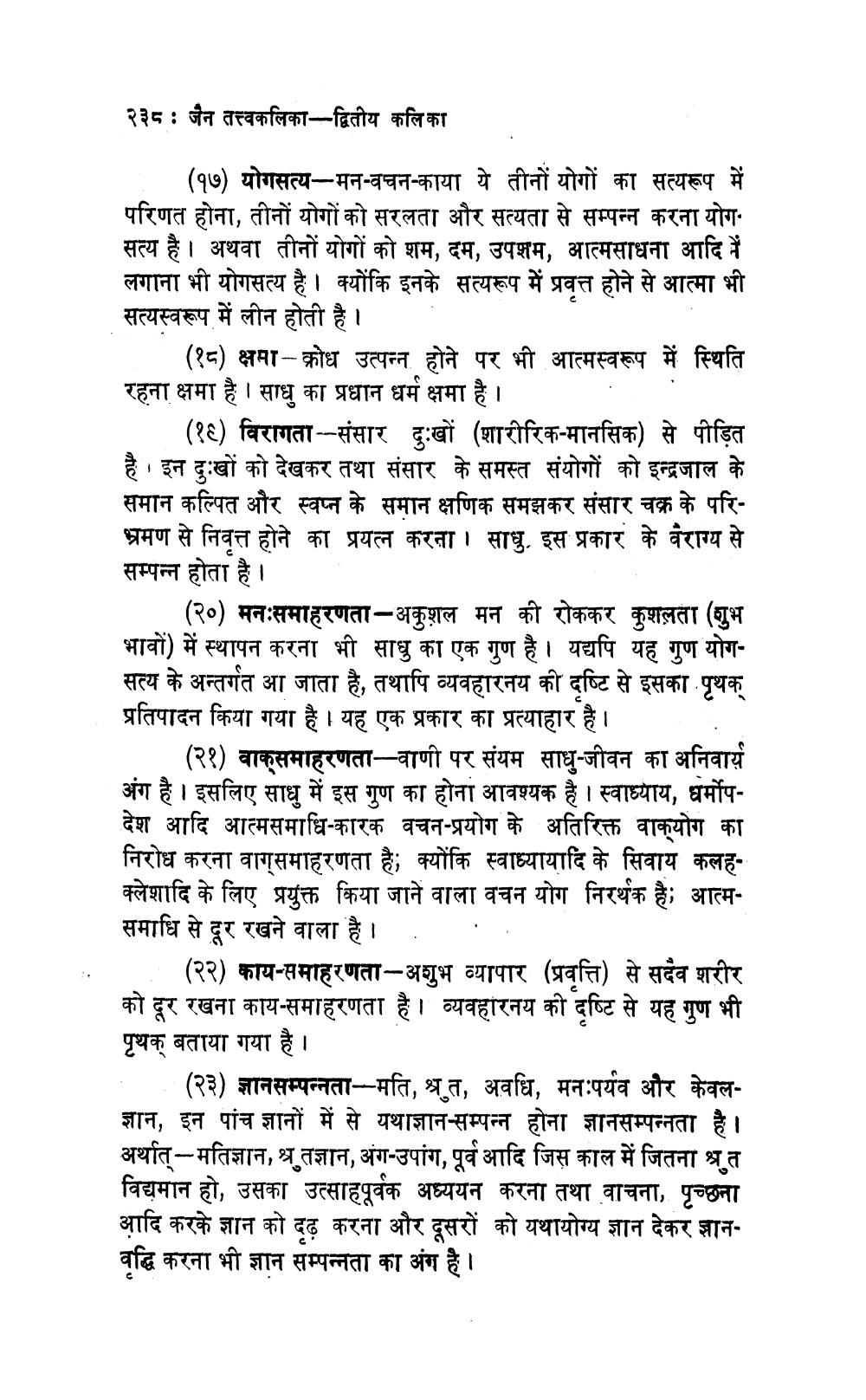________________
२३८ : जैन तत्त्वकलिका-द्वितीय कलिका
(१७) योगसत्य-मन-वचन-काया ये तीनों योगों का सत्यरूप में परिणत होना, तीनों योगों को सरलता और सत्यता से सम्पन्न करना योगसत्य है। अथवा तीनों योगों को शम, दम, उपशम, आत्मसाधना आदि में लगाना भी योगसत्य है। क्योंकि इनके सत्यरूप में प्रवत्त होने से आत्मा भी सत्यस्वरूप में लीन होती है।
(१८) क्षमा-क्रोध उत्पन्न होने पर भी आत्मस्वरूप में स्थिति रहना क्षमा है । साधु का प्रधान धर्म क्षमा है।
(१९) विरागता--संसार दुःखों (शारीरिक-मानसिक) से पीड़ित है। इन दुःखों को देखकर तथा संसार के समस्त संयोगों को इन्द्रजाल के समान कल्पित और स्वप्न के समान क्षणिक समझकर संसार चक्र के परिभ्रमण से निवृत्त होने का प्रयत्न करना। साधु, इस प्रकार के वैराग्य से सम्पन्न होता है।
(२०) मनःसमाहरणता-अकुशल मन की रोककर कुशलता (शुभ भावों) में स्थापन करना भी साधु का एक गुण है। यद्यपि यह गुण योगसत्य के अन्तर्गत आ जाता है, तथापि व्यवहारनय की दृष्टि से इसका पृथक् प्रतिपादन किया गया है। यह एक प्रकार का प्रत्याहार है।
(२१) वाक्समाहरणता-वाणी पर संयम साधु-जीवन का अनिवार्य अंग है। इसलिए साधु में इस गुण का होना आवश्यक है। स्वाध्याय, धर्मोपदेश आदि आत्मसमाधि-कारक वचन-प्रयोग के अतिरिक्त वाक्योग का निरोध करना वाग्समाहरणता है; क्योंकि स्वाध्यायादि के सिवाय कलहक्लेशादि के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला वचन योग निरर्थक है; आत्मसमाधि से दूर रखने वाला है।
(२२) काय-समाहरणता-अशुभ व्यापार (प्रवृत्ति) से सदैव शरीर को दूर रखना काय-समाहरणता है। व्यवहारनय की दष्टि से यह गुण भी पृथक् बताया गया है। ___(२३) ज्ञानसम्पन्नता-मति, श्र त, अवधि, मनःपर्यव और केवलज्ञान, इन पांच ज्ञानों में से यथाज्ञान-सम्पन्न होना ज्ञानसम्पन्नता है। अर्थात्-मतिज्ञान, श्रु तज्ञान, अंग-उपांग, पूर्व आदि जिस काल में जितना श्रुत विद्यमान हो, उसका उत्साहपूर्वक अध्ययन करना तथा वाचना, पृच्छना आदि करके ज्ञान को दढ़ करना और दूसरों को यथायोग्य ज्ञान देकर ज्ञानवृद्धि करना भी ज्ञान सम्पन्नता का अंग है।